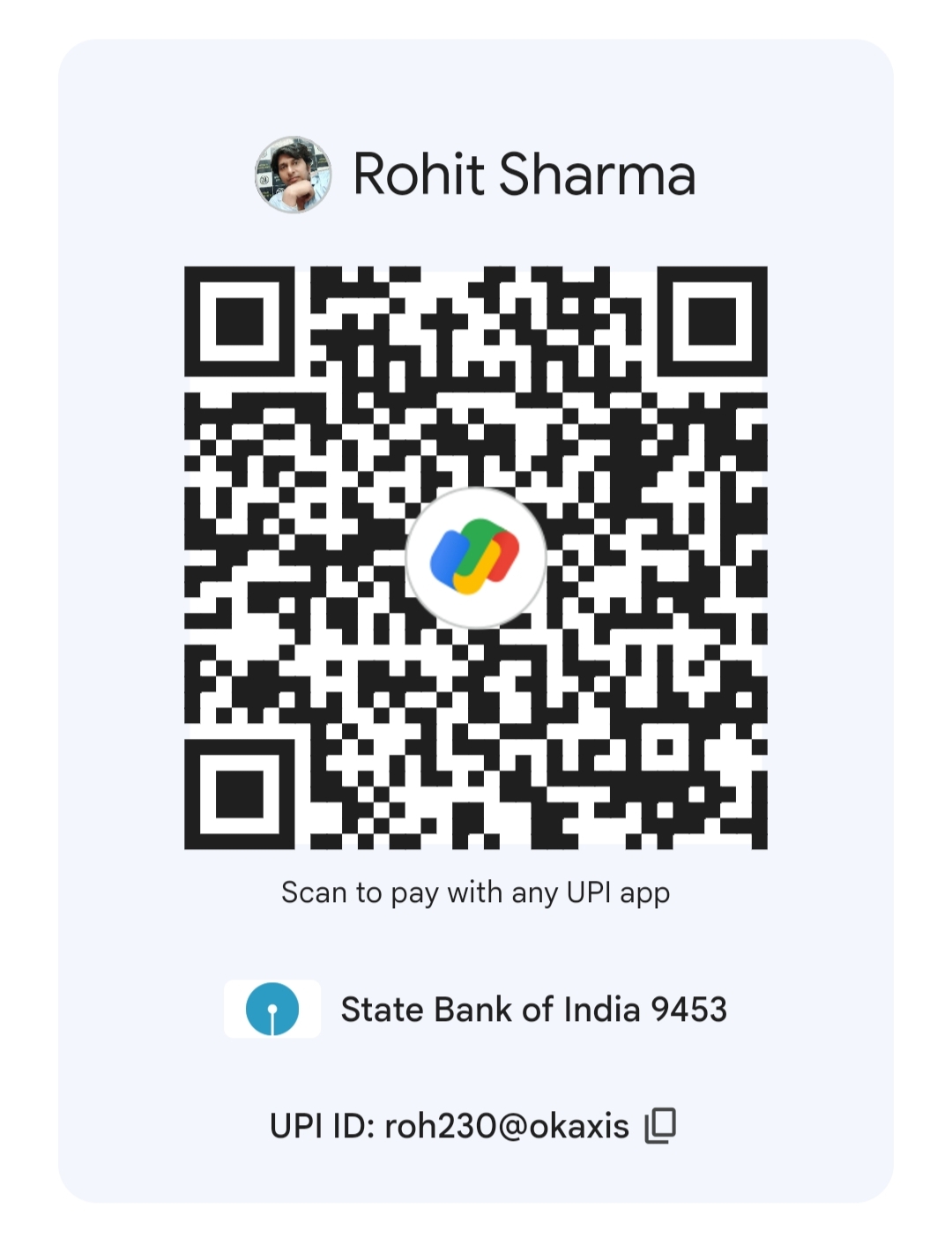इन्द्र कुमार
लेखक एक जीवित ईकाई है. इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि वह प्रत्येक अन्याय के विरोध में मुखर रहे. विरोध जीवित होने का प्रमाण है. वह किसी ऐसे समूहगान का हिस्सा न बने, न ही किसी ऐसे सुर में सुर मिलाए जो तात्कालिक है. उसकी मंशा वह नहीं ही रहे जो एक सरलीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हों. यद्यपि उस मध्य एक लेखक की ओर से एक भिन्न स्वर का उठना लेखक के लिए एक अनावश्यक जोखिम हो सकता है; लेकिन वह बेहद जरूरी है.
एक लेखक के लिए यह अनिवार्य शर्त की तरह है कि वह सत्ता के गलियारों की कि उसकी पहुंच के आधार पर पुरस्कृत होने का कामी न हो. वह किसी भी सामाजिक प्रभाव-शक्ति को अपनी साहित्यिक क्षमता न माने. किसी योग्य लेखक को उपेक्षित कर अन्य अयोग्य को सम्मानित किया जाए, यह अकादमिक बातें हैं.
लेखक न सिर्फ समाजिक महत्वाकांक्षा से परे है, बल्कि वह लेखकीय महत्वाकांक्षा से भी परे है. वह किसी दरबार का चारण है न भाट. वह लिखता इसलिए है क्योंकि वह प्रतिरोध का जरिया होता है.
अब सच बात यह है कि अकादमी पुरस्कार के लिए कविता नहीं चाहिए होता है ! न ही वह किसी कवि की कविता का कोई मानकीकरण है. बल्कि अकादमी पुरस्कार के लिए कविता में भाववादी रूझान की दरकार होती है, जो एक नियोजन में ही लिखी जा सकती है.
अकादमी के लिए ‘टर्म एंड कंडीशन्स’ ऐसे अप्लाइड होते हैं कि विचार या कि विचारधारा से कविता मुक्त रहें. यानी, कवि चोर के दाड़ी में तिनके को नज़रंदाज़ करे. वह हवा हवाई में मनुष्यता की बात कहे, मनुष्य के जरूरी और बुनियादी संघर्ष से विलग एक ऐसे प्रलाप में पाठक को उलझा दे कि आह के सिवा कोई और तान दिखाई ही न दे, सिर्फ कलात्मक बाजीगरी ही दिखे.
मसलन गगन गिल की इस कविता को ही ले लें, जो उनके अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य संग्रह ‘मैं जब तक आई बाहर’ से है. उम्मीद और धैर्य का रिश्ता चोली और दामन का है. लेकिन गगन गिल को बस उम्मीद चाहिए; थोड़ी-सी उम्मीद चाहिए वह भी कैसे और, कितना ?
‘जैसे मिट्टी में चमकती
किरण सूर्य की
जैसे पानी में स्वाद
भीगे पत्थर का”
बस इत्ती-सी.
भाई ! कविता हवाई उड़ान भरने के बजाय यथार्थ की जमीन पर क्यों नहीं चल सकती ? क्या कोई श्रम करता मेहनत मजूर कि किसान कविता की ज़मीं को बंजर बना देगा ??
जीवन जितना जटिल और संकटग्रस्त हुए हैं, उसका कोई भी बिंब कवि के लिए इस कदर औचित्यहीन हो जाए ! कि कवि के पास वह नहीं है और है तो बस –
‘जैसे भीगी हुई रेत पर
मछली में तड़पन”
की ही तरह बची हो
कि बस थोड़ी-सी उम्मीद चाहिए
यह उम्मीद भी चाहिए तो कितनी ?
बस इतना ही कि
जैसे गूंगे के कंठ में
याद आया गीत
जितना ही. आह ! क्या कामनाएं हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बीच कामातुर सत्ताएं और उसकी ग्रंथियां नहीं हो रहे हैं जवां ? जो दिन ब दिन डैने पसारे, पांव फैलाए हजारों योजन की दूरी तय कर सकी हैं.
गगन गिल की इस भाववादी पोयटिकल समझ और चेतना विहीन रचना (रचनात्मक नहीं कहूंगा) उपस्थिति को जो कुछ टटके हुए बिंबों के भरोसे है; उस पर अकादमी को तो न्यौछावर होना ही है जहां हल्की-सी सांस सीने में अटकी रहे ! या कि जैसे नदी की यह में
डूबी हुई प्यास बनी रहे. अकादमी को बस यही थोड़ी सी उम्मीद ही चाहिए ! बाक़ी तो अकादमी भीतर बाहर तक पैवस्त है.
कविता में बिना संघर्ष के उम्मीद का इससे बेहतर नमूना क्या ही हो ? पाठकों सोचो कि पुरस्कृत कवि और अकादमी मिल हिंदी का बंटाधार कैसे-कैसे करने लगे हैं. विशेष यह कि कवि इस कविता पर कोट करते हुए लिखता है कि – ‘मैं लिखना तभी चाहती हूं जब वह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो और मुझे किसी नई अनजानी जगह पर ले जाने वाला हो.’
यह देख, ताज्जुब होता है कि कवि किस अनजानी जगह जाने की बात कह रहा है ? कि कौन से मुश्किलात में है ?
थोड़ी-सी उम्मीद चाहिए
जैसे मिट्टी में चमकती
किरण सूर्य की
जैसे पानी में स्वाद
भीगे पत्थर का
जैसे भीगी हुई रेत पर
मछली में तड़पन
थोड़ी -सी उम्मीद चाहिए
जैसे गूंगे के कंठ में
याद आया गीत
जैसे हल्की-सी सांस
सीने में अटकी
जैसे कांच से चिपटे
कीट में लालसा
जैसे नदी की यह में
डूबी हुई प्यास
थोड़ी सी उम्मीद चाहिए.
‘मैं जब तक आई बाहर’ यह संकलन की शीर्षक कविता है. सिर्फ निजी और एकांतिक भाव है. बाहर आने की न कोई जद्दोजहद है, न संघर्ष. सुनियोजित प्रलाप है.
‘मैं जब तक आई बाहर
एकांत से अपने,
बदल चुका था
रंग दुनिया का
अर्थ भाषा का
मंत्र और जप का
ध्यान और प्रार्थना का
कोई बंद कर गया था
बाहर से’
बड़ी अजीब बात है, कौन है जो बदल दे रहा है चीजों का अर्थ ? कि कपाट बंद कर गया है ? जब आप कीमियागर हो, उसमें मजबूत दखल रखते हों तो जीवन के असल संघर्ष इसी तरह के अर्थहीन प्रलाप में ढांप देते जाएंगे. तमाम संकट और दुर्धुर्ष संघर्ष को इसी तरह धुंधला कर देखेंगे. तब आपको न लोक का संघर्ष दिखेगा, न कोई वैज्ञानिक चेतना ही आपको को मजबूत बना पाएंगे. चूंकि आप कोठरियों और मंत्रों में भटकते रहेंगे –
‘देवताओं की कोठरियां
अब वे खुलने में न आती थीं
ताले पड़े थे तमाम शहर के
दिलों पर
होंठों पर
आंखें ढंक चुकी थीं
नामालूम झिल्लियों से
सुनाई कुछ पड़ता न था
मैं जब तक आई बाहर
एकांत से अपने
ऐसा तब ही होता है जब आप विशुद्ध निजी ख्याल, ख्याति और प्रसिद्धि में खो जाते हैं. इस कविता में यद्यपि गगन गिल जो कह रही हैं कि –
रंग हो चुका था लाल
आसमान का
यह कोई युद्ध का मैदान था
चले जा रही थी
जिसमें मैं
जीवन और संघर्ष के रास्ते वही है, पथ वही है भटकने हो स्वाभाविक रूप से देरी कर ही आएंगे
लाल रोशनी में
शाम में
मैं इतनी देर में आई बाहर
कि योद्धा हो चुके थे
अदृश्य
शहीद
युद्ध भी हो चुका था
अदृश्य
एक प्रगतिशील कविता और कलावादी कविता के मध्य एक बड़ा अंतर यही है कि कलावादी कविता बिना किसी ज्ञात स्त्रोतों और अपुष्ट माध्यमों में तथा हवा हवाई भाव उद्वेगों के भरोसे चलती है, जबकि प्रगतिशील कविता के हाथ पांव साबूत होते हैं जैसा कि गगन गिल त्रासदी के बयां पर कहतीं हैं –
अब भी
सब ओर
कहां पड़ रहा था
मेरा पैर
चीख़ आती थी
किधर से
पता कुछ चलता न था
मैं जब तक आई बाहर
ख़ाली हो चुके थे मेरे हाथ
न कहीं पट्टी
न मरहम
पूरी कविता एक आवरण में रचाई गई जो भीतर से खोखला है.
अंत में , बकौल दुष्यंत कुमार के कहूंगा कि –
‘सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए.’
Read Also –
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]