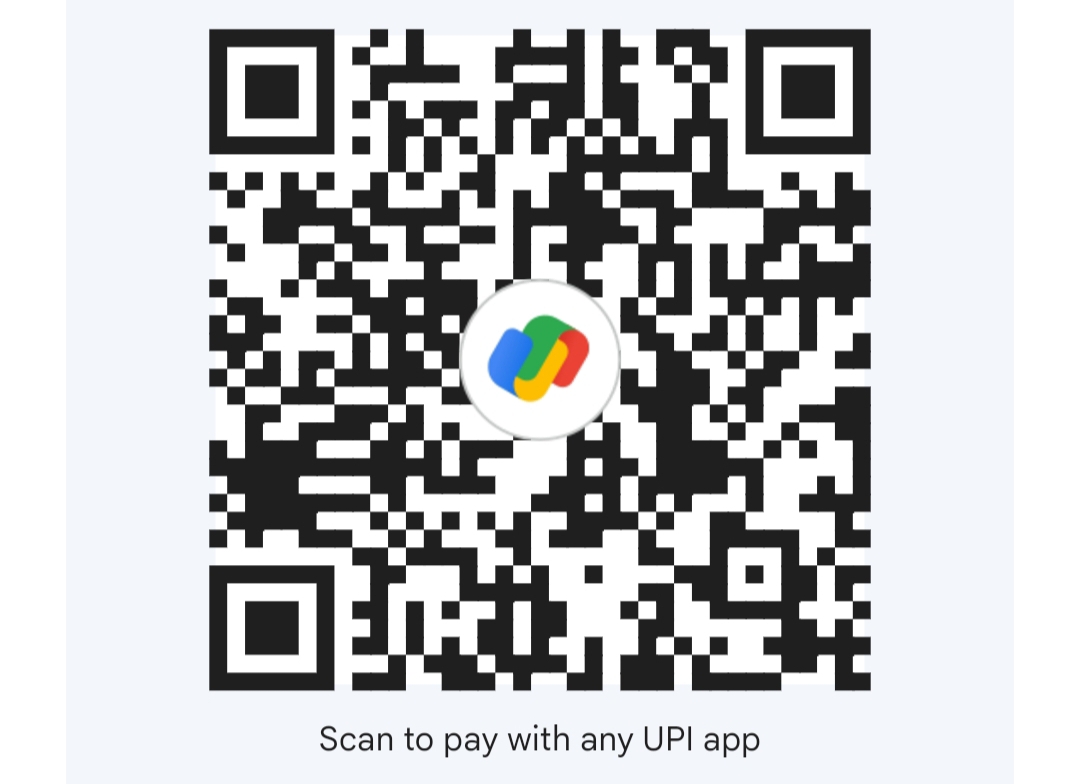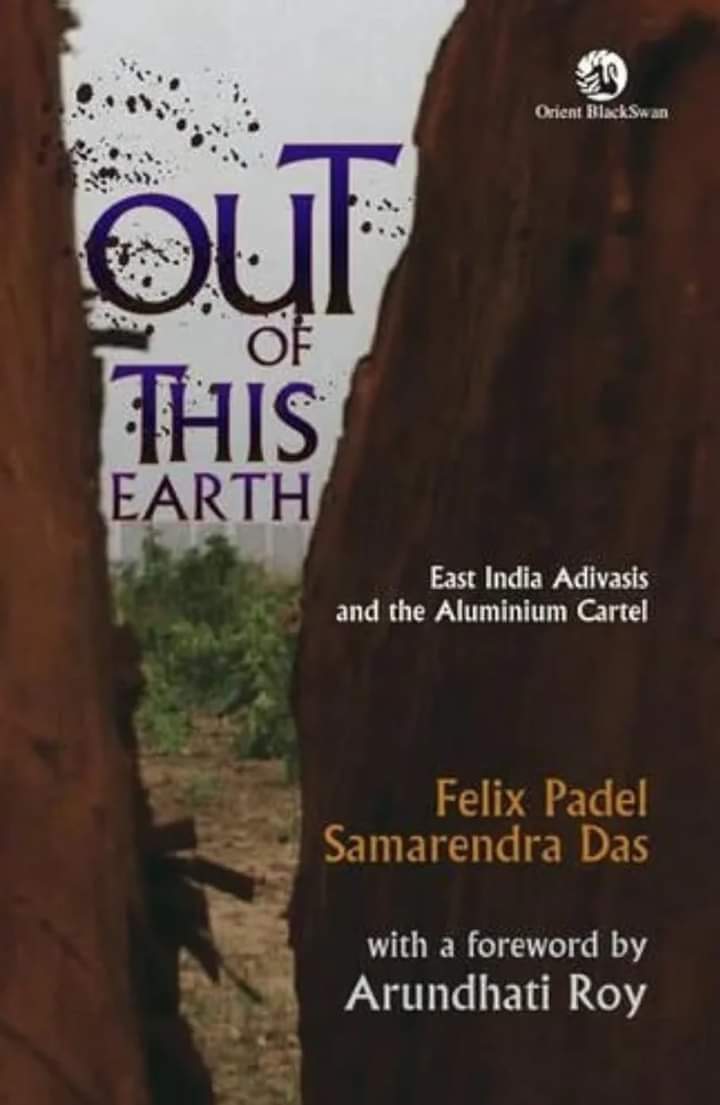
मनीष आजाद
भारत के पूर्वी राज्यों विशेषकर उड़ीसा, छत्तीसगड़ और झारखण्ड में खनन कम्पनियों और वहां के मूल निवासियों के बीच संघर्ष की खबरें आती रही हैं. सरकार अपने चरित्र के अनुसार प्रायः कम्पनियों के साथ ही खड़ी नज़र आती है. जिन्होंने भी इन घटनाक्रमों को थोड़ा फालो किया होगा, वे ‘फेलिक्स पडेल’ और ‘समरेन्द्र दास’ का नाम जरुर जानते होगेे.
लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता फेलिक्स पडेल और समरेन्द्र दास की संयुक्त रुप से लिखी पुस्तक ‘आउट ऑफ दिस अर्थ’ 2010 में प्रकाशित हुई थी. इसकी भूमिका ‘अरुंधति राय’ ने लिखी है. 742 पृष्ठों की यह बृहद पुस्तक एक तरफ खनन कम्पनियों और प्रकारान्तर से पूंजीवाद के काम करने के तरीकों की बहुत तीखी पड़ताल करती है तो वही दूसरी तरफ अदिवासियों के जीवन मूल्यों, उनके दर्शन, उनके प्रतिरोध तथा प्रकृति के साथ उनके संबंधो पर पर्याप्त रोशनी डालती है.
हालांकि केस स्टडी के रुप में यह पुस्तक उड़ीसा में अल्यूमिनियम खनन और इससे हो रहे पर्यावरण विनाश तथा आदिवासियों-दलितों के विस्थापन और उनके प्रतिरोध को ही सामने रखती है. लेकिन संदर्भ के बहाने यह किताब पूरी दुनिया का भ्रमण करती है और बहुत दिलचस्प और सशक्त तरीके यह बताती है कि आज जो उड़ीसा में हो रहा है वह कोई अलग थलग घटना नही हैं, वरन साम्राज्यवाद की विशेष नीतियों के तहत यह पूरी दुनिया में घटित हो रहा है.
हर जगह ‘दमन और प्रतिरोध’ की कहानी एक ही है
अल्यूमिनियम को ‘ग्रीन मेटल’ माना जाता है, क्योंकि इसे आसानी से ‘रिसाइकिल’ किया जा सकता है. इसके अलावा इसका भार कम होने से इसका बड़े पैमाने पर वाहनों विशेषकर कारों की बंडी बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे वाहनों का भार कम हो रहा है और उनकी प्रति किमी क्षमता बड़ रही हैं. फलतः ईधन की बचत हो रही है.
लेखक ने इसी मिथक को तोड़ा है. दरअसल अल्यूमिनियम अपने मूल रुप में अंक्सीजन के साथ ‘केमिकल बाण्ड’ बनाये रखता है. अल्यूमिनियम निकालने के लिए इस बाण्ड को तोड़ना पड़ता है, इसके लिए काफी उर्जा की जरुरत होती है. इस उर्जा की जरुरत को पूरा करने के लिए अल्यूमिनियम फैैक्टरी यानी ‘स्मेल्टर’ के नजदीक बिजली घर की जरुरत होती है. और इस बिजली घर के लिए पानी की जरुरत को पूरा करने के लिए बड़े बांधों की जरुरत होती है. अब तक बड़े बांधों पर जो भी विमर्श रहा है, वह विस्थापन के इर्द गिर्द ही रहा है. यहां तक की अरुंधति राय ने भी बड़े बांधों पर लिखे अपने लेखों में इस पहलू को नजरअंदाज किया है.
लेकिन लेखक के अनुसार दुनिया में जहां भी बड़े बांध बने हैं, उनमें से ज्यादातर का उद्देश्य अल्यूमिनियम उद्योग की सेवा करना रहा है. अन्य चीजें इसके बाद ही आती है. 1947 के बाद बना ‘हीराकुण्ड बांध’ भी मुख्यतः बिरला की अल्यूमिनियम कंपनी ‘हिंडाल्को’ को पानी देने के लिए बना था. इस रुप में दुनिया की सभी अल्यूमिनियम कंपनियां सरकारी सब्सिडी का भरपूर इस्तेमाल करती है और अपने उत्पाद का दाम कम से कम रखने में कामयाब रहती है.
ये सभी कंपनियां सरकार से सामान्य से कई गुना तक कम दर पर बिजली प्राप्त करती हैं. ‘रिहन्द बांध’ से बन रही बिजली अल्युमिनियम कम्पनी हिन्डाल्को को किस दर पर दी जा रही थी ? समाजवादी नेता ‘राममनोहर लोहिया’ द्वारा संसद में पूछे गये एक प्रश्न के जवाब में बताया गया कि हिन्डाल्को को बिजली 1.99 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जा रही है. उस समय सामान्य लोगों को यह बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जा रही थी.
यही पर ‘विश्व बैंक’ और ’आईएमएफ’ का पदार्पण होता है क्योकि बांध बनाने के लिए, बिजलीघर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए कर्ज यहीं से आयेगा और शर्तो के साथ आयेगा. इस तरह इन कर्जो का पूरा इस्तेमाल ये निजी कंपनियां करती हैं और देश कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है. फिर इन कर्जों से निकलने के लिए सरकारों को और कर्ज लेना पड़ता है और फिर और शर्ते माननी होती है. इन शर्तो में यह भी शामिल होता है कि आपको फलां कम्पनी को अपना सलाहकार नियुक्त करना होगा. और अनिवार्यतः ये कम्पनियां यूरोपियन-अमरीकन या जापान की ही होती हैं. यानी कर्ज मिलते ही इसका एक बड़ा हिस्सा तत्काल फिर उन्हीं के पास वापस लौट जाता है.
2002 में ब्रिटिश संस्था ‘डीएफआइडी’ से उड़ीसा सरकार को मिले कर्ज में से 350 करोड़ रुपये उन ब्रिटिश सलाहकार फर्मो को देने पड़े, जो उड़ीसा सरकार को यह सलाह देने वाली थी कि वे अपने राज्य में निजीकरण की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाये. इसके अलावा इन शर्तों में अब यह भी शामिल हो जाता है कि सरकार जनता पर खर्च करने वाली सब्सिडी खत्म करेगी. और यहीं से शुरु हो जाता है – ‘नवउदारवाद.’ इस परिघटना का बहुत ही रोचक, सरल और तथ्यतः वर्णन इस किताब में किया गया है.
आज अल्यूमिनियम का इस्तेमाल चीजों को ताजा रखने के लिए डिब्बाबन्द पैकिंग में विशाल पैमाने पर हो रहा है. ‘टेट्रा पैक’ नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनी का काम ही है, ऐसी मशीनों का निर्माण जो डिब्बाबन्द पैकिंग का काम करती हैं. हमारे घरों में भी अल्युमिनियम का ‘फायल पेपर’ अब एक जरुरत बन चुका है. लेखक ने शरीर पर पड़ने वाले इसके खतरनाक दुष्प्रभावों पर काफी जोर दिया है, जिससे प्रायः हम लोग अनजान हैं.
कई शोधों का हवाला देते हुए लेखक बताता है कि विश्व में बढ़ रहे ‘अल्जाइमर’ रोग का प्रधान कारण अल्युमिनियम ही है. इसके अलावा कई तरह के कैन्सर तथा अन्य रोगों का भी अल्यूमिनियम एक बड़ा कारण है. अल्युमिनियम कम्पनियां अपनी ताकत और पैसे के बल पर इन शोधों को दबा रही है इसलिए यह मुख्यधारा की मीडिया की चिन्ता नही बन रहा है. ये कम्पनियां कई तरह के झूठे शोध भी करा रही है, जिसमें यह स्थापित किया जा रहा है कि अल्जाइमर का अल्यूमिनियम से कोई लेना देना नहीं है.
अल्यूमिनियम उद्योग आज इसलिए भी इतना ताकतवर है कि इसका सीधा संबंध युद्ध उद्योग से है. आज युद्ध उद्योग में विशेषकर युद्धक विमान बनाने में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है. सभी बड़ी अल्यूमिनियम कम्पनियां किसी ना किसी युद्ध उपकरण बनाने वाली कम्पनियों से जुड़ी हुई हैं. जैसे टाटा की अल्यूमिनियम कम्पनी और ‘एचएएल’ ‘लाकहिड मार्टिन’ (यह एफ 16 बनाती है) से जुड़ी है तो ‘हिल्डाको’ ‘बोइंग’ और ‘एयरबस’ से. इसी कारण इसे ‘स्ट्रैटेजिक मेटल’ भी कहते हैं.
तेल और कोयले की तरह अल्यूमिनियम जमीन के अन्दर निष्क्रिय पड़ा नही रहता. ऑक्सीजन के साथ सहज बाण्ड होने के कारण यह नमी को जमीन में बनाये रखता है. और इस कारण जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है. नियामगिरी के पहाड़ों पर जो बाक्साइट है, उसका महत्व तो और भी ज्यादा है. बारिश के पानी को यह नमी के रुप में सोखकर साल भर अपने छोटे छोटे सोते के रुप वहां के आदिवासियों को बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराता है.
वेदान्ता कम्पनी को इसी नियामगिरी को खोदने को ठेका मिला था. इससे पर्यावरण का भयानक विनाश होता है और इसी से जुड़ा हुआ है विस्थापन का सवाल, जिसे बहुत शिद्दत के साथ इस किताब में उठाया गया है. लेखक ने इस पूरे विस्थापन के सवाल को एक पूरे समुदाय के ‘सांस्कृतिक जनसंहार’ (cultural genocide) से जोड़ कर देखा है. लेखक ने अनुमान लगाया है कि 1947 के बाद करीब 6 करोड़ लोग इस सांस्कृतिक जनसंहार के शिकार हो चुके हैं. इसमें से करीब 75 प्रतिशत आदिवासी और दलित हैं.
विस्थापन के अलावा इन उद्योगों और बांध बनने के दौरान जो औद्योगिक दुर्घटनाएं होती है, लेखक ने उस पर भी चर्चा की है. भारत के पहले बांध हीराकुण्ड बांध पर तो उन 200 मजदूरों के बकायदा नाम दर्ज हैं, जो इसके निर्माण के दौरान मारे गयेे. बाद में यह परंपरा खत्म कर दी गयी और अब तो इस तरह की किसी भी दुर्घटना को औपचारिक रुप से दर्ज नही किया जाता.
कान्ट्रैक्ट, सब कान्ट्रैक्ट की पूरी श्रंखला के कारण अब मूल कंपनी ऐसे मामलों में साफ बच निकलती है. लेखक ने भारत में 1991 में घटी एक ऐसी ही दुर्घटना का जिक्र किया है जब एक बांध के टनल में अचानक पानी भर जाने से करीब 400-500 मजदूर मारे गये, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ.
प्रथम विश्व युद्ध के पहले और बाद में किस तरह से बड़ी बड़ी कार्टेलों (अल्यूमिनियम के क्षेत्र में ‘आल्को’ और ‘कैसर’ पहली एकाधिकारी कम्पनियां हैं. भारत में 1938 में जो पहली अल्यूमिनियम कम्पनी ‘इण्डेल’ का निर्माण हुआ. वह अमरीकी कम्पनी ‘अल्कान’ के सहयोग से हुआ. ‘हिण्डाल्को’, ‘कैसर’ के सहयोग से खड़ी हुई.) का निर्माण हुआ और इनके पीछे वित्तीय संस्थाओं और बड़े बैंकों की क्या भूमिका रही है, इसे बहुत विस्तार से बताया गया है. सरकारों के साथ इनके गठजोड़ के लगभग सभी आयामों को विस्तार से बताया गया है. यहां एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा.
‘मैकनमारा’ का पहला परिचय यह है कि वह ‘फोर्ड मोटर्स’ के डायरेक्टर थे, उसके बाद वे अमरीका के ‘डिफेंस सेक्रेटरी’ हुए. वियतनाम युद्ध की नीेंव इन्हीं के समय पड़ी और अन्त में वे विश्व बैंक के डायरेक्टर हुए. अपने देश में भी हम इसे आज आसानी से देख सकते हैं. ‘चिदम्बरम’ भारत के वित्त मंत्री बनने से पहले वेदान्ता कम्पनी के डायरेक्टरों में से एक थे और वेदान्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रह चुके थे.
‘वेदान्ता’ कम्पनी का विस्तार से वर्णन करते हुए लेखक ने बताया है कि वेदान्ता को ’लंदन स्टाक एक्सचेन्ज‘ में रजिस्टर कराने में ‘जेपी मार्गन’ जैसी वित्तीय कम्पनी की बड़ी भूमिका है. लेखक ने साफ किया है कि आज वेदान्ता, टाटा, बिडला जैसी बड़ी कम्पनियां साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी की गिरफ्त में हैं. इसी संदर्भ में लेखक ने बताया है कि वेदान्ता भारत में जो खनन कार्य कर रही है, उसके लिए उसे ‘जेपी मार्गन’, ‘डच बैंक’, ‘एचएसबीसी’, ‘आइसीआइसीआइ’, ‘सिटी ग्रुप’ से मदद मिल रही है. ये सभी दुनिया की बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं.
वेदान्ता उड़ीसा में जो गैरकानूनी तरीके अपना रही है, वह तो ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन लेखक ने दिखाया है कि यह उसकी पुरानी कार्यपद्धति है. ‘हर्षद मेहता प्रकरण’ में भी वेदान्ता की पूर्ववर्ती ‘स्टारलाइट’ कम्पनी का हाथ था. इसके अलावा लंदन स्टाक एक्सचेंज में रजिस्टर होने के लिए इसने झूठी रिपोर्ट लगायी. ऐसे उत्पादों को अपनी कम्पनी का उत्पाद दिखाया जो कम्पनी बनाती ही नहीं. वेदान्ता के एक डायरेक्टर ‘रजत भाटिया’ ने जब इस पर आपत्ति की तो अनिल अग्रवाल ने उन्हें निकाल दिया और धमकी दी कि ‘देखते हैं तुम इस धरती पर कैसे जिन्दा रहते हो.’ इस प्रकरण का बहुत ही दिलचस्प वर्णन लेखक ने किया है.
उड़ीसा सरकार, वेदान्ता द्वारा कानून के उल्लंघन पर क्या रुख अपनाती है, यह एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है. उड़ीसा में वेदान्ता को लीज पर जो जमीन दी गयी थी, उससे 10 हक्टेयर ज्यादा जमीन पर वेदान्ता ने कब्जा जमा लिया. पहले तो सरकार ने इसे नजरअन्दाज करने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा विरोध होने पर सरकार ने वेदान्ता पर महज 11000 रुपये का जुर्माना लगाया.
इसके अलावा यह भी एक तथ्य है कि नार्वे सरकार ने वेदान्ता को पर्यावरण के उल्लंघन के आरोप में अपनी ‘काली सूची’ में डाला हुआ है. और भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया जाने वाला ‘गोल्डेन पीकाक अवार्ड’ 2009 में किसी और को नहीं बल्कि इसी वेदान्ता को दिया गया. क्या विरोधाभास है !
इन कम्पनियों की सरकार में घुसपैठ का एक अन्दाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है – ‘रियो टिन्टो’ एक बड़ी बहुराष्ट्रीय खनन कम्पनी है. इसने उड़ीसा में लौह अयस्क निकालने के लिए बड़ी जमीन लीज पर ली हुई है. इस कम्पनी के वित्तीय डायरेक्टर ‘गे इलियट’ ने 27 जून 2006 को लंदन में ‘इण्डिया-यूके बिजनेस लीडर्स फोरम’ में एक भाषण दिया. इसमें उन्होंने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि उसे अपनी ‘नेशनल मिनरल पालिसी’ में क्या संशोधन करना चाहिए. बाद में जब ‘नेशनल मिनरल पालिसी’ पर ‘हुडा रिपोर्ट’ प्रकाशित हुई तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें गे इलियट के लगभग सभी ‘सुझावों’ को स्वीकार कर लिया गया था.
‘नवउदारवाद’ के इतिहास पर भी किताब में काफी विस्तार से प्रकाश डाला गया है. नवउदारवाद के जनक ‘फ्रेडरिक हाइक’ और उनके शिष्य ‘मिल्टन फ्रीडमैन’ के दर्शन की विवेचना करते हुए ‘चिली’ में इसके पहले प्रयोग की भी विस्तार से चर्चा की गयी है. नवउदारवाद में ‘शाक थेरेपी’ की भूमिका पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है, जिसे बहुत शानदार तरीके से ‘नोमी क्लेन’ ने अपनी पुस्तक ‘शाक डॅाक्ट्रिन’ में रखा है. ‘शाक थेरेपी’ का एक उदाहरण इण्डोनेशिया भी है.
इण्डोनेशिया में जैसे ही राष्ट्रवादी ‘सुकर्णो’ ने अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की और इस कोशिश में जमीन्दारी उन्मूलन की कोशिश की और इण्डोनेशिया को ‘आइएमएफ’ से बाहर निकाला, पश्चिमी ताकतों ने विशेषकर अमरीका ने वहां तख्तापलट करा दिया. 10 लाख लोगों के कत्लेआम के बाद नये शासक ‘सुहार्तो’ के नेतृत्व में इण्डोनेशिया अगले ही वर्ष 1966 में पुनः ‘आइएमएफ’ का सदस्य बन गया और उसे एक बड़ा लोन मिल गया. शाक थेरेपी सफल रही.
पुस्तक का एक पूरा चैप्टर ‘एनजीओ’ पर है. यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है. लेखक ने दिखाया है कि ज्यादातर एनजीओ यथास्थितिवाद के पोषक होते हैं और इस रुप में वे कम्पनी की नीतियों को जाने अनजाने लाभ पहुंचा रहे होते हैं. कुछ एनजीओ तो कम्पनी के ‘पीआर’ के रुप में भी काम करने लगते हैं जबकि कुछ एनजीओ जनता के आन्दोलन पर कब्जा करने और उसे नख दन्त विहीन बनाने का प्रयास करते हैं. एनजीओ के इतिहास को टटोलते हुए लेखक ने इसे औपनिवेशिक समय के ‘मिशनरियों’ से जोड़ा है जो उस समय की उपनिवेशवाद की नीतियों के तहत ही काम करते थे.
लेखक ने यहीं एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है. एक एनजीओ के माध्यम से वेदान्ता ने देश भर के वकीलों का एक सम्मेलन कराया. इस सम्मेलन में ‘अरिजीत पसायत’ ने भी हिस्सा लिया. बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इन्होंने वेदान्ता के खिलाफ एक मुकदमे में वेदान्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया. इस मुकदमें में मशहूर वकील ‘संजय पारिख’ जब ‘डोग आदिवासियों’ का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए तो जज अरिजीत पसायत ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया और एकतरफा फैसला सुना दिया.
भारत और दुनिया में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को बढ़ाने में भी इन कम्पनियों का बड़ा हाथ है. सच तो यह है कि अपने फायदे के लिए देश की पूरी की पूरी नौकरशाही को ये कम्पनियां भ्रष्ट कर देती है. इस संदर्भ में लेखक ने छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का दिलचस्प बयान उद्धृत किया है जो उसने एक खनन कम्पनी से घूस लेते हुए बोले थे- ‘पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं.’
इसके अलावा उड़ीसा के आदिवासी जीवन और उनकी समस्याओं को दर्शाने के लिए लेखक ने साहित्य का भी सहारा लिया है. उड़िया के मशहूर साहित्यकार ‘गोपीनाश मोहन्ती’ के उपन्यास ‘पराजा’ को कई बार उद्धृत किया गया हैं. इसी ‘पराजा’ उपन्यास में जब एक सरकारी कर्मचारी एक आदिवासी से पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है तो वह बोलता है कि मेरा धर्म ‘पहाड़’ है. प्रकृति से ये लोग इस रुप में एकात्म हैं.
आदिवासियों के अलग इतिहास को रेखांकित करते हुए लेखक आज उनके उपर हो रहे दमन को अशोक के कलिंग विजय से जोड़ता है. उस वक्त करीब 20000 आदिवासी मारे गये थे. उसके बाद अंग्रेजों के समय में कृत्रिम अकाल से उस वक्त की जनसंख्या का करीब एक तिहाई मौत के आगोश में समा गयी थी.
इसके अलावा यदि रोमिला थापर की माने तो कलिंग युद्ध के समय ही करीब 1 लाख लोगों को जबरन विस्थापित करके वहां ले जाया गया था, जहां उन्हें जंगल साफ करके उसे कृषि योग्य बनाने की जरुरत थी. जाहिर है यह कठिन काम उन्हीं से कराया गया. उड़ीसा में शायद यह विस्थापन की पहली दर्ज घटना है.
लेकिन किताब में कई बातें ऐसी भी हैं जो इसके समग्र प्रभाव को कम करती है और किताब की मूल विषयवस्तु के ही खिलाफ खड़ी हो जाती हैं. किताब में ‘एडम स्मिथ’ को अनेकों बार बहुत प्यार से याद किया गया है और उनकी एक अलग तस्वीर गढ़ने की कोशिश की गयी है. अर्थशास्त्र की सामान्य जानकारी रखने वाला छात्र भी इस बात को जानता है कि आज जो नंगा और लंपट पूंजीवाद है वो अपना दर्शन अपने गुरु ‘एडम स्मिथ’ से ही लेता है. ‘बाजार का गुप्त हाथ सब कुछ नियंत्रित कर लेता है और सरकार का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाये रखना है’ यह ‘ब्रहम वाक्य’ एडम स्मिथ का ही दिया हुआ है, जिसका शंखनाद आजकल अक्सर होता रहता है.
वर्तमान पूंजीवाद की इतनी रैडिकल आलोचना पेश करने के बाद भी लेखक का एडम स्मिथ से लगाव समझ से परे है. इसके विपरीत पहली बार पूंजीवाद की समग्र आलोचना पेश करने वाले ‘कार्ल मार्क्स’ का जिक्र महज 7 बार किया गया है और हर बार नकारात्मक अर्थ में. विशेषकर उनकी ‘स्टेज थ्योरी’ की आलोचना के अर्थ में. एडम स्मिथ की थ्योरी के आधार पर हम पूंजीवाद का कौन सा विकल्प गढ़ पायेंगे ?
लेखक की भारतीय दर्शन में काफी रुचि है. वेदान्ता कम्पनी के बहाने भारतीय दर्शन ‘वेदान्त’ और ‘अद्वैतवाद’ की काफी ‘रैडिकल’ ब्याख्या लेखक ने पेश की है और वेदान्ता कम्पनी के कार्य-व्यवहार को वेदान्त दर्शन के खिलाफ बताया गया है. कमोवेश इसी तरह का अप्रोच अरुन्धति राय का भी है.
वेदान्त, अद्वैतवाद और हिन्दुत्व को एक ही मानते हुए लेखक कहता है- ‘भारत में आदिवासियों के धर्म और हिन्दुत्व के बीच कोई फर्क नही है.’ पहली बात तो यह है कि इस किताब में इसकी चर्चा एकदम अनावश्यक है. लेकिन लेखक ने जब इस दर्शन की इतनी ‘रैडिकल’ ब्याख्या कर दी है तो यहां संक्षेप में कुछ बातें करना जरुरी है. सूत्र में कहे तो अद्वैतवाद पूरे विश्व की एकता की बात करता है. और यह एकता केद्रित होती है ब्राह्मण में, जो ‘परम ज्ञान’ है. इस रुप में यह समाज के सभी अन्तरविरोधों से इन्कार करता है. स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-दलित, आदिवासी-गैर आदिवासी…
संक्षेप में कहें तो यह शोषक और शोषित के बीच के अन्तरविरोधों से इंकार करता है. उस पर पर्दा डालता है. जाहिर है इन अन्तरविरोधों में जो शोषक की स्थिति में हैं उनके लिए यह दर्शन अनुकूल है. लेकिन जो शोषित की स्थिति में हैं और यथास्थिति तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह दर्शन प्रतिक्रियावादी दर्शन है. शंकराचार्य के इस प्रसिद्ध कथन ‘ब्रहम सत्यम जगत मिथ्या’ के पीछे की राजनीति यही है, चाहे आप इसे लेकर कितनी भी उलटबांसी कर लीजिए.
इसके अतिरिक्त लेखक के वर्णन से ऐसा लगता है कि भारतीय दर्शन में यही एकमात्र दर्शन मान्य है. वेदान्त दर्शन के मजबूत विरोधी ‘बुद्ध दर्शन’ और ‘चार्वाक दर्शन’ का लेखक ने कहीं जिक्र तक नहीं किया हैं. आदिवासियों के सर पर इस प्रतिक्रियावादी दर्शन को मढ़ना उनके साथ एक तरह का ‘अकादमिक अत्याचार’ ही है. आदिवासी और दलित कभी हिन्दू नहीं रहे हैं. उन्हें हिन्दू धर्म का हिस्सा बनाने का प्रयास बहुत बाद में शुरु हुआ है. सवर्णो द्वारा आदिवासी और दलित को हिन्दू बताना दरअसल उन्हें दूसरे धर्मों में जाने से रोकना और उन पर अपनी ‘कल्चरल हेजेमनी’ स्थापित करने का एक प्रयास है.
इतनी बृहद किताब में कुछ छोटी छोटी तथ्यात्मक चूक होना लाजिमी है. लेकिन एक जगह यह चूक काफी खटकती है. इण्डोनेशिया में सुहार्तो द्वारा तख्तापलट का जिक्र करते हुए लेखक ने बताया है कि इसमें 50,000 लोग मारे गये थे. लेकिन वस्तुतः इसमें 10 लाख लोग मारे गये थे. इण्डोनेशिया की सरकारी किताब में भी यह संख्या 85,000 बतायी गयी है. लेखक को यह 50,000 संख्या कहां से मिली, पता नहीं.
हालांकि यहां लेखक ने एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी दिया है कि इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप ने (जो नंदीग्राम में अपना केमिकल कारखाना लगाना चाह रहा था) 65-66 में हुए कत्लेआम में सुहार्तो का साथ दिया था.
कुल मिलाकर देश दुनिया से सरोकार रखने वालों के लिए यह एक अनिवार्य किताब है. हां, फेलिक्स पडेल के बारे एक रोचक तथ्य यह है कि वे ‘चार्ल्स डार्विन’ के पड़पोते के पड़पोते हैं. अभी यह किताब ‘ऑउट ऑफ प्रिंट’ है. जैसे ही इसका पीडीएफ मिलेगा, आप सबसे साझा किया जाएगा.
Read Also –
शापित कब्र के अंदर दस करोड़ लोग
काली-वार काली पार : दुःख, संघर्ष और मुक्ति की दास्तान…
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]