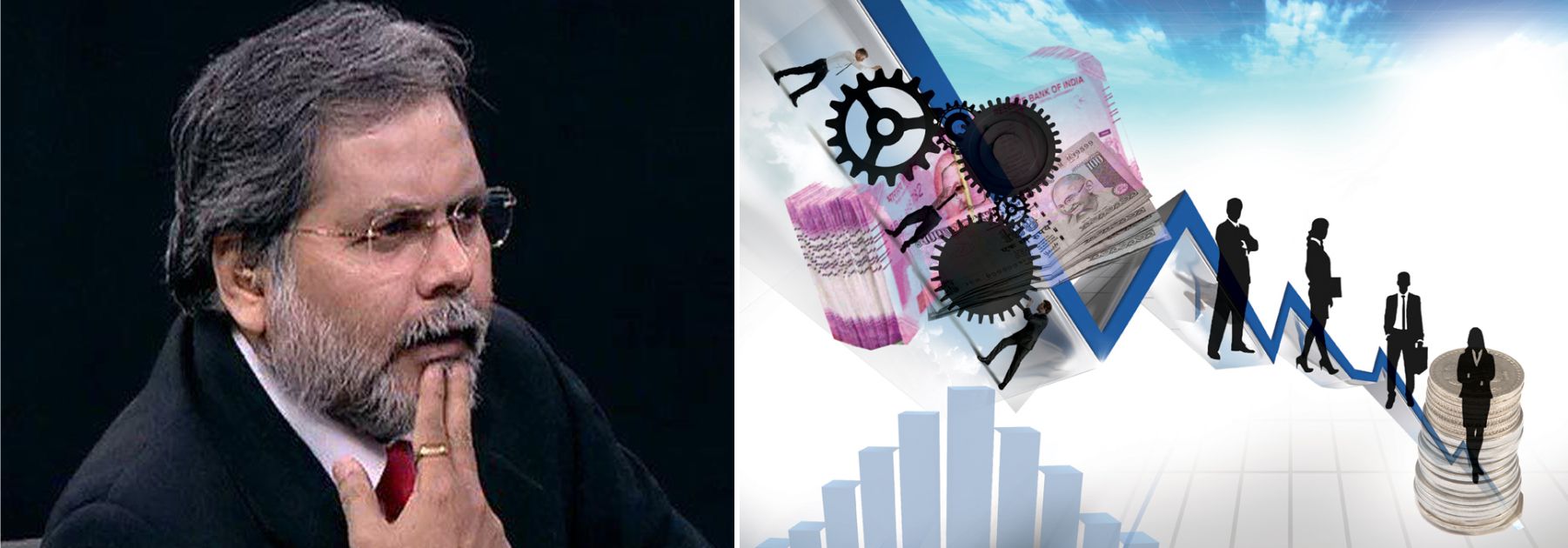
हो सकता है डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत का असर सरकार पर ना पड़ रहा हो और सरकार ये सोच रही हो कि उसका वोटर तो देशभक्त है और रुपया देशभक्ति का प्रतीक है क्योंकि डॉलर तो विदेशी करेंसी है. पर जब किसी देश की अर्थव्यवस्था संभाले ना संभले तो सवाल सिर्फ करेंसी का नहीं होता. और ये कहकर कोई सरकार बच भी नहीं सकती है कि उसके खजाने में डॉलर भरा पड़ा है. विदेशी निवेश पहली की सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा है. तो फिर चिन्ता किस बात की !
दरअसल किस तरह देश जिस रास्ते निकल पड़ा है, उसमें सवाल सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने भर का नहीं है. देश में उच्च शिक्षा का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि 40 फीसदी की बढ़ोतरी बीते तीन बरस में छात्रों के विदेश जाने की हो गई है. सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं बल्कि कोयला खादानों को लेकर सरकार के रुख ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि कोयले का आयात 66 फीसदी तक बढ़ गया है. भारत में इलाज सस्ता जरुर है लेकिन जो विदेश में इलाज कराने जाने वालां की तादाद में 22 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है. चीनी, चावल, गेहूं, प्याज के आयात में भी 6 से 11 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो गई है. और दुनिया के बाजार से कोई भी उत्पाद लाने या दुनिया के बाजार में जाकर पढ़ाई करने या इलाज कराने का मतलब है डॉलर से भुगतान करना.
तो सच कहां से शुरु करें. पहला सच तो शिक्षा से ही जुड़ा है. 2013-14 में भारत से विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों को 61.71 रुपये के हिसाब से डॉलर का भुगतान करना पड़ता था. तो विदेश में पढ़ रहे भारतीय बच्चों को ट्यूशन फीस और हास्टल का कुल खर्चा 1.9 बिलियन डॉलर यानी 117 अरब 24 करोड 90 लाख रुपये देने पड़ते थे. और 2017-18 में ये रकम बढकर 2.8 बिलियन डॉलर यानी 201 अरब 88 करोड़ रुपये हो गई और ये रकम इसलिये बढ़ गई क्योंकि रुपया कमजोर हो गया. डॉलर का मूल्य बढ़ता गया यानी डॉलर जो 72 रुपये को छू रहा है अगर वह 2013-14 के मूल्य के बराबर टिका रहता तो करीब तीस अरब रुपये से ज्यादा भारतीय छात्रों का बच जाता. पर यहां सवाल सिर्फ डॉलर भर नहीं है. सवाल तो ये है कि आखिर वह कौन से हालात हैं, जब भारतीय यूनिवर्सिटिज को लेकर छात्रों का भरोसा डगमगा गया है. तो सरकार कह सकती है कि जो पढ़ने बाहर जाते हैं उन्हें वह रोक नहीं सकते लेकिन शिक्षा के हालात तो बेहतर हुये हैं तो इसका दूसरा चेहरा विदेश से भारत आकर पढ़ने वाले छात्रों की तादाद में कमी क्यां आ गई ? इससे समझा जा सकता है.
रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट कहती है कि 2013-14 में जब मनमोहन सरकार थी तब विदेश से जितने छात्र पढ़ने भारत आते थे उससे भारत को 600 मिलियन डॉलर की कमाई होती थी. पर 2017-18 में ये कम होते-होते 479 मिलियन डॉलर पर आ गई. यानी कहीं ना कहीं शिक्षा अनुरुप हालात नहीं है तो फिर डॉलर या रुपये से इतर ज्यादा बडा सवाल तो ये हो चला है कि उच्च शिक्षा के लिये अगर भारतीय बच्चे विदेश जा रहे हैं और पढाई के बाद भारत लौटना नहीं चाहते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी या फिर वोट बैक पर असर नहीं पडता है, यह सोचकर हर कोई खामोश है.
क्योंकि आलम तो ये भी है कि अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जाकर पढने वाले बच्चों की तादाद लाखों में बढ़ गई है. सिर्फ अमेरिका जाने वाले बच्चों की तादाद मनमोहन सरकार के आखिरी दिनों में 1,25,897 थी जो 2016-17 में बढकर 1,86,267 हो गई. इसी तरह आस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में 35 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हो गया. 2014 में 42 हजार भारतीय बच्चे आस्ट्रलिया में थे तो 2017 में ये बढ़कर 68 हजार हो गये. लोकसभा में सरकार ने ही जो आंकडें रखे वह बताता है कि बीते तीन बरस में सवा लाख छात्रों को वीजा दिया गया. तो क्या सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपये की कम होती कीमत भर का मामला है क्योंकि देश छोडकर जाने वालां की तादाद और दुनिया के बाजार से भारत आयात किये जाने वाले उत्पादों में लगातार वृद्दि हो रही है. और इसे हर कोई जानता समझता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा तो आयल इंपोर्ट बिल बढ जायेगा. चालू खाते का घाटा बढ़ जायेगा. व्यापार घाटा और ज्यादा बढ़ जायेगा. जो कंपनियां आयात ज्यादा करती है, उनका मार्जिन घट रहा है.
विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ने लगा है क्योंकि दुनिया के बाजार में छात्रों की ट्यूशन फीस की तरह ही सरकार को भी भुगतान डॉलर में ही करना पडता है. और इन सब का सीधा असर कैसे महंगाई पर पड़ रहा है और सवाल मीडिल क्लास भर का नहीं है बल्कि देश में किसानों को सिंचाई तक की व्यवस्था ना कर पाने वाली अर्थवयवस्था या कहें इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के दावों के बीच का सच यही है कि 42 फीसदी किसान डीजल का उपयोग कर ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं. और महंगा होता डीजल उनकी सुबह-शाम की रोटी पर असर डाल रहा है.
तो महंगे हालात या कहें डॉलर के मुकाबले रुपये की चिंता तब नहीं होती जब भारत स्वालम्बी होता. सरकार ही जब विदेशी चुनावी फंड या विदेशी डॉलर के कमीशन पर जा टिकेगी तो फिर डालर की महत्ता होगी. क्या ये बताने की जरुरत होनी नहीं चाहिये. और ये सवाल होगा ही कि सरकार इक्नामी संभालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि चीन अमेरिका व्यापार युद्द में भी भारत फंसा. अमेरिकी फेडरेल बैंक ने ब्याज दर बढाई तो अमेरिकी कारोबारी उत्साहित हुये. भारत में डॉलर लगाकर बैठे अमेरिकी कारोबारी ही नहीं, दुनिया भर के कारोबारियों ने या कहें निवेशकों ने भारत से पैसा निकाला. वह अमेरिका जाने लगे हैं.
इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग लगातार बढ़ गई. यूरोपीय देशों के औसत प्रदर्शन से भी अमेरिका में निवेश और डॉलर को लगातार मजबूती मिल रही है. और इन हालातां के बीच कच्चे तेल की बढती कीमतों ने भारत के खजाने पर कील ठोंकने का काम कर दिया है. यानी ये सोचा ही नहीं गया कि इक्नामी संभालने का मतलब ये भी होता है कि भारत खुद हर उत्पाद का इतना उत्पादन करें कि वह निर्यात करने लगे. तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के जरिये दुनिया को पाठ पढाने वाले भारत को आज विदेशी शिक्षकों तक की जरुरत पड़ गई. यानी कैसे सत्ता ने खुद को ही देश से काटकर देश से जुडे होने का दावा किया ये भी कम दिलचस्प नहीं है. लकीर महीन पर समझना जरुरी है कि गांव का देश भारत कैसे स्मार्ट सीटी बनाने की दिशा में बढ़ गया. और स्मार्ट सिटी बनाने के लिये जिस इन्फ्रास्ट्र्क्चर को खड़ा करने की जरुरत बनायी गई, उसमें भी विदेशी कंपनियो की ही भरमार है.
चीन ने अपने गांव को देखा. जनसंख्या के जरीये श्रम को परखा. अपनी करेंसी की कीमत को कम कर दुनिया के बाजारों को अपने उत्पाद से भर दिया. भारत ने गांव की तरफ देखा ही नहीं. खेत से फैक्ट्री कैसे जुडे ? खनिज संसाधनों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में कैसे लगाये ? उत्पादन के साथ रोजगार को कैसे जोडें ? इन हालातों को दरकिनार कर उल्टे रास्ते इकनामी को चला दिया, जिससे सरकार का खजाना बढ़े या कहे राजनीतिक सत्ता तले ही सारे निर्णय हो. उसकी एवज में उसी को पूंजी मिले. उसी पूंजी से वह चुनाव लडे. और चुनाव लड़ने के लिये रास्ता इतना महंगा कर दें कि कोई सामान्य सोच ना सके कि लोकतंत्र का स्वाद वह भी चख सकता है.
तो हुआ यही कि भारतीय मजदूर सबसे सस्ते हैं. जमीन मुफ्त में मिल जाती है. खनिज संपदा के मोल कौड़ियों के भाव है और इसकी एवज में सत्ता सरकार को कुछ डॉलर थमाने होंगे. क्योंकि ध्यान दीजिये देश की संपदा की लूट बेल्लारी से लेकर झारखंड तक कैसे होती है. और तो और भारतीय कंपनियां ही लूट में हिस्सेदारी कर कैसे बहुराष्ट्रीय बन जाती है. सब कुछ आंखों के सामने है पर ये कोई बोलने की हिम्मत कर नहीं पाता कि राजनीतिक सत्ता ने देश की इक्नामी का बेडा गर्क कर देश के सामाजिक हालातों को उस पटरी पर ला खड़ा किया, जहां जाति-धर्म का बोलबाला हो. क्योंकि जैसे ही नजर इस सच पर जायेगी कि रिजर्व बैंक को भी अब डॉलर खरीदने पड रहे हैं. और अपनी जरुरतों को लेकर भारत दुनिया के बाजार पर ही निर्भर हो चुका है तो फिर अगला सवाल ये भी होगा कि चुनाव जीतने का प्रचार मंत्र भी जब गुगल, ट्विटर, सोशल मीडिया या कहें विदेशी मीडिया पर जा टिका है तो वहां भी भुगतान को डॉलर में ही करना पडता है. तो तस्वीर साफ होगी कि सवाल सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ने या रुपये का मूल्य कम होने भर का नहीं है बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था ने सिर्फ तेल, कोयला, स्टील, सेव, मेवा, प्याज, गेहूं भर को डॉलर पर निर्भर नहीं किया है बल्कि एक वोट का लोकतंत्र भी डॉलर पर निर्भर हो चला है.
- पुण्य प्रसून वाजपेयी के ब्लॉग (http://prasunbajpai.itzmyblog.com/) से साभार
- (बोल्ड लाइनें हमारी ओर से है)
Read Also –
देश को सबसे ज्यादा कर्ज में डुबाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी
डॉलर से मुकाबले ढ़हता रूपया : तब से अब तक
रिलायंस समूह की दलाली में मोदी
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करे…]


