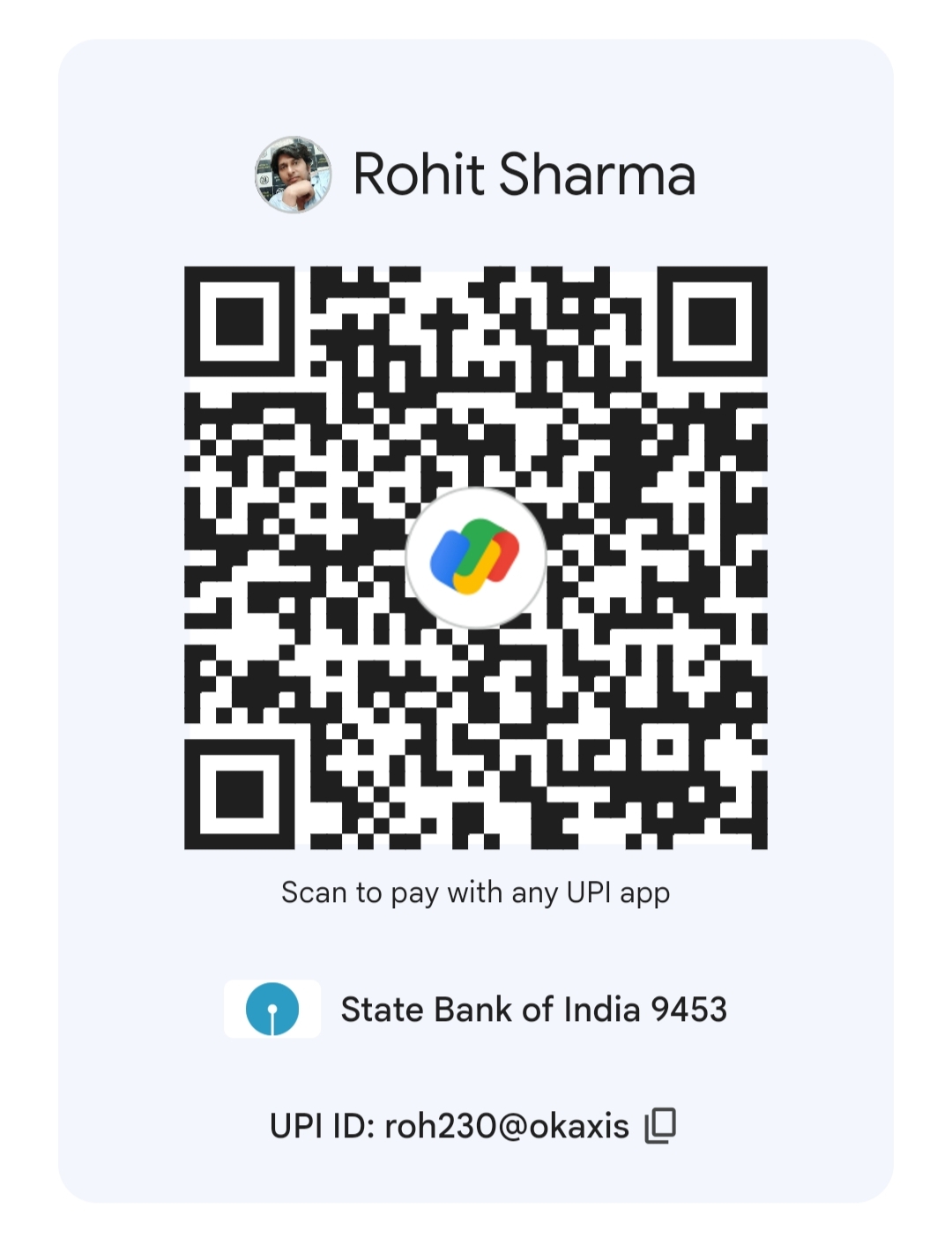भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी द्वारा ‘भारत देश में जाति का सवाल-हमारा दृष्टिकोण’ नामक दस्तावेज मई 2017 में जारी किया गया था. उसके बाद कुछ सीसी सदस्यों से और राज्य कमेटियों के सदस्यों से दस्तावेज पर कुछ सलाहों, व्याख्याओं और संशोधन केंद्रीय कमेटी के पास आए. भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी ने इस पर चर्चा की और जनवरी 2021 में इस ‘संशोधित दस्तावेज’ को जारी किया था, जिसके दूसरे अध्याय में बी. आर. आम्बेडकर पर चर्चा किया है. आज आम्बेडकर की जयंती के मौक़े पर हम इस आलेख को प्रकाशित कर रहे हैं. – सम्पादक

डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर (बी.आर. आंबेडकर) ने विपरित परिस्थितियों में अध्ययन करते हुए उच्च षिक्षा हासिल की। बचपण से ही जातीय उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार और अत्याचार को झेलते हुए वे बडे़ हुए. तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति और खुद भूक्तभोगी रहने के कारण स्वाभाविक रूप से ही जाति उनके अध्ययन का विषय बना. उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था पर प्रबंध लिखे. उन्होंने अर्थषास्त्र का भी गहन अध्ययन किया और प्रबंध लिखे.
महिलाओं को समान हक देने के लिए वे सतत प्रयत्नषील रहे. वे केवल लिखने तक ही सिमित नहीं रहे, बल्कि अपने अध्ययन के व्दारा उन्होंने जाति के विष्लेषण और निमूर्लन के लिए बताए रास्ते को धरातल पर उतारने के लिए तमाम दलित जनता को संगठित करने आगे बढ़े. उन्होंने अपने पूर्व में जाति के निमूर्लन के लिए कार्य किए सुधारकों को गुरू के रूप में स्विकारा. वे कहते थे उनके तीन गुरु हैंः गौतम बुध्द, कबीर और ज्योतिबा फूले.
महाराष्ट्र में आंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन उभरा. उन्होंने दलितों के अंदर अस्मिता का अलख जगाया और सम्मान से जीने के लिए संघर्ष करना सिखाया. उन्होंने दलित मुक्ति की आषा के साथ दलितों के हितों के लिए जिन सिद्धांतों पर उन्होंने भरोसा किया था, उनके मुताबिक आजीवन प्रयास किया. आधुनिक भारत के इतिहास में वे एक समाज सुधारक, अर्थषास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं भारत के संविधान के रचनाकार के ही रूप में विख्यात नहीं हुए थे बल्कि दलितों के स्वाभिमान का प्रतीक बन गए. वे एक सामाजिक क्रांतिकारी थे.
आंबेडकर का जीवन – राजनीतिक आचरण
भारत देश की जातियता की श्रेणी में सबसे निचली पायदान पर अतिशुद्र या दलित जातियां हैं. उन्हें जातीय उत्पीड़न की सबसे घिनौनी व अमानवीय प्रथा छुआछुत का सामना करना पड़ता. इन्हें अछूत कहा जाता. ये सामान्य ग्राम सेवक, खेत मजदूर थे. परंपरागत स्थाई पेशे के अभाव में तथा जातीय हिंसा और अत्याचार की वजह से दलित जातियों का गांवों से निरंतर पलायन होता रहा.
वे वहां जूट मिलों, रेल्वे, बंदरगाहों, सेना, रक्षा संबंधी कार्य एवं छोटे व्यापार आदि क्षेत्रों में आजीविका हासिल करते थे. इन्हें वहां अंग्रेजों की सैनिक व ईसाई मिशनरियों की शालाओं द्वारा शिक्षा के अवसर उपलब्ध हुए. इनसे दलितों के एक छोटे तबके पेटि बुर्जुआ वर्ग के रूप में विकसित हुआ. एक उल्लेखनीय तबका मजदूर वर्ग बन गया. महाराष्ट्र में दलितों में सबसे ज्यादा संख्या महार जाति की है. वे बड़े पैमाने पर शहरों में पलायन हुए और औद्योगिक मजदूर बने.
ब्रिटिश सेना में सूबेदार मेजर रैंक वाले की संतान आंबेडकर उस जाति के सबसे पहले स्नातक थे. उन्होंने 1906 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी. उसके बाद बरोड़ा महाराजा के यहां एवं कोलेज के प्रोफेसर के रूप में काम किए. फिर इंग्लैण्ड जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में आर्थिक मामलों पर एक प्रबंध लिखे. लंदन विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई पूरी करके 1923 में भारत देश वापस आए थे.
1920 के उत्तरार्द्ध में अछूतों के मानवाधिकारों के लिए, जाति निर्मूलन के लिए, अन्यों की तरह दलितों के लिए भी समान अधिकार हासिल करने के लिए, महिलाओं को समान अधिकारों के लिए एवं मजदूरों के अधिकारों के लिए किए गए कई संघर्षों में आंबेडकर सक्रिय रूप से शामिल होकर उनका नेतृत्व किया था. इन संघर्षों में प्रमुख थे, कोंकण इलाके के महाड में गांव के तालाब का पानी सभी जातियों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए 1927 में आयोजित महार सत्याग्रह, बड़ी महासभा, मनुस्मृति का दहन, 1928- 1930 के बीच में अमरावती एवं नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए किए गए संघर्ष. इनमें नासिक संघर्ष 5 साल तक जारी रहा.
इन जन संघर्षों ने दलितों के जुझारू युवा तबके को प्रेरित करके सभी दलितों को सामूहिक चेतना से लैस किया. इस संघर्ष ने दलितों को पशुवत देखने वाली समाज व्यवस्था के नियमों और परंपराओं को धुत्कारने का साहस पैदा किया और दलितों की अस्मिता को जागृत किया तथा समानता के सिध्दान्तों को एजेंडे पर ले आया.
इस पूरी कालावधि में डॉ. आंबेडकर ने ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को जनता के दो दुश्मन हैं, ऐसा कहते आए थे, बावजूद व्यवहार में वे ब्राह्मणवाद को प्रधान दुश्मन के रूप में लेकर काम किए थे. इन दोनों के खिलाफ एवं प्रतिक्रियावादी जाति व्यवस्था के खिलाफ कई सामाजिक आंदोलनों को और मजदूर आंदोलनों को संचालित करके सामाजिक और मजदूर आंदोलनकारी के रूप में डॉ. आंबेडकर ने एक मुख्य भूमिका निभाई.
उसके बाद उन्होंने जाति के सवाल पर सामाजिक सुधारों के लिए, जाति-निर्मुलन के लिए कोशिशें करते हुए ही प्रधानतया राजनीतिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से शुरू किया था.
1936 में आंबेडकर ने इंडिपेंडेण्ट लेबर पार्टी (आईएलपी) की स्थापना की थी. जिसका झंडा लाल था और उसके उपरी बायें कोने मे 11 स्टार थे जो तत्कालीन भारत के 11 प्रोव्हीन्स को दर्शाते थे. आईएलपी ने मजदूरों के हकों के लिए संघर्ष किए. कम्युनिस्टों एवं समाजवादियों के साथ मिलकर कपड़े मिल मजदूरों के हड़ताल किए. खोती प्रथा (कोंकण के भूस्वामी) के विरोध में आंदोलन किए. आंबेडकर ने जाति-विरोधी आंदोलन में महिलाओं को अनगिनत संख्या में गोलबंद की. उन्होंने जाति सहित लिंग उत्पीड़न का केंद्र हिंदूवाद के मौलिक नियमों पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि महिलाओं से संबंधित कुछ समस्याओं पर आंदोलन किए.
आंबेडकर के क्रियाकलापों का अधिकांश हिस्सा संघर्षों व जन गोलबंदी के लिए ही खर्च होने के बावजूद, ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी से दलितों के लिए सुविधाएं व रियायतें हासिल करने के लिए उन्होंने कोशिशें की. दलितों के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र, नौकरियों में आरक्षण एवं छात्रवृत्ति जैसी मांगें मुख्यतया उभरते दलित एवं मध्यम वर्ग की उन्नति एवं विकास के लिए मददगार थी.
इस क्रम में ही उन्होंने ‘स्वतंत्र’ भारत में वंचित वर्गों के हकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उनका प्रतिनिधी बनकर अधिकार स्थापित करने का निर्णय किए. क्योंकि गांधी खुद को ही कमजोर वर्गों का प्रतिनिधी बताकर नई व्यवस्था में वंचित वर्गों के हकों के साथ छल कपट कर रहे थे. ऐसी परिस्थितियों में 1928 में साईमन कमिशन में, 1930 एवं 1931 में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में आंबेडकर शामिल हुए थे.
दूसरा विश्व युद्ध जब छिड़ गया था, आंबेडकर ने फासीवाद के खिलाफ मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन, अमेरिका आदि देश) की निशर्त मदद दी थी. फरवरी, 1941 में उन्होंने वायसराय से भी मुलाकात करके ब्रिटिश सेना में दलितों को शामिल करने की मांग की थी. वायसराय द्वारा उनकी मांग स्वीकार किए जाने पर उन्होंने स्वयं विभिन्न इलाकों में जाकर दलित युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने प्रोत्साहित किया था.
उस वक्त वंचित वर्गो के लिए नौकरी प्राप्त करना आर्थिक, सामाजिक और उन्नति के दृष्टी से बहुत आवश्यक था, क्योंकि ब्राम्हणवादियों ने यह कहकर कि ‘महार या अस्पृष्य लड़ाकू जमात नही है’ अतः उन्हें सेना में भर्ती नही करना ऐसी शर्त भी अंग्रेजों से मनवा ली थी और अंग्रेजों ने दलितों को सेना में भर्ती करना बंद कर दिया था. विश्वयुद्ध के समय वह मौका आया जिसको आंबेडकर ने भाँपकर यह भर्ती फिर चालू करवा दी और दलितों को एक आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध करवाया.
आंबेडकर जब वे जुलाई, 1941 में ब्रिटिश इंडिया राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद के सदस्य एवं जून, 1942 में वायसराय कैबिनेट में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे, उसी समय में केन्द्रीय मंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने देश में कुछ श्रमिक कल्याणकारी कानूनों के बनने में मदद की. उसी तरह इस कालावधि में भी दलित-मध्यम वर्ग की सुविधाओं के लिए कोशिशें करते हुए कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 8.33 प्रतिशत आरक्षण एवं विदेशों में भारतीयों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां वे हासिल कर सके थे.
अंग्रेजों के चले जाने के बाद गठित होने वाले नई संवैधानिक व्यवस्था में कुछ हद तक जगह प्राप्त करने के उद्देश्य से इस दौरान आंबेडकर ने अपनी दिशा तय की थी. इसे ध्यान में रखकर 1942 में इंडिपेंडेण्ट लेबर पार्टी को रद्द करके दलित प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा करने के लिए शेड्यूल्ड कॉस्ट फेडरेशन (एससीएफ) का गठन किए थे. बाद में ‘स्वतंत्र’ भारत में नेहरु के मंत्रीमंडल मे कानून मंत्री बने. युद्ध के बाद भारत के दलाल पूंजीपति व सामंती वर्गों की सत्ता के संविधान के मसौदा कमेटी के चैयरमेन बनना स्वीकार कर उन्होंने भारत के संविधान की मौलिक रचना में प्रधान भूमिका निभाई.
संविधान समिति में जाना स्वीकारना एक ऐसा समय था जब उनको लग रहा था की उनके जीवन में रहते हुए दलितों के लिए कुछ न कुछ तरतुद करना जरुरी है. उनकी सेहत भी खराब हो रही थी. उनको लग रहा था कि उनके द्वारा शुरु किए आंदोलन की परिणिती किसी निर्णयात्मक ठोस उपलब्धी के बिना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए जब उनको संविधान लिखने का मौका आया तो उसे उन्होंने स्वीकार कर दलितों और आदिवासियों के लिए कुछ प्रावधान किए ताकि कल लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ते वक्त एक अधिकृतता (लेजीटीमसी) प्राप्त हो. फिर भी जब उन्होंने यह कार्य पूरा किया और मात्र उसके अमल के तीन साल बाद ही उन्होंने कहा की, यह संविधान दलितों को समानता नहीं दे सकता, मेरा कांग्रेस व्दारा इस्तेमाल हुआ है. इसे जलाने वाला पहला शक्स मैं ही रहुंगा.
1947 के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में आंबेडकर न्यायशाखा मंत्री बन गए. इस काल में वे भारतीय सेना द्वारा तेलंगाना के सशस्त्र जन संघर्ष पर अमल किए गए अमानवीय दमन के बारे में मौन रहे थे. 1951 में हिन्दू कोड बिल का अनुमोदन कराने की बात पर अड़े हुए आंबेडकर का विरोध करते हुए, उस बिल का विरोध करने वाली प्रतिक्रियावादी ब्राह्मणीय सामंती शक्तियों के पक्ष में नेहरू के खड़े होने के चलते उसके विरोध स्वरूप आंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था.
अपने जीवनकाल में हिन्दू धर्म पर एवं जाति पर आंबेडकर द्वारा किए गए शोध कार्य एवं विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण हैं. इन विषयों पर उन्होंने कई सैद्धांतिक रचनाएं की. लेकिन उन्होंने जाति की पैदाइश को लेकर सही निष्कर्ष नहीं निकाल सके. उसी तरह आंबेडकर ने जाति उन्मूलन के हल को शोषणमूलक सामाजिक संबंधों को ध्वस्त करने की बजाए हिन्दू धर्म से बौद्ध धर्म में धर्मांतरण के जरिए हासिल करने की कोशिश की. फलस्वरूप अपने निधन के कुछ समय पहले 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके दलितों को बौद्ध धर्म की ओर मोड़ दिया.
अपने जीवन की आखिरी समय में वे गंभीर अस्वस्थता का शिकार हुए. इस समय में औरंगाबाद एवं मुम्बई में महाविद्यालयों का निर्माण जैसे कार्यक्रमों को अपनाने के साथ ही वे कुछ सुधार कार्यक्रमों तक सीमित होते आए. इस समय में ही उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का समर्थन किया था.
आंबेडकर के प्रति हमारा राजनीतिक आकलन
आंबेडकर ने जातीय सीढ़ी में सबसे नीचे रहने वाले न केवल दलित जनता के समानता के लिए जुझते रहे बल्कि मजदूरों और महिलाओं के लिए भी उन्होंने संघर्ष संचालित किए. उनके दृष्टिकोण में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा को एकसाथ गुंफा हुआ समाज और भारत था. साम्राज्यवाद के बारे में उनकी समझ थी कि जब तक जमींदारों, मिल मालिकों और सूदखोरों जैसे देश के भीतर मौजूद साम्राज्यवाद के मित्रों के खिलाफ संघर्ष किए बगैर साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई असरदार युद्ध लड़ा जाना संभव नहीं. उन्होंने रणनीतिक तौर पर औपनिवेशिक शासन के बरअक्स तटस्थता बनाई रखी.
उनके अनुसार साधनहीन दलितों के लिए यह संभव नहीं था कि सभी ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ एक साथ लड़ पाए. कांग्रेस को वे बुनियादी तौर पर जमींदारों और शहरी पूंजीपतियों का प्रतिनिधि समझते थे. उनके साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध माने जाने पर सवालिया निशान लगाते थे. उन्होंने जाति व्यवस्था को हिंदू साम्राज्यवाद के रूप में आरोपित किया जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तुलना में दलितों के लिए निश्चित ही दुष्ट था.
आंबेडकर सही अर्थ में वंचित वर्गों के प्रतिनिधि थे. उन्होंने तमाम अस्पृष्य, उत्पीड़ित जातियों, दबे-कुचले लोगों और महिलाओं को एक वर्ग के रूप में संबोधित किया था. वे सभी दबे कुचले लोगों को ‘डिप्रेस्ड क्लास’ (वंचित वर्ग या दबे कुचले लोगों का वर्ग) कहते थे और मराठी में ‘दलित’ कहकर संबोधित करते थे. जाति व्यवस्था को वर्गीय दृष्टि से संगठित होकर ही तोड़ा जा सकता है, यह उनके डिप्रेस्ड क्लास की संकल्पना में था.
हालांकि उनका इन समूह को वर्ग के रूप में संकल्पित करना मार्क्स के वर्ग संकल्पना से अलग है. उन्होंने ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद यह भारत की शोषित जनता के दो दुश्मन है, ऐसा बार-बार कहा. उनके नेतृत्व में जन गोलबंदियों एवं जनांदोलनों में लाखों की संख्या में यह वंचित वर्ग शामिल हुए थे.
उनके द्वारा संचालित आंदोलन शुरुआत में सामाजिक एवं मानवाधिकारों के लिए, आत्मसम्मान के लिए थे, लेकिन बाद में दलितों, किसानों एवं मजदूरों और महिलाओं के जनवादी अधिकारों के लिए भी वो आन्दोलन हुए थे. यह सामंतवाद विरोधी संघर्षों के मुख्य हिस्से के रूप में संचालित कई जाति विरोधी संघर्षों का उन्होंने नेतृत्व किया. उस तरह वे और उनके नेतृत्व में जारी आंदोलन, जनवादी शक्तियों तथा आंदोलनों का एक मुख्य हिस्सा थे.
आंबेडकर ने प्रधानतया दलितों के हकों को हासिल करने और उनका कल्याण के लिए अपना जीवन को समर्पित किए. लेकिन दलितों के अधिकारों एवं उनके कल्याण के लिए उन्होंने मुख्यतः संसदीय जनवाद का दामन थाम लिया था. दरअसल यह रुख उन्हें जुझारू संघर्षों की राह से भटकाकर, उनमें संसदीय व्यवस्था के प्रति भ्रम पैदा किया. दूसरी तरफ उनकी सेवाएं 1941 के बाद की अवस्था में अंग्रेजी साम्राज्यवादियों, 1947 की बाद की अवस्था में दलाल नौकरशाही पूंजीपति-सामंती वर्गों के लिए इस्तेमाल हुई.
कुल मिलाकर देखा जाए, तो आंबेडकर ने जाति निर्मूलन को अपना जीवन लक्ष्य बनाकर यथासंभव हर अवसर को दलित और वंचित लोगों के हितों के लिए इस्तेमाल करने अपनी पूरी शक्ति के साथ ईमानदारी से कोशिश किए. आंदोलन के बारे में और रास्तों के बारे में वे हमेशा अन्वेषरत थे और बदलाव के लिए हमेशा तर्त्पर रहते थे. वे भारत की नवजनवादी क्रांति के व्यापक संघर्ष में ऐतिहासिक मित्रशक्ति थे.
इस दृष्टि से देखकर, समाज की परिवर्तन के लिए उनके सकारात्मक पहलू को लेना चाहिए. साथ ही क्रांति के रास्ते में अवरोध बनने वाले पहलुओं से बचना है. आंबेडकर के नेतृत्व में चला आंदोलन, उनका साहित्य निश्चित ही जाति निर्मूलन आंदोलन और जनवादी समाज के निर्माण में प्रेरणा देती है. उसे आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए. उसी समय में आंबेडकर को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वालों पर और उनके विचारों का गलत अर्थ निकालते हुए जनता को भटकाने वालों पर भी संघर्ष करना चाहिए.
आंबेडकर का जाति उन्मूलन सिद्धांत जनवादी समाज के निर्माण की दीर्घकालीन प्रक्रिया में एक प्रमुख हिस्सा तो है ही, लेकिन यही उसका अंत नहीं है. वह सिद्धांत पर्याप्त नहीं है. यह प्रक्रिया आंबेडकर के पहले भी जारी थी, अब भी जारी है. हमें इसे अंत ले जाना होगा. इसके लिए विशेषकर दलित मुक्ति के लिए मजदूर वर्ग के नेतृत्व में उत्पीड़ित वर्गों, दलित अन्यान्य उत्पीड़ित जातियों एवं अन्य उत्पीड़ित तबकों का संयुक्त व जुझारू संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है और वह नव जनवादी क्रांति ही है. इसे स्पष्ट रूप से देश की तमाम जनता के बीच हमारी पार्टी राजनीतिक रूप से लगातार प्रचार करते हुए उन्हें एक महान शक्ति के रूप में संगठित करना होगा.
लंबे समय से ही दलितों की समस्याओं के हल के लिए विभिन्न क्षेत्रों में असंख्य संगठन व संस्थाएं काम कर रही हैं. दलितों के नाम पर शासक वर्गीय, पेटि बुर्जुआई, जाति एवं उपजाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियां गठित होकर काम कर रही है. ये संगठन, संस्थाएं एवं पार्टियां सभी आंबेडकरवाद की मनमानी व्याख्या करते हुए उसे ही अपना सिद्धांत बता रही हैं. शासक वर्गीय दलित पार्टियों, मार्क्सवाद एवं हमारी पार्टी का विरोध करने वाले दलित संगठनों एवं संस्थाओं जो आंबेडकर का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, के शासक वर्गीय स्वभाव/शासक वर्गीय अनुकूल राजनीतिक अवसरवाद का जनता, खासकर दलित एवं अन्य उत्पीड़ित जातियों की जनता के बीच भंडाफोड़ करना चाहिए; उनके नेतृत्व को जनता से अलग-थलग करना चाहिए.
अन्य आंबेडकरवादी, दलित संगठनों व संस्थाओं को व्यापक जनवादी आन्दोलन में खड़ा करने के लक्ष्य से उनके साथ दोस्ताना रुख अपनाकर उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए. पार्टी को उनके आंदोलनों का समर्थन करना है. हमारे साथ जोड़कर संघर्ष करना चाहिए. उसी समय दलित जन समुदायों की मुक्ति के लक्ष्य से हमें स्वतंत्र रूप से दलित समस्याओं पर व्यापके आधार के साथ मजबूत आंदोलनों का निर्माण करना चाहिए और संगठनों को गठित करना चाहिए.
आंबेडकर का सिद्धांत
आंबेडकर सैद्धांतिक रूप से मार्क्सवाद के विरोधी नहीं थे. उन्होंने मार्क्सवाद का यथासंभव प्रचार किया. उनका कहना था कि यदि कोई फिलॉसॉफी उनके नजदीक है तो वह मार्क्सवाद है. लेकिन वे ‘लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स’ में पढ़ाई के दौरान देवे फेबीयनवाद से प्रभावित थे. इस तरह के सैद्धांतिक विचारधारा को व्यवहारवाद (pragmatism) या कारणवाद (instumentalism) कहा जाता है. कारणवादी को वैज्ञानिक विचारधारा की मान्यता है.
आंबेडकर ने जो प्राग्माटिस्ट दृष्टिकोण अपनाकर व्यवहार में लागू किया, जिससे ‘जाति उन्मूलन’ से संबंधित सामाजिक और आर्थिक बुनियाद को महत्व नहीं दिए. इस सवाल पर उन्होंने यह समझदारी को सामने रखा कि धर्मशास्त्रों को मान्य श्रद्धाओं का स्वाभाविक परिणाम यानी जाति है. जिस धर्मभावनाओं पर जातिभेद आधारित है, वह धर्मभावना नष्ट करना यह जातिभेद नष्ट करने का मार्ग है.
इस तरह जाति के उद्भव के लिए भारतीय समाज के प्राचीन उत्पादन संबंध कारण नहीं बल्कि हिंदू धर्म है, ऐसी गलत समझदारी सामने लाए. इसके फलस्वरूप उन्होंने यह आशा की कि सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की बजाए, हिन्दू धर्म को सुधारने के जरिए जाति का उन्मूलन कर सकते हैं. इसी कारण से वेदों को रद्द करने, तमाम हिन्दुओं के लिए मान्य एकमात्र मानक हिन्दू धार्मिक ग्रंथ बनाने, सभी जातियों के लिए लागू होने के हिसाब से परीक्षाएं आयोजित करके तद्वारा धर्मगुरुओं की नियुक्ति करने के कानूनों को प्रस्तावित किए. उन्होंने यह माना कि अंतरवर्णीय विवाह ही जाति उन्मूलन का अंतिम हल है.
इस तरह उन्होंने यह भ्रम प्रचारित किया कि मनुष्य की सोच-विचारों में बदलाव के जरिए ही जाति व्यवस्था रद्द हो सकती है. हालांकि अंतरजातीय विवाहों को निरंतर प्रोत्साहित करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि जाति की सामाजिक व आर्थिक बुनियाद को ध्वस्त किए बगैर जाति व्यवस्था के उन्मूलन में वे सिर्फ आंशिक रूप से ही मदद करती हैं.
वे यह नहीं बता सके कि भारत में इस्लाम, ईसाई, सिक्ख धर्मों, आखिर बौद्ध धर्म में भी अलग-अलग रूपों में जाति क्यों मौजूद है ? इसका जवाब उनके द्वारा प्रस्तावित हिन्दू धर्म का सुधार या बाद में उनका धर्मांतरण भी नहीं दे सका. इसलिए अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म में अपना जो धर्मांतरण किया था, वह सहज ही जाति व्यवस्था से मुक्ति का मार्ग दिखा नहीं सका.
इसके अलावा जातीय सांप्रदायिकवादियों के खिलाफ उनके द्वारा अपनाए गए संघर्ष में ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी पर उल्लेखनीय स्तर पर उन्हें निर्भर बनाया. उन्होंने यह माना कि चूंकि अंग्रेज पश्चिमी ईसाई धर्मावलंबी हैं इसलिए वे हिन्दू जाति सिद्धांत के खिलाफ रहेंगे. वे आचरण में यह देखने में विफल हो गए थे कि हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्यवादी, सामंती सनातन ताकतों पर आधारित होकर अपने शोषण व दमनकारी नीतियों को जारी रखे हुए थे.
आखिर, आंबेडकर की बुर्जुआ उदारवादी सोच के चलते राज्ययंत्र के स्वाभाव के बारे में उनके अंदर गलत समझ बनी थी. इस बुर्जुआ सिद्धांत कि राज्यसत्ता तटस्थ है, पर विश्वास करते हुए उन्होंने उसे एक दमनकारी साधन के रूप में एवं उसके वर्ग स्वभाव को चिह्नित करने से इनकार किया.
इसके चलते वे यह सोचते थे कि कानूनों में बदलाव एवं संवैधानिक सुधारों के जरिए राज्ययंत्र के चरित्र को बदल सकते हैं. हालांकि ‘स्वेच्छ, समानता, भाईचारा’, इन बुर्जुआ जनवादी उसूलों से प्रेरणा हासिल करने के बावजूद बुर्जुआ जनवाद के मूलभूत चरित्र – तानाशाही चरित्र को वे चिह्नित नहीं कर सके. विषेषकर साम्राज्यवाद एवं उसके ताबेदार सामंतवादी, दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग के राज्ययंत्र के प्रतिक्रियावादी चरित्र को वे चिह्नित नहीं कर सके. नतीजतन वे सामाजिक बदलाव लाने के लिए प्रधानतया कानूनों, कोर्टों, संसद व संविधान पर ही निर्भर रहे.
केन्द्र में सत्तारूढ़ ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा के साथ-साथ शासक वर्गीय व संशोधनवादी पार्टियां आंबेडकर के प्रति दलितों एवं अन्यान्य उत्पीड़ित जातियों की जनता में मौजूद असीमित मान्यता को ध्यान में रखकर अपने स्वार्थ हित साधने के लिए उन्हें भारत के संविधान के निर्माता, संसदीय जनवाद के प्रदाता के रूप में एवं विचारधारा के तौर पर उन्हें हिंसा व क्रांति के विरोधी के रूप में अविराम प्रचारित कर रहे हैं. ये तमाम पार्टियां एक से बढ़कर एक आंबेडकर के कथन के रूप में यह प्रचारित कर रही हैं कि क्रमिक बदलावों व जनवादी तौर तरीकों के जरिए दलितों को अपने जीवन सुधार के लिए संयम के साथ कोशिश करनी चाहिए.
इस तरह तमाम शोषक वर्गीय पार्टियां आंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करते हुए दलितों को बुर्जुआ, पेटि बुर्जुआ सुधारों तक सीमित रखते हुए जुझारू वर्ग संघर्षों से उन्हें दूर करने के लिए एवं नव जनवादी क्रांति में संगठित होने से रोकने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं. देश में 1947 के बाद, अभूतपूर्व स्तर पर ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी संघ परिवार के एजण्डे के अनुरूप मोदी सरकार राज्ययंत्र एवं ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी जाति दुरहंकारी शक्तियों का फासिजीकरण कर रही है.
एक तरफ मोदी सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारें क्रांतिकारी आंदोलन पर चौतरफे हमले को तेजी से जारी रखी हुई हैं तो दूसरी तरफ राज्ययंत्र की मदद से संघ परिवार की शक्तियां दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, धर्म निरपेक्ष, जनवादी एवं क्रांतिकारी’ शक्तियों पर सैद्धांतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व भौतिक हमलें जारी रखी हुई हैं. इन फासीवादी सरकारों व ताकतों के साथ समझौताविहीन संघर्ष करने वाली क्रांतिकारी शक्तियों, अन्य जुझारू शक्तियों पर अत्यंत क्रूर दमन अमल कर रही है.
ये फासीवादी ताकतें, अन्य आंदोलनों की ताकतों को लालच देकर या डरा धमकाकर अपने वशीभूत करके देश की जनता को गुलामी में धकेलकर उन्हें बेरोकटोक शोषण व उत्पीड़न का शिकार बनाते देख रहे हैं. इस परिप्रेक्ष्य में ही मोदी की नेतृत्ववाली भाजपा सरकार आंबेडकर को आसमान तक ऊंचा उठाते हुए उनके 125वीं जयंती समारोह का शानदार ढंग से आयोजन किया.
सत्ताधारी वर्ग द्वारा उनके हित के लिए बनाए गए इस आंबेडकर के प्रतीक को हमें बेनकाब करना चाहिए और आबेंडकर को व्यापक जनवादी संघर्ष के हथियार के रूप में लेने के लिए जरूरी है कि उन्हें सत्ताधारीाा वर्ग के दुर्ग से बाहर निकालकर, उनके सही प्रतीक के रूप में देखना है, जिसके लिए उनका जीवन अर्पित था.
Read Also –
अंबेडकर की वैचारिक यात्रा को कैसे समझा जाए ?
(संशोधित दस्तावेज) भारत देश में जाति का सवाल : हमारा दृष्टिकोण – भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ संविधान, सत्ता के बंटवारे पर आकर अटक गई
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लॉग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लॉग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]