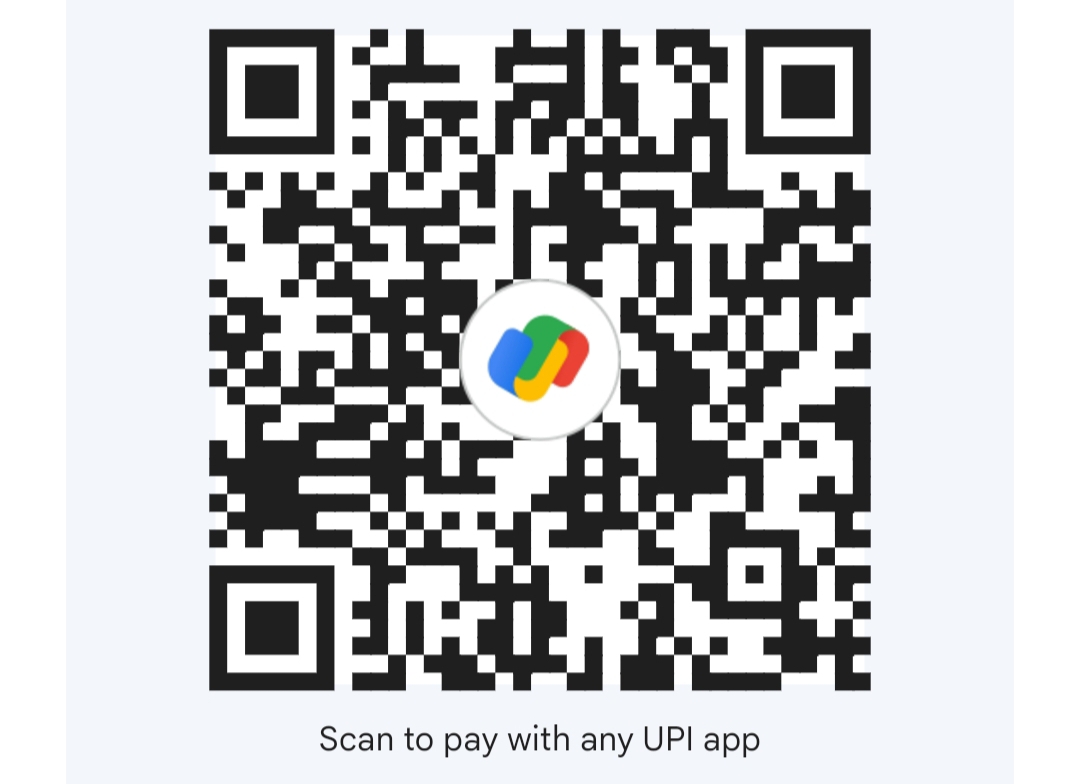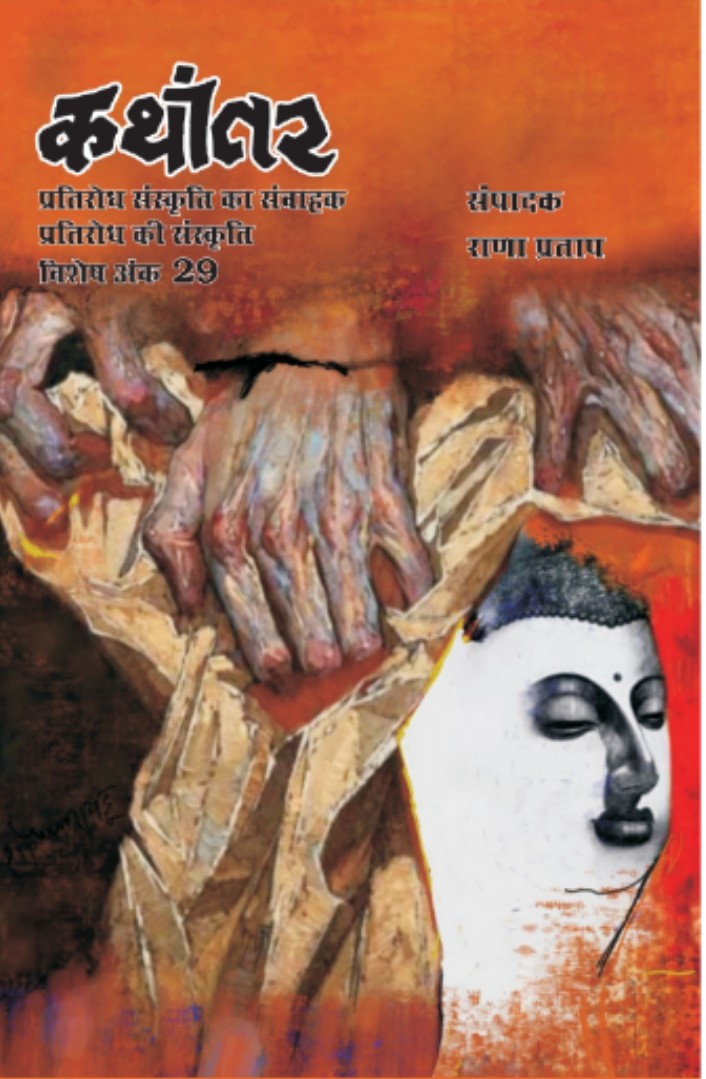‘कथांतर’ का ‘प्रतिरोध की संस्कृति’ विशेषांक : संस्कृति की जन पक्षधारिता
प्रोफेसर राणा प्रताप के संपादकत्व में पटना से प्रकाशित ‘कथांतर’ का प्रतिरोध की संस्कृति विशेषांक मेरे हाथों में है. राणा जी के कथांतर विशेषांक प्रेरक ज्ञान और जानकारियों की दृष्टि से करिश्माई होते हैं. विशेषांक की विषय वस्तु, लेखकों का चयन, सामग्री की विविधता, भाषा और उनका खुद का संपादकीय अद्भुत होता है, जो मन और दिमाग की गहराइयों को स्पर्श करता है.
वह अपने इस काम को इतने मिशनरी अंदाज से डूब कर करते हैं कि कथान्तर का हर विशेषांक एन्सैक्लोपीडियक होने के कारण पठनीय एवं संग्रहणीय होता है. उसमें विशेषज्ञों की वैचारिक स्थापनाएं और विश्लेषण शोधपरक होते हैं. उम्र की तमाम चुनौतियों को स्वीकारते हुए राणा जी अपने इस बौद्धिक और रचनात्मक मिशन में पूरी प्रतिबद्धता और तल्लीनता से लगे हैं और हमें प्रेरित करते हैं.
इस अंक में संस्कृति के विविध पहलुओं और प्रतिरोध की संस्कृति के औचित्य पर जिन विद्वान लेखकों नें अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनके नाम हैं, फा. जार्ज एन. डेविस, ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद, जितेन्द्र भाटिया, रामविलास शर्मा, आनंदस्वरूप वर्मा, अमिल्कर कबारल, गोपाल नायडू, ऋतिक घटक, लू शुन, विजय गुप्त, तुषारकांत, माओत्से तुंग, ओ. पी. जयसवाल, दिपांजन सिन्हा, प्रकाश चंद्रायन, नारायण सिंह, अनुज लुगुन, विजय शर्मा, शैलेन्द्र शांत और बतौर संपादक स्वयं राणा प्रताप.
राणा जी अपने संपादकीय में लिखते हैं कि जब भी संस्कृति की राजनीति पर वाद विवाद की शुरुआत होती है, तब हम सहमत होते हैं कि संस्कृति की अपनी राजनीति होती है. संस्कृति सदैव जन पक्षधर होती है. आप कितना भी नाक भौँ सिकोड़े संस्कृति की राजनीति से बच कर निकल नहीं सकते हैं. या तो आप भाड़े के टट्टू बन कर उपभोक्ता सांस्कृतिक (महाजनी संस्कृति) से जुड़ेंगे या फिर स्वतंत्र होकर जन-गण के गीत गायेंगे. बीच का कोई रास्ता नहीं होता. यही कारण है कि संस्कृति को छुईमुई बताने वाले कलावादियों की चीख पुकार अब बेअसर होने लगी है.
संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी उत्प्रेरण शक्ति. वह लेखकों और कलाकारों को सृजन के लिए उत्प्रेरित ही नहीं करती बल्कि प्रतिरोध की संस्कृति से जोड़ती भी है. वर्चस्ववादी संस्कृति के विरुद्ध डट कर खड़ा होने के लिए प्रेरित भी करती है. संस्कृति के भीतर प्रतिरोध की क्षमता अन्तर्निहित होती है, उसे सिर्फ पहचानने और उभारने की जरूरत है. एक नोबेल पुरस्कार विजेता कवयित्री विस्साव शिम्बोस्का की कविता कुछ पंक्तियों के जरिये राणा जी कहते हैं, ‘हमारी त्वचा का रंग राजनैतिक है / हमारी दृष्टि का कोण राजनैतिक है / हमारे, तुम्हारे और उसके मसले राजनैतिक हैं.’
फा. जा. एन. डेविस अपने लेख में लिखते हैं कि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त समग्र मानवीय मूल्यों का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने और कार्य शैली में निहित होता है. मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म दर्शन और विज्ञान होते हैं. सौन्दर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु आदि कलाओं तक पहुंचते हुए उन्हें उन्नत करता है. इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक कृति, संस्कृति का अंग बनती है. संस्कृति यानी कल्चर अर्थात कल्टीवेट करते हुए निरंतर परिष्कृत करना सुधारना, सजाना, सुन्दर बनाना, सर्जना जो मनुष्य के सुख का एक मात्र स्रोत है.
ई. एम. एस. नम्बुदरीपाद अपने लेख में लिखते हैं कि उत्पादन के मोर्चे पर सर्वहारा की एकजुटता ही संस्कृतिक मोर्चे पर एकजुटता कायम करेगी, जो एक जन संकृति का सृजन करेगी, जो असल सर्वहारा की संस्कृति होगी और उपभोक्तावादी संकृति को कड़ी टक्कर देते हुए उसे नस्तेनाबूद कर देगी.
मार्क्सवादी लेखक डा. रामविलास शर्मा अपने लेख में लिखते हैं कि फासिज्म सबसे पहले नागरिकता के अधिकारों को खत्म करता है, जनवादी विधान को नष्ट कर देता है और पूंजीवादी तानाशाही कायम करता है. इसलिए फासिज्म जनवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है और जन संस्कृति का भी. फासिज्म अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड, अवैज्ञानिकता फैला कर तर्कहीनता पैदा करता है ताकि जनता उसका भक्त बन सके और तानाशाह भय और दमन के जरिये निर्बाध शासन कर सके.
हम सबके प्रिय जनवादी प्रगतिशील बहुचर्चित लेखक आनंदस्वरूप वर्मा के विस्तृत लेख में संस्कृति के विविध पहलुओं पर वैश्विक दृष्टिकोण से रौशनी डाली गयी है. यह लेख प्रो. लालबहादुर वर्मा की स्मृति में 4 मई 2023 को दूसरे स्मृति दिवस पर आयोजित व्याख्यानमात्रा में दिये गये उनके व्याख्यान का सम्पादित अंश है. उनका मानना है कि संस्कृति में प्रतिरोध के बीज छिपे होते हैं. संस्कृति का कोई निरपेक्ष अस्तित्व नहीं होता है.
भारत सहित तीसरी दुनिया के वर्ग विभाजित समाज में संस्कृति दो प्रकार की होती है. एक संस्कृति शासन करने वाली शोषक वर्ग की और दूसरी शाशित और उत्पीड़ित वर्ग की, शाशक वर्ग जिन पर राज करता है. इतिहास गवाह है इन दोनों संस्कृतियों बीच हजारों वर्ष का संघर्ष है, जो आज भी चल रहा है. वर्गीय समाज में प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी परिघटनाओं का संबंध संस्कृति से होता है.
उनका यहां तक कहना है कि भारत में बीजेपी और आरएसएस के कट्टर और प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद के उदय के पीछे आर्थिक और राजनैतिक कारणों के साथ-साथ सांस्कृतिक कारण भी मुख्य है. इसके मूल में जन संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय तत्वों की विफलता है, जो उन मुद्दों को संबोधित नहीं कर सके, जिनसे जनपक्षीय चेतना और प्रतिरोध की संस्कृति का विकास होता है. इसलिए बदलाव के कार्य में लगे लोगों के लिए प्रतिरोध की संस्कृति को समझना आज एक मुख्य कार्यभार है.
जितेन्द्र भाटिया अपने लेख में लिखते हैं कि शासकीय अंकुश और एवं इतिहासकारों की सारी बेईमानी के बावजूद लगभग हर युग में साहित्य और दूसरी रचनात्मक विधाएं जन संस्कृति के बेहद करीब रही हैं. टेक्नोलोजी बनाम संस्कृति को इस भयानक त्रासदी के तह तक पहुंचने का एक मात्र रास्ता भी इन विधाओं के उदास चटक रंगों से होकर ही गुजरता है. सत्ता पक्ष यह भलीभांति जानता है कि लेखक के सबसे घातक हथियार अर्थात उसके शब्द और उन शब्दों का असर की काट उसकी तमाम मिसाइलों और आधुनिक हथियारों के पास नहीं है.
गिनी बिसाऊ के अफ्रीकन लेखक अमिल्कर कबराल्न ‘राष्ट्र मुक्ति और संस्कृति’ नामक व्याख्यान में जो उन्होंने 20 फरबरी 1970 को न्याूयार्क में एदुआर्दों मोंदालेन मेमोरियल्र लेक्चर में दिया था, में कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि किसी देश की जनता पर हुकूमत करने के लिए हथियारों से ज्यादा कारगर तरीका उनकी संस्कृति को या तो लकवाग्रस्त कर दिया जाय या बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय.
कारण यह है कि यदि देशज संस्कृति जीवन शैली के रूप में मौजूद रही तो साम्राज्यवादी शक्तियां कभी निश्चिन्त होकर शासन नहीं कर सकतीं. वह अपने व्याख्यान में बकायदे घोषणा करते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष कर रही जनता की संस्कृति संगठित राजनैतिक अभिव्यक्ति होती है. इसलिए आर्थिक विकास का जो भी स्तर हो, मुक्ति-आन्दोलन का नेतृत्व करने वालों पास संघर्ष के ढांचे के अंतर्गत संस्कृति के मूल्य की तथा जन संस्कृति की साफ़ समझ होना निहायत जरूरी है.
गोपाल नायडू अपने लेख ‘हिंसा के बरक्स कला’ में शुरुआत भगत सिंह के कोट से करते हैं, ‘गलत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आत्मिक बल का प्रयोग भी हिंसा की श्रेणी में आता है, वहीं किसी अच्छे उद्देश्य को हासिल करने के लिए शारीरिक और आत्मिक दोनों बलों का इस्तेमाल हिंसा नहीं कहलाती’.
आगे वह लिखते हैं कि राज्य सत्ता कभी जाति, कभी धर्म, कभी भाषा, कभी वर्चस्व, कभी रंग, कभी लिंग के आधार पर रूपांतरित होती रहती है. ये शक्तियां, एक दूसरे का समर्थन और अलगाव के अंतर्विरोधों की प्रक्रिया को अपने-अपने सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक हित में आसानी से इस्तेमाल्र कर लेती हैं. राज्य सत्ता के लिए ये शक्तियां हिंसा का हथियार हैं. यानी एक आक्रामक और दूसरी रक्षात्मक शक्ति है.
हिंसा के नैतिक, अनैतिक, धार्मिक, गलत या सही के नजरिये से देखने का तर्क हर काल खंड में एक चालाक व्यवस्था निर्माण करती रही है. हम इन्हीं अवधारणाओं में उलझे और फंसते रहे हैं. इस तरह राज्य सत्ता अपने हित के लिए परिस्थितियां और व्यवस्थाएं बनाती रहती है. अहिस्ता अहिस्ता मनुष्य के दिलों दिमाग पर कब्ज़ा कर सोच को नियंत्रित करती है. इसलिए जब भी कोई आंदोलन अपने प्रश्नों को लेकर उभरता है तब विकल्पहीन सत्ता के समक्ष इन समस्याओं का निदान सिर्फ हिंसा होती है. ये बदलाव समाज के अन्दर से ही उभरे हैं इसलिए इसका असर कला साहित्य पर भी आता है. जहां दमन है वहां प्रतिरोध है. जिस तरह हिंसा एक नैसर्गिक प्रक्रिया है तो प्रतिहिंसा उसके बाहर कैसे रहेगी.
देश में कम्युनिस्टों की कार्य शैली पर चिंता जाहिर करते हुए प्रगतिशील फ़िल्मकार ऋतिक घटक कहते हैं – कम्युनिस्ट होने के नाते हम जानते हैं कि कौन से जीवन मूल्य हमारे लिए अनमोल हैं. उन्हें अभिव्यक्त करना और जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है. हम यह भी जानते हैं कि जिस क्षण हम अपना काम शुरू करते हैं बुर्जुआ संस्कृति हमारे सामने खड़ी हो जाती है, जनता में जिसकी जड़ें गहराई तक व्याप्त हैं. इसलिए उस संस्कृति में जो भी अच्छा है और मनुष्यता से भरपूर है हमें स्वीकारना होगा.
महान चीनी लेखक लू शुन लिखते हैं कि क्रांति एक कड़ुवी चीज है. इसमें धूल और खून मिला हुआ है. यह वैसी प्यारी और सम्पूर्ण नहीं होती जैसा कि कवि वर्णित करते हैं. इसमें थकाने वाले काम होते हैं. बेशक क्रांति में विनाश किया जाता है, पर निर्माण उससे ज्यादा जरूरी होता है. जितना विनाश आसान होता है निर्माण उतना ही कठिन होता है. इसके लिए इसमें संयुक्त मोर्चे का गठन करना अपरिहार्य है.
विजय गुप्त अपने ‘साम्राज्यवादी संस्कृति’ लेख में लिखते हैं कि साम्राज्यवाद संस्कृतियों के बीच पारस्परिक सहमेल और सौहार्द मिटाने के लिए उन्हें आपस में लड़वाने के दुश्चक्र रचता है. नियोजित दंगे और हत्याकांड रचता है. उसे हम आज भी भारतीय सन्दर्भ में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं. हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई और आदिवासी भी इस लड़ाई में झोंके जा रहे हैं. झूठ को सच के रूप में पेश करना साम्राज्यवाद का बुनियादी चरित्र है.
तुषारकान्त अपने लेख ‘भारत में बौद्ध संस्कृति बनाम ब्राह्मण संस्कृति’ में लिखते हैं कि जैन और बौद्ध संस्कृति कोई आसमान से नहीं टपकी हैं बल्कि उभरती सामजिक वास्तविकताओं से उपजी हैं और उन्हीं का प्रतिबिम्बन करती हैं. इससे भी पहले आजीवक या लोकायत परम्परा बड़ी व्यापक रूप में भारतीय समाज में जड़े जमाये हुए थीं. बौद्ध संस्कृति ने ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ के मूल मंत्र के हर देश में जाकर वहां का चोला पहना. भारत में बौद्ध धर्म ने हर वर्ण और स्त्रियों के लिए अपने दरवाजे खोले. तर्क और विवेक सम्मत छुआछूत मुक्त समतापरक समाज के निर्माण के शुरुआत का पूरी दुनिया में स्वागत हुआ. भारत आज भी गाँधी और बुद्ध से जाना जाता है.
महान क्रन्तिकारी चीन के महानायक माओत्से तुंग अपने लेख ‘नव जनवाद की संस्कृति’ में लिखते हैं कि नव जनवादी संस्कृति साम्राज्यवाद विरोधी संस्कृति है. इस संस्कृति का नेतृत्व केवल सर्वहारा वर्ग और कम्युनिज्म विचारधारा ही कर सकती है.
दीपांजन सिन्हा अपने लेख में सोवियत संघ के उस स्वर्णिम काल को याद करते हैं जब तीसरी दुनियां के देश क्रन्तिकारी समाजवादी साहित्य से पटे रहते थे. भारतीय युवा मार्क्स, लेनिन और एंगेल्स के साथ साथ रूसी लेखकों जैसे मैक्सिम गोर्की, फ्योदोर दोस्तोवस्की, निकोलोई गोगोल, तुर्गनेव को पढ़ कर जन संस्कृति और क्रांति के भाव निर्मित होते थे.
प्रकाश चंद्रयान अपने लेख में लिखते हैं कि सामाजिक बदलाव के पक्षधरों की भाषा अलग होती है जो सामाजिक यथास्थितिवाद से कतई भिन्न होती है. क्योंकि शब्दों के तानबाने से ही जीवन के घटकों और सृजन की विधाओं के अस्तित्व और अस्मिता परिभाषित होती हैं और संस्कृति में किसी बदलाव की शिनाख्त करते हैं.
अनुज लुगुन ‘आदिवासी संस्कृति’ में अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखते हैं कि अमेरिका की जिस सभ्यता को आज एक शीर्ष सभ्यता के रूप में देखा जा रहा है, उसकी बुनियाद वहां बेगुनाह आदिवासियों के खून से सनी हुई है. इसलिए जल, जंगल और जमीन के आंदोलनों को हमें ठीक से समझने की जरूरत है, जो अस्तित्व और संस्कृति दोनों के बचाव की लड़ाई है.
सिनेमा में प्रतिरोध की संस्कृति का उल्लेख करते हुए विजय शर्मा कहते हैं कि प्रतिरोध की बात मन में आते ही आक्रोश और हिंसा के भाव उभरते हैं. इसी तरह प्रतिरोध के आंदोलनों को लेकर भी आम धारणा है. सिनेमा में भी प्रतिरोध के स्वर स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिस्थियों के कारण उभरे और भारतीय सिनेमा में आक्रोश, भूमिका, अर्ध सत्य के अतिरिक्त स्पेनिश फिल्म अगोरा, न्यूजीलैंड की दि पियानो, पोलिश फिल्म समर-43 जैसे तमाम फ़िल्में दुनिया के सिनेमाई परदे पर उभर कर आयीं, जिसमें मनुष्य को अपने पूरे समुदाय के लिए लड़ता हुआ लहूलुहान होते देखा गया.
अन्त में राणा जी अपने संपादकीय में लिखते हैं कि सच्चे जीवन के प्रत्येक चरण का अपना शब्द सूत्र होता है जो राजनीति के बगैर पूरा नहीं होता है. मुक्तिबोध ने कहा है, ‘ध्यान रखने की बात है कि एक कला सिद्धांत के पीछे एक विशेष जीवन दर्शन होता है और उस जीवन दर्शन के पीछे एक राजनैतिक द्रष्टि भी होती है.’ कथांतर का ‘प्रतिरोध की संस्कृति’ का यह विशेषांक पठनीय भी है और संग्रहणीय भी है.
- भगवान स्वरूप कटियार
Read Also –
सोया युवामन और कचड़ा संस्कृति
महात्मा बुद्ध, संस्कृति और समाज
संस्कृतियों का फर्क : सरहुल की शोभायात्रा में ‘पथराव’ क्यों नहीं होता कभी ?
गालियां और कु-संस्कृति : हम बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं
भारतीय सिनेमा पर नक्सलबाड़ी आन्दोलन का प्रभाव
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]