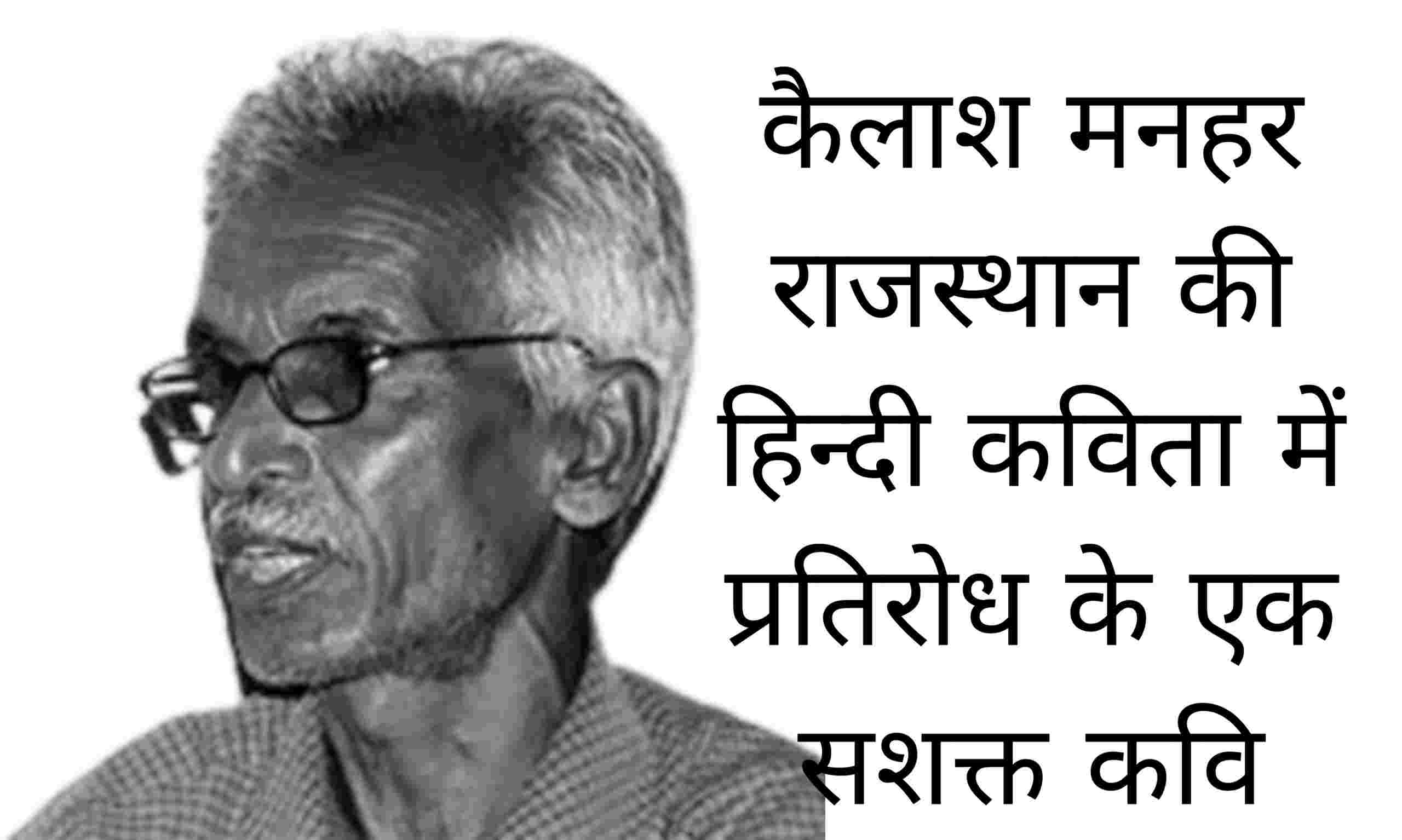
मिथ-कथाओं की बात करें कि प्रमाणिक सच का ? कि ऐतिहासिक दस्तावेजों से लबरेज़ इतिहास बोध की ? या फिर राजसत्ता के विरुद्ध मुखर प्रतिरोध की कविताओं की ही ? राजस्थान अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवटता का परिचय देते आया है. इस कड़ी में मीरा की धरती अपने साहित्यिक अवदानों से किसी भी स्तर पर कमतर नहीं उतरती. यानी, प्रतिरोधी आवाजों की विशाल परंपरा ने राजस्थान के साहित्यिक भूमि को कभी बंजर होने नहीं दिया, उसकी ऊर्वरता को बचाए रखी.
यह मैं राजस्थान के समकालीन हिंदी कविता और उसके प्रतिरोधी तेवर के कवियों की कविताओं के आधार पर कह रहा हूं, ना कि लकदक, सुसज्जित, सभ्य और कुलीन कविताओं के आधार पर. जबकि राजस्थान से आने वाले कई युवा कवियों की एक पूरी पीढ़ी इस समय सृजनशील हैं (जो यहां छूट रहे हैं), उनमें सतीश छिम्पा, माधव राठौड़, राहुल बोयल, अमर दलपुरा, देवेश पथ सारिया की सराहनीय उपस्थिति को लेकर फिर कभी बात की जाएगी.
खैर अभी राजसत्ता के प्रतिरोध में आवाज़ उठाने वाली कविताओं की बात मेरी प्राथमिकता में है. अतः मीरा की परम्परा का निर्वाह करते हुये कवियों में कन्हैया लाल सेठिया, मनुज देपावत, मदन डागा, नन्द चतुर्वेदी, मरुधर मृदुल और हरीश भादानी की कविताओं की जनपक्षधरता और वैचारिक प्रतिबध्दता को स्वीकार करते हुए मैं इस परम्परा का निर्वाह करने वाले कवियों में विजेन्द्र, ऋतुराज, राजाराम भादू, जुगमंदिर तायल, नन्द भारद्वाज, सवाई सिंह शेखावत, कृष्णकल्पित गोविन्द माथुर, विनोद पदरज, अम्बिका दत्त, अनुपमा तिवारी, प्रभात, किशन कबीरा के अलावा इसी वर्ष कन्हैया लाल सेठिया जन्म शताब्दी सम्मान से सम्मानित किए गए जनवादी तेवर के कवि कैलाश मनहर की बात करना मुझे लाज़िम लगा.
कहना न होगा कि कैलाश मनहर राजस्थान की हिन्दी कविता में प्रतिरोध के एक सशक्त कवि के रूप में पहचाने गए. कैलाश मनहर आठवें दशक की हिंदी कविता से आने वाले वे कवि हैं, जिन्होंने खूब लिखा. यहां तक कि आठ-आठ संग्रह प्रकाशित भी हुए किन्तु हिंदी के मुर्दा राजनीति के कारण वे वह स्थिति संभवतः हासिल नहीं कर पाए जिसका कि वे हकदार रहे हैं. बावजूद असल और महत्त्वपूर्ण यह है कि वे इससे बेपरवाह रह ठहरे नहीं, रूके नहीं बल्कि और अधिक बल तथा वेग से आगे आए. हिंदी में यह भी अपने तरह का एक साहसी और जैविक प्रतिरोध है, जो कैलाश मनहर में निखरता रहा.
कैलाश मनहर यूं तो प्रतिरोधी चेतना के कवि हैं और तेज़ तथा आक्रामक प्रतिरोध के साथ अपनी कविताओं में उपस्थित होते हैं. पर उनकी कविताओं में एक दूजा पक्ष भी है जो उनके काव्य विषय की वैविध्यता और अपने वैशिष्ट्य में भिन्न-भिन्न रूप, रस और गंध के तीखे आस्वाद में आता दिखाई देता है, यह उनके अन-सेलेक्टिव होने की वजह से है. यानी कि वे पक्षधरता के मामले में दायें बायें के पक्ष के इतर दोनों ही के नाकामियों को उजागर करते हैं. मसलन कि इस कविता को ही लें. इस कविता में वे दायें से अधिक निर्मम बाएं पर हैं. चूंकि दायें का क्रिया-कलाप जगजाहिर है परन्तु बाएं से ऐसा उम्मीद कभी नहीं किया जा सकता जैसा कि वे देख रहे हैं. इसलिए वे साफ और खरी-खरी में बाएं की आलोचना कर कहते हैं कि –
‘सच बोल कर
सुरक्षित रह सकने की
आज़ादी चाहिये उन्हें
जिसकी संभावनायें दूर-दूर तक नहीं
आशंकाओं से घिरा कवि
आत्मग्लानि में
डूब रहा है अभी’
बृहद मानव संघर्ष चेतना के दिमागी होने से कुछ भी नहीं होता ! जब भय और आशंकाओं से घिर कर सच को कह पाने का साहस क्षींण हो जाए. सच को सच के सरीखे कहने में कुवत और औकात का अतिक्रमण करना पड़ता है. कैलाश मनहर के कथन का वस्तुत: पर्याय यही है. यह कोरी बकैती के बजाय जैसा कि ‘भाषा को गाली देना बहुत आसान है’, वैसा सहज और सरल जीवन यथार्थ नहीं है. जीवन यथार्थ इसके उलट है, पर इधर उन थर्ड डिग्रीधारक कवि को –
‘कवि को चाहिये ऐसी भाषा कि
सुरक्षित रहे सच बोल कर’
यह संभव कम है. नतीजतन कैलाश मनहर कह ही रहे हैं ऐसा
‘कौन-सी भाषा में ऐसी सुरक्षा है कवि !’
अस्ल सवाल तो यह है कि
सुरक्षित रहा भी जा सकता है क्या
सच बोलते हुये वास्तव में कहीं
यदि इतनी ही चिन्ता है सुरक्षा
और सम्मान की तो फिर
सच बोलने की जरूरत क्या है कवि !’
कविता आत्मआलोचना और पुनः पुनः विचार करने के जरूरत पर बल देती है. सचेत करती है मुक्तिबोध के शब्दों में कि कुछ करना है तो वैसा ही – ‘अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ-गढ़ सब’ और ‘कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वातंत्रय व्यक्ति का वादी, छल नहीं सकता मुक्ति के मन को, जन को.’
सच बोल कर
सच बोल कर
सुरक्षित रह सकने की
गारंटी चाहिये उन्हें
जिसकी संभावनायें दूर-दूर तक नहीं
आशंकाओं से घिरा कवि
आत्मग्लानि में
डूब रहा है अभी
भाषा को गाली देना बहुत आसान है
कवि को चाहिये ऐसी भाषा कि
सुरक्षित रहे सच बोल कर
कौन-सी भाषा में ऐसी सुरक्षा है कवि !
अस्ल सवाल तो यह है कि
सुरक्षित रहा भी जा सकता है क्या
सच बोलते हुये वास्तव में कहीं
यदि इतनी ही चिन्ता है सुरक्षा
और सम्मान की तो फिर
सच बोलने की जरूरत क्या है कवि !
सुरक्षा सम्मान और सच
एक साथ नहीं पाये जाते हैं !
***
इधर बीते कुछ सालों में देश ने खूब विकास किया ! तथाकथित अनुयायियों की मानें तो असीमित, अपरीमित और अविश्वसनीय भी कह सकते हैं पर भक्ति भाव से भरे मूर्खता की हार सच के आगे सुनिश्चित है, हारता ही है वह ! कैलाश मनहर इस विकास के वादे-इरादे को शानदार साफ़गोई में कैसे दर्ज कर रहे हैं, देखा भी जाना चाहिए और माना भी चाहिए कि तथाकथित विकास फरार है. विकास के पक्ष में कि उसके ज़रूरत को भला कैसे अस्वीकारा जा सकता है.
यह एक मानवीय क्रिया व्यवहार है. न इसे कैलाश मनहर नकारेंगे और न कोई अन्य. परन्तु इधर, जितना भी विकास का गान गाया गया है उसके तह में जाएं तो एक भयानक सच उद्घाटित होता है, जिसके मुख्य घटक दलाल पूंजी, सत्ता और मीडियोकरी का गठजोड़ है. यह वस्तुत: छद्म है और इस छद्म को कैलाश मनहर इस कविता में सिरे से अस्वीकार रहे हैं. ऐसा हर समाजिक दायित्वबोध से सम्पन्न, मानव चेतस और प्रकृति प्रेमी प्राणी करता आया है. वह मेधा पाटकर हो कि अरुंधति राय या बाबा आमटे या फिर सुंदर लाल बहुगुणा, जिन्होंने ग्राउंड वर्क से अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया. कैलाश मनहर उसी परिपाटी में विकास के अर्थ को देखते हैं, समझते हैं. जो प्रतिकार दर प्रतिकार में गीतात्मक और और लयात्मक काव्य सौंदर्य सघन अनुभूतियों में उच्चारित होता है.
सच कहने से डरना क्या ?
भोग-लोभ के अंध-कूप में,
जान-बूझ कर मरना क्या ?
कब तक सहन करें, झूठों को,
सच कहने से डरना क्या ?
अपने पर्वत,अपनी नदियां,
अपनी धरती, अपने जंगल ।
पर विकास का कपट-ढोंग रच,
ऐश करे धनपति-शासक दल ।।
प्रकृति को ही नष्ट करे जो,
उस विकास का करना क्या ?
सब संसाधन गिरवी रखकर,
जो पूंजी निवेश करवाये ।
उस शासक का क्या यक़ीन यदि,
देश समूचा बेचे खाये ।।
पराधीन बन खाना-पीना,
सजना और संवरना क्या ?
***
उदासियों में खुशियां ढूंढ़ते रहने वाले कैलाश मनहर की कविता ‘मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में हूं’ एक मार्मिक कविता है. वे जिस आदमी के तलाश में हैं वह कहीं छिपता-छिपाता भागा नहीं है, वह उनके आसपास ही है और बिल्कुल करीब है. जो रोजमर्रा के जुटान में निबट अकेला है. वह हर दिन मरता रहा है, खपता रहा है और लौट आता है अगले रण के लिए रणभेदक बनकर.
वस्तुत: वह आदमी पतझड़ को झेला है, वसंत की मस्ती में झूमा है. उस आदमी की जितनी चिंतायें है उसके चिंताओं का आकाश उससे भी बड़ा है. बड़ी बात यह कि उसमें हर फिक्र को उंगली में रख उड़ा देने का सामर्थ्य है. यह माद्दा रखता आदमी सपने खुली आंखों से देखता है और जुटा रहता है अपने धुन पर इसीलिए ही झेल लेता है वह सूरज की कड़ी धूप या भयंकर शीत की भी परवाह नहीं करता.
वह आदमी परिश्रमी है. हाड़ तोड़ मेहनती है. वह आदमी मरूस्थल में भटकते हुए भी गाता जाता है कई-कई नदियों का गीत. कैलाश मनहर जिस आदमी की तलाश में हैं वह थेथर व चोंचल हुए वर्तमान के भोथरे अस्त्र पर आदिम संगीत का शान चढ़ाता है तो अपने कुवत और हुनर से.
कैलाश मनहर की कविता का यह लोकधर्मी रूप श्रम के सौंदर्य व संघर्ष से आते हैं. बताना न होगा कि कैलाश मनहर के तलाश में जीवन की संभावना के प्रति गहरी आस्था कूटकर भरी हुई है.
मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में हूं
मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में हूं
जो मृत्यु से मिलता हो प्रतिदिन
किन्तु लौट आता हो जीवन के पास
जो पतझड़ को झेलने के बाद
अचानक वसंत की मस्ती में झूमने लगे
मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में हूं
जो चिन्तायें करते हुये भी लगे निश्चिन्त
सपने देखने की आदत हो जिसे खुली आंखों
अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत हो
और झेल सके जो सूरज की कड़ी धूप
पुरवाई की उम्मीद में बहा सके अपना पसीना
मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में हूं
जो मरुस्थल में भटकते हुये गाता हो नदियों के गीत
जो भौंथरे हथियारों को धार दे सके
अपने ही सवालों में खोया हुआ जो
जानना चाहे मनुष्य की मुक्ति के जवाब
जो दुर्गम यात्राओं को सुगम बना सके
मैं किसी कवि की तलाश में हूं वाक़ई
मैं स्वयं की तलाश में हूं !
प्रतिरोध का अपना काव्य सौंदर्य होता है. एक, चीजों को दृश्य चित्रों में रख, स्थितियों-परिस्थितियों को आधारभूत ढांचा दे, माकूल जवाब की तैयारी करते रहना; जन को जगाए रखना. दूसरी, सीधे उग्र उद्घोष, लक्षित और चिन्हित के प्रति स्पष्ट-आक्रामक, अस्वीकार भाव. समकालीन हिंदी कविता में दोनों ही मौज़ू हैं. दोनों की अपनी व्यंजकता है. कैलाश मनहर के यहां पहले तरह का सौंदर्य और व्यंजना है पर यह खरी खोटी में न होकर लक्षित और चिन्हित व्यक्तिवादी केन्द्रिकता से परे है तथा चरित्र केन्द्रित है. इस तरह के काव्य रूझानों की अपीलिंग में तत्काल का प्रभाव कम पड़ते हैं और निरंकुश व्यवस्था बलशाली बने रह जाता है. इसका यह अर्थ भी नहीं कि ये महत्वहीन हैं !
देश के सिर पर बैठा है अपशकुनी कागा
स्वतंत्रता का चूहा घुसा हुआ है बिल में
लोकतंत्र नक्काली
करता है महफ़िल में
संविधान की नाव मरुस्थल में भटकी है
गलियारे में समानता की खाट खड़ी है
नहीं राज्य का रूप लोकहितकारी बिल्कुल
लूट रहे हैं मुल्क धनिक अरु नेता मिलजुल
तत्त्व नीति-निर्देशक सारे लुप्त हो चुके
सभी मूल अधिकार न जाने कहां खो चुके
नहीं धर्म-निरपेक्ष आचरण करता शासक
ले विकास का नाम बना है घोर विनाशक
श्रमिक सभी हैं दुखी ,
मज़े में पूंजीपति हैं
प्रगति हुई है विस्मृत गतियां सब दुर्गति हैं
देश के सिर पर बैठा है अपशकुनी कागा
सोचा तो सीने पर कोई दुहत्थड़ लागा
जाग रहा कवि किसे सुनाये मन का दुखड़ा
सच भूसे के ढेर में कच्चे सूत का टुकड़ा
***
क्रांतिकारी कवि वरवर राव पिछले दो सालों से जेल में बंद हैं और अस्वस्थ हैं. न्याय के पक्ष में हुंकार भरने की सजा काट रहे हैं. वरवर राव को समर्पित इस कविता में कैलाश मनहर की संजीदगी देखते बन रही है. वे कहते हैं एक कवि अपने तमाम रहमो-करम को छोड़ इस दुनिया से निरापद ही विरक्ति ले लेता है और एक कवि सत्ता की खुशफहमी से विरक्तावस्था में है. यह हमारे समय के सच की बयानी है. वह इन अर्थों में कि हिंदी जन के ही अनेक चिरकुटों का बयान इस बीच जैसा दिखा वह बेहद शर्मनाक था, जिसे कैलाश मनहर की बयानी और बानगी में देखा जा सकता है –
‘एक कवि कोसा जा रहा है
नफ़रत के सौदागरों द्वारा सरेआम
देश पर किसी का
एकाधिकार नहीं होने की बात कहने पर
और उधर एक कवि
टीपू सुल्तान की यादगार इमारत के सामने
उकड़ू बैठा है चप्पलें पहने’
सीधी सपाट अभिधा कम व्यंजना में, कैलाश मनहर इस कविता के माध्यम से उस संवैधानिक कुठाराघात की ओर इशारा कर रहे हैं, जो सत्ता के मद में चूर स्वमेव ही इमाम अथवा पैगंबर सा ब्रम्हवाक्य सुनाते विस्तारवाद के प्रचारकर्ता हैं.
लोकतंत्र की आवाज को दबाने का सीधा तात्पर्य है, अपवादी हो जाना. इसमें महत्वपूर्ण यह कि मनुष्यहंता सत्ता तो इस कविता के घेरे में है ही, वे भी हैं और सभी आए हैं जिन्होंने सृजनशीलता की खाल ओढ़े, प्रगतिशीलता का दंभ भरते अघाए नहीं अब तक और पिछले अथवा चोर दरवाजे से भी सत्ता की तीमारदारी में मशगूल हैं.
असहमति की आवाज़ में पहले पहल
फुसफुसाने वाले एक कवि का जन्मदिन है आज
जबकि एक कवि
दरबार में घुसपैंठ बनाने के लिये
लिख रहा है वीरतापूर्ण पाखण्ड का महाकाव्य
यहां उल्लेखनीय यह है कि वीरता के इस पाखंड को कैलाश मनहर अपने प्रगतिशील चेतना और मानवीय मूल्य बोध से धराशाई कर उसे औकात दिखाते नजर आते हैं –
आज ही चला गया कोई कवि अनन्त यात्रा पर
आज ही चला गया कोई कवि अनन्त यात्रा पर
जबकि एक कवि बहुत बीमार चल रहा है
इस अकाल में बहुत चहेता रहा जो संज़ीदगी से
एक कवि कोसा जा रहा है
नफ़रत के सौदागरों द्वारा सरेआम
देश पर किसी का
एकाधिकार नहीं होने की बात कहने पर
और उधर एक कवि
टीपू सुल्तान की यादगार इमारत के सामने
उकड़ू बैठा है चप्पलें पहने
असहमति की आवाज़ में पहले पहल
फुसफुसाने वाले एक कवि का जन्मदिन है आज
जबकि एक कवि
दरबार में घुसपैंठ बनाने के लिये
लिख रहा है वीरतापूर्ण पाखण्ड का महाकाव्य
अकेलेपन से घिरा हुआ अंधेरे में अपने
सिर के बाल नोंच रहा हूं मैं
किंकर्तव्यमूढ़ बना सवालों की अकड़ से
और कविता अभी तक सुलझाने में लगी है
समय का वायवीय संजाल
विकट कपट से गुंथा हुआ जो विरोधाभासी
दो वर्ष से एक कवि सरकार की क़ैद में है
शोषितों की आवाज़ उठाने के ज़ुर्म में
प्रताड़ित किया गया जिसे
और मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया जो
फिर भी उससे डरती है राष्ट्रवादी सरकार
***
एक प्रहरी का कार्य बहुत अधिक न होने के बाद भी बहुत बड़ा और जवाबदेही से भरा होता है. इधर बीते दिनों में हिंदी के प्रहरियों ने जवाबदेही को त्याग लोभ-लाभ, चमक-दमक का दामन थाम न सिर्फ राजनीति की बल्कि चेतना से भी विमुख हो पथविहीनता को अंगीकार किया. बताना न होगा कि कैलाश मनहर भी इस चरित्र के शिकार हुए, पर वे न रूके और न ठहरे. पथविहीन लोगों के राह की कांटे चुनने की दिशा में, एक सुघर प्रहरी की भूमिका का निर्वाह करते, निर्द्वंद ही अकेले निकल आए इसीलिए ही वे इस सौम्य और मृदुल रचना का सृजन बतौर सीख और चेतावनी के कर सके.
बेबाक और दो टूक में जवाबदेही तय करती कैलाश मनहर की इस कविता का जीवन तब तक का है, जब तक इस सुंदर धरती के प्रहरी अपने जवाबदेही से भागते रहेंगे और तब तक कैलाश न रूकेंगे न ठहरेंगे. उनका कंधा एक मजबूत आदमी का कंधा है –
ओ कवि
ओ कवि!कुछ तो तनना सीख
लालच में मत सनना सीख
सरकारी गुण गाना छोड़,
ख़ुद से भी कुछ ठनना सीख
जनता के दु:ख-दर्द भी देख,
अच्छा-बुरा समझना सीख
पूँछ हिला कर मालिक के,
टुकड़ों पर मत पलना सीख
मस्त-मलंगी जीवन जी,
अक्खड़-औघड़ बनना सीख
***
मिथ कथाएं अपने अप्रामाणिकता के कारण ही रहस्यमयी बनी हुई हैं. यद्यपि सतत् वैज्ञानिक विकास और पुरातत्व अन्वेषण इसे नकारती रही है परन्तु लोक का विश्वास इन अप्रामाणिक चीजों की सत्य के खोज के प्रति उदासीन है. राजस्थान के जयपुर-अलवर मार्ग में स्थित भानगढ़ का किला अपने भुतहा किंवदंतियों के लिए इसलिए ही विख्यात हो गया कि लोक की चेतना इन किंवदंतियों के सामने नत् है. वस्तु जगत की विडंबना कहिए कि अप्रामाणिकता पर उनके विश्वास का प्रतिशत अप्रत्याशित है.
कैलाश मनहर में ज़िद की स्वभाविकता की माने तो और उसके तह में जाएं तो चीज़ें तस्करी, बाजार, पूंजी, आधिपत्य, अधिग्रहण की सात पर्दे पीछे चल रहे कुचक्र की बदबू में परिलक्षित होता है. बाजार और मीडियाकरी दौर की बिडंबना देखिए कि वह उसे कैसे भुनाता है और सच को और अधिक रहस्य के लबादे से किस तरह ढंकने लगता है.
कैलाश मनहर चूंकि वस्तु तथ्य सत्य का अविष्कार बतौर सचेतक पूरी साफ़गोई से इस कविता में दर्ज कर ही दिए हैं तो शेष के प्रति जवाबदेही या कि उसके लाज लोक के कांधों पर है. अतः लोक यथार्थ; लोक के सिनसिज्म के निमित्त किसी दिन एक अवधारणा बने, कैलाश मनहर चाहते हैं लोक अपने जागरण से उसे ध्वस्त करे. ‘भानगढ़ भुतहा नहीं है’ यह लोक में जय घोष की तरह गूंजे.
उत्तर भानगढ़
भुतहा नहीं था भानगढ़ बहुत पहले
वहाँ झरना बहता था अनवरत
कलकल करता सोमकुण्ड में भरा रहता था
स्वच्छ नील-जल जिसमें
किलोळ करती रहती थीं मछलियाँ और
पाळ पर से कूद कूद कर नहाते रहते थे लड़के
लड़कियाँ और बड़ी उम्र की महिलायें
झरने या छोटे वाले दूसरे कुण्ड में नहाती थीं.
वास्तव में भुतहा नहीं था भानगढ़ जब जंगल के पेड़ लहलहाते थे
ठेठ जेठ की धूप में भी
छाया की क़तई कमी नहीं थी उन दिनों
भुतहा था ही नहीं भानगढ़
बिल्कुल नहीं था अभिशप्त भी
केवड़े के झुरमुट में बैठे रहते थे बेवड़े
सोमेश्वर की सीढ़ियों पर इन्तज़ार करती थीं माशूक़ायें
पलाश में दहकती थी प्रेमाग्नि की लपटें
और अमलतास से झड़ती थी मिलन-कामनायें
जब गोपीनाथ
किसी तस्कर के तहख़ाने में क़ैद
अपने दुर्भाग्य पर अश्रु बहा रहे होते थे
सभ्यता के हाहाकार से सताये हुये लोग
जीवन-सौभाग्य के स्वप्न संजोते थे
और तनिक भी नहीं मानते थे
भानगढ़ को भुतहा या कि अभिशप्त
वे अपने प्रेम में
वहां की मूर्तियां जब शोभित होती थीं
अभिजन-गृहों में और
तस्करों के हाथों में दी जाती थीं
नोटों की गड्डियां जब
रिकार्डर से बजाये जाते थे
पूर्णिमा की चांदनी में घुंघरू और
अखबारों में छपते थे अफ़वाहों की तरह
भूत-प्रेतों के अविश्वसनीय किस्से
वास्तव में तब भी भानगढ़ भुतहा नहीं था और
न ही अभिशप्त था अपने अकेलेपन में
वह विचारता रहता था प्राय:
सभ्यता के संजाल को तोड़ने का कोई मन्त्र
और पता नहीं कब और कैसे कि धीरे-धीरे
सूखने लगा मनसासर का जल
हर वर्ष झरनों का बहाव कम होने लगा उधर
ढाक और सिरिस और अमलतास होने लगे कम
गुग्गुल तो जैसे नष्ट ही हो गया और
केवड़े के झुरमुट में निरापद नहीं रहे बेवड़े
माशूक़ाओं की याद में
उदास रहने लगीं सोमेश्वर की सीढ़ियां और
कुण्ड में बच गया सिर्फ़
कीचड़ जैसा सड़ा हुआ जल
तो लगा अचानक कि शायद अब
होने लगा है भूतों का प्रकोप भानगढ़ पर जबकि
पहले नहीं था बिल्कुल भी भुतहा
या अभिशप्त यह भानगढ़
भानगढ़ में नहीं बचा जल और
छाया को भी तरसती हुई भानगढ़ की भूमि
भैंस-पाडियों और भेड़-बकरियों के
स्पर्श की याद में तड़कने लगी
जब गाय-बछड़ों के रंभाने के स्वर
लुप्त होने लगे भानगढ़ में
बिकने लगीं पानी की बोतलें और शीतल पेय
भानगढ़ में होटल और रिसोर्ट्स खुल गये
आने जाने लगीं चमचमाती गाड़ियां
भानगढ़ में हनुमान पूजा होने लगी
मेहनत की बज़ाय
व्यवसाय करने लगे भानगढ़ के किसान
ठगे जाते अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों के हाथों प्राय:
भानगढ़ में फैलने लगा माया-जाल
और जो भानगढ़ कभी भी भुतहा नहीं रहा था
ग्रस्त होने लगा भूत-प्रेतों के प्रकोप से
किसने बना दिया भानगढ़ को भुतहा
किसकी नज़र लगी भानगढ़ के जंगलों में
किसने पी लिया मनसासर का अथाह जल
किसने छीन लिया
गाय-भैंस और भेड़-बकरियों से उनका
हरा भरा रहने वाला चारागाह
उफ्फ क्यों जले जा रहे हैं
रेगिस्तान में चलने के अभ्यस्त पांव भी
भानगढ़ के पत्थरों पर
क्यों नहीं महकती केवड़े की गंध
इन दिनों
भानगढ़ बहुत विकसित हो रहा है किन्तु
पूछो उससे कि खुश है क्या तनिक भी ?
बस इसीलिये तो कहा मैनें कि
भुतहा नहीं था भानगढ़ पहले कभी भी
और न ही अभिशप्त था वह
ओ अफ़वाहबाज़ो !
ओ अखबारनवीसो !
ओ हॉन्टेड भानगढ़ कहने वाले फिल्मकारों !
ओ तस्कर सहयोगियो !
ओ व्यापारियों !
भानगढ़ पहले भुतहा नहीं था कभी भी
किन्तु उसे तुम अब बना रहे हो
भुतहा और अभिशप्त
अपने विकास के मोह में तुम भूलते जा रहे हो
भानगढ़ की नैसर्गिक उदासी और
थोप रहे हो मिथ्या-मुस्कान
वर्तमान के होंठों पर कंटीली धार देते
बेवड़ों का भी उतार दिया रे सारा नशा तुमने
सेवड़े को भी से लिया रे छलियों!
भैरव को भी कर दिया भयभीत रे
माशूक़ाओं को भी कर दिया आशिक़ों से दूर
हाय !
रोको रे रोको !अंधाधुंध दौड़ाते
अपने इस
उच्छृंखल घोड़े को अब तो तुम रोको रे !
***
‘अकाल की आशंका’ निश्चय ही अच्छी कविता है. तमाम-तमाम उन्माद, भय और आशंकाओं के बाद भी प्रेमियों ने वादे के अनुरुप मिलना तय किया, छोड़ा नहीं; मिला ही. बागवान ने एक नहीं कई कई वासंती पुष्प को रोंपा अनथक परिश्रम कर और सींचा भी उसी
लगन से. गृहणियों ने समय पर स्नान किया, रोकी नहीं और न रीतने दिया चूल्हे को तथा न ही रखा भूखा अपने परिवार को. सूखी भूमि पर किसानों ने हल चलाई तो वजहें बिल्कुल साफ़ और पारदर्शी है !
यहां तक कि भरी दुपहरी में वह नन्हीं चिड़िया अपनी धूल राग को नहीं छोड़ी. आकाल की आशंका के बावजूद, खुले पीपल की खोह में टिटहरी ने अंडे दिए, प्रकृति की स्वभाविकता को साकार करते हुए. ठीक वैसे ही बचे रह जाएंगे तमाम-तमाम भय और आशंकाओं से मनुष्य के जीवन में ‘जीवन-राग.’ हालांकि इस तरह की चिंतनशीलता बड़े अनुभवों से आते हैं पर प्रछन्न में सिनसिज्म का निर्माण करते हैं. ठहराव पैदा करने वाले होते हैं जबकि मनुष्य और प्रकृति की स्वभाविकता उसके क्रियाशील गतिशीलता से शिनाख्त होता है.
वह सतत संघर्ष शील रहता है और अपने आज तथा भविष्य के बुनियादी जरूरतों के लिए तात्कालीन विछोह के खिलाफ लड़ता रहता है. जो न सिर्फ खुद को क्रियाशील और चलायमान बनाता है पूरी प्रकृति और प्रक्रिया को भी अपने प्रभाव से प्रभावित करता है. वस्तुत: यह इन अर्थों में परिणाम मूलक है कि वह प्रकृति का अग्रगामी होता है और प्रकृति उसकी सहचर.
अकाल की आशंका
अकाल की आशंका के बावज़ूद
टिटहरी ने अण्डे दिये हैं पीपल की खोह में
दुपहरी भर वह चिड़िया गर्म धूल से नहाती रही
सूखी ज़मीन पर भी हल जोत दिये किसानों ने
गृहिणियों ने समय पर नहाना-धोना किया
अकाल की आशंका के बावज़ूद
बाग़वान ने रोप दीं चम्पा की छह-सात क़लमें
मैनें सरिस्का जाने के बारे में सोचा
युवाओं ने गोठ का कार्यक्रम बना लिया
लड़कियों ने खरीद लिये लहरिया-वसन
अकाल की आशंका के बावज़ूद
प्रेमियों ने वादा किया बरसात में मिलने का
बाग़ियों ने नदी घाटी में डाल दिये डेरे
***
कैलाश मनहर की कविताई यह पड़ाव है. जो मुझे उनके समग्र मूल्यांकन में, इस कविता में दिखाई देता है. अभिधा में कि व्यंजना में कहें मारक तो है ही, काव्य भाषा में भी प्रवाह पूरी गहराई ली हुई यह इस कविता में साफ़ दिखाई दे रही है. कैलाश मनहर की कविता इक्कीसवीं यानी नई और आधुनिक सदी के समय-समाज और उसके चाल-चरित्र में आए तथाकथित विकास को केन्द्रीय बनाता है, जिसमें सर्वाधिक और साफगोई भरी बात मूल्यों का अवमूल्यन है, उसकी सुनिश्चितता में लिख दी गई इबारत है.
इस कविता में कैलाश मनहर बहुस्तरीय पागल और गंवारू पन से मुठभेड़ करते दिखाई देते हैं. वे बताते हैं कि प्रगतिशीलता के गर्वानुभव के तह में न सिर्फ आधुनिक पुरुष शामिल हैं, स्वतंत्र चेत्ता युवतियां भी भंग मग्न है. विश्व बंधुत्व के ग्लोबल इवेंट की नग्नता खेतों को पाटकर चौड़ी चिकनी सड़क के रास्ते चुंधियाते मल्टीप्लेक्स और माल में घुस आए हैं इस नई सदी में.
सदी के इस मुहाने पर नदी-नाले, पर्वत, भूखंड को खा जाने को आतुर सभ्यता के पोषक धनपति, राज्याधीश गंतव्य की शीघ्रता में अधिक चाक चौबंद हो गए हैं. अपने विलासिता ऐश्र्वर्य के लिए इक्कीसवीं सदी का ‘आततायी सूर्य’ समानता के संघर्ष के नाम जाति-धर्म और संप्रदायिकता का विष बेल को बढ़ा रहे हैं. वे कहते हैं –
‘जबकि स्वतंत्रता की जरूरत
अब किसी
औपनिवेशिक सौदेबाज़ी में ढूंढ़ी जा रही थी’
कैलाश मनहर की यह कविता सेलेक्टिव नहीं है. हमलावर कविता है. गाहे-बगाहे फ़ैल गए उन्माद के खिलाफ की कविता है जो इस सदी का चारित्रिक पतन को दर्ज करने में कामयाब कविता है. वे कहते हैं –
‘कि हर कहीं राष्ट्रवाद का उग्र प्रेत
लपलपाता हुआ अपनी रक्तिम जीभ
नुकीले पंजों में दबोच रहा था
मनुष्यता की गर्दन निर्विघ्न’
यह क्रूर और कुटिल अंध राष्ट्रवाद के राजनय के जबड़ों में फंस गए शागिर्दों को बचाने की एक पवित्र कोशिश और कामना को अभिव्यक्त करने में सफल कविता है कहना लाज़िम है कि भयग्रस्त मानसिक अवस्था में हत्यायें किसी गैरजरूरी प्रक्रिया का भाग बन जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा दिख रही है.
रूग्ण और मानसिक विकार यदि व्यवस्था का भाग हो तो वह हमेशा ही दो मुंह लिए आता है, जो विश्व बंधुत्व और शांति की बात कर सामरिक महत्व के नाम उसे झुठलाता है और वह बर्बरता के अरण्यों में चहलकदमी करते भोली भाली जनता को युद्ध की विभीषिका में झोंक देता है, जहां से लौटना मुनासिब नहीं होता है.
किन्तु गौर करने वाली बात है. दृष्ट्या पंक्तियों को देखें तो कैलाश मनहर ‘सातवें आसमान’ से उतरी जिन किताबों की बात का जिक्र कर रहे हैं वह अस्पष्टता में हैं. चूंकि किताबें दहशतगर्दी का बहाना न होकर विचारों का संवाहक होते हैं. पर वे इसी काव्य पंक्ति में आगे कहते हैं कि समृद्धता का आंकलन पूंजी और हथियारों से हो रहा था तो कविता अपनी खोती व्यंजकता को पुनः हासिल करती है.
‘जब सातवें आसमान से उतरी किताबें
दहशतगर्द़ी का बहाना बन रही थीं
और समृध्दता का आकलन हो रहा था
पूंजी और हथियारों के संग्रह से
आगे वे बीसवीं सदी की हिंदी कविता के उन्मत काव्य प्रवृत्तियों पर सवाल खड़ा करते हुए उस समकाल में बेहतर का विश्वास से भरे कविगणों के पक्ष को दृढ़ आसक्ति भाव में रखने की कोशिश तो करते हैं पर अंत रचना के आवेग से बिदक कर कहीं दूर जाती प्रतीत होने लगता है. खैर ! इसे रचना प्रक्रिया में रख और बेहतर किया जा सकता है और विश्वास करता हूं कि वे इस काम में कोताही भी नहीं ही बरतेंगे.
‘उस तपती हुई शताब्दी के ज्वलन्त समय में
कुछ कवि जो
दहकते मरूस्थल में तलाश कर रहे थे
कविता का विषय अभी जैसे
मृग-मरीचिका की तरह दिख रहा था
उनकी प्यास के लिये थोड़ा-सा निर्मल जल’
यह इक्कीसवीं शताब्दी की किशोरावस्था थी
यह इक्कीसवीं शताब्दी की किशोरावस्था थी
कि जब
मूल्यों के अवमूल्यन को ही कहा जाता था विकास
और आधुनिकता के
मिथ्यावरण से ढँकी जा रही थीं निपट रूढ़ियाँ
कि जीन्स-टी शर्ट पहन कर
तिलक लगाये हुये
अथवा अनमूंछी दाढ़ियों में
गर्वानुभव करते थे
तथाकथित आधुनिक युवक और
पुरूष वर्चस्व का विरोध करते हुये भी
नियमपूर्वक करवा चौथ का व्रत रखती थीं
या कि बुर्क़े में निकलती थीं
आभासी स्वतंत्रचेत्ता युवतियां
जबकि विश्व बंधुत्व अब
ग्लोबल इवेंट में बदल चुका था और
खेतों का अधिग्रहण कर के बनाये जा रहे थे
चौड़ी-चिकनी सड़कों पर
चुंधियाते मल्टी-प्लैक्स और मॉल
कि नदियों का पानी सोखने की होड़ मची थी
धनपतियों और राज्याधीशों में जब
गन्तव्य की शीघ्रता के लिये
बनाये जा रहे थे एक में मिलते हुये पांच-पांच पुल
भ्रामक रास्तों की तरह शहर-शहर
अपने सुख-विलास के लिये प्रदीप्त
इक्कीसवीं सदी का यह आतताई सूर्य
समानता की प्राप्ति के लिये चमका रहा था जाति-वाद और साम्प्रदायिकता की चकाचौंध
जबकि स्वतंत्रता की जरूरत
अब किसी
औपनिवेशिक सौदेबाज़ी में ढूंढ़ी जा रही थी
कि हर कहीं राष्ट्रवाद का उग्र प्रेत
लपलपाता हुआ अपनी रक्तिम जीभ
नुकीले पंजों में दबोच रहा था
मनुष्यता की गर्दन निर्विघ्न
क्रूर और कुटिलतापूर्ण राजनय के जबड़ों में
पिस रहा था अन्तर्राष्ट्रीयता का चरित्र
उस भयग्रस्त मानसिकता के समय में हत्यायें
किसी जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन रही थीं
पवित्रता के नाम पर
मसीही संदेशों से निकाले जा रहे थे
छद्म-युध्द के अर्थ जबकि
अपौरुषेय ग्रन्थों में ढूंढ़े जा रहे थे
बर्बरता के अरण्यों की ओर
लौटने के मार्ग
जब सातवें आसमान से उतरी किताबें
दहशतगर्द़ी का बहाना बन रही थीं
और समृध्दता का आकलन हो रहा था
पूंजी और हथियारों के संग्रह से
उस तपती हुई शताब्दी के ज्वलन्त समय में
कुछ कवि जो
दहकते मरूस्थल में तलाश कर रहे थे
कविता का विषय अभी जैसे
मृग-मरीचिका की तरह दिख रहा था
उनकी प्यास के लिये थोड़ा-सा निर्मल जल
- इन्द्र राठौड़
Read Also –
अल-सल्वादोर के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी कवि रोके दाल्तोन की छह कविताएं
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]



