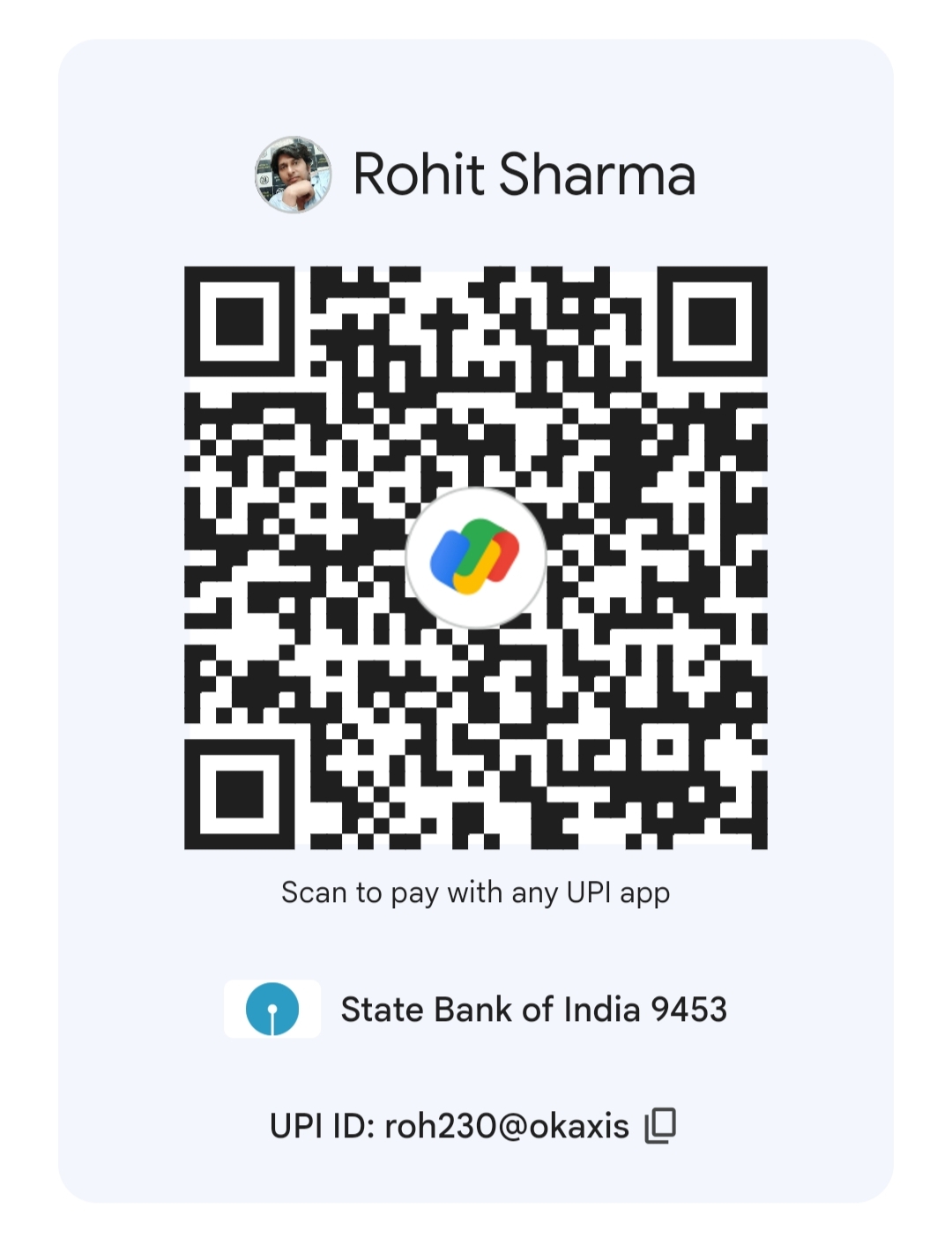चन्द्रभूषण
अक्टूबर 1990 का आखिरी हफ्ता था, जब मैं कवि रघुवीर सहाय से मिलने साकेत में उनके घर गया. दिल्ली के इस पॉश इलाके को मैंने अपने सामने खड़ा होते देखा है. 1981 में, जब एशियाड को ध्यान में रखते हुए मौजूदा साउथ दिल्ली की बसावट शुरू ही हो रही थी, यहीं के एक निर्माणाधीन मकान में रह रहे अपने भाई के पास मैं यह सोचकर आया था कि पढ़ाई-लिखाई गई भाड़ में, अब तो इस परदेस में ही कुछ कर खाऊंगा, कलह भरे घर में वापस नहीं जाऊंगा. जिद ज्यादा टिकी नहीं, और बात है.
1990 में साकेत अभी जैसा नहीं हुआ था लेकिन 1981 से तो यह इतना आगे चला आया था कि उसका कुछ भी सिर-पैर मेरी पहचान में नहीं आ रहा था. रघुवीर सहाय से मेरी मुलाकात का प्रयोजन कोई साहित्य-चर्चा नहीं, उन्हें अपनी पत्रिका ‘समकालीन जनमत’ में कुछ नियमित लिखने का आमंत्रण देना था. मेरे प्रधान संपादक महेश्वर ने उनसे साप्ताहिक कॉलम, और वह न हो सके तो उनकी रुचि से कुछ भी लगातार लिखवाने के लिए कहा था.
दुर्भाग्यवश, सहाय जी से मेरी मुलाकात अच्छी नहीं रही. उनके जैसे ईमानदार, रचनात्मक और पूरी तरह बेरोजगार बुद्धिजीवी के लिए यह बहुत कठिन समय था. एक तेज घटनाक्रम में चौ. देवीलाल के इस्तीफे से संकट में आई वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू करने की घोषणा की थी और बीजेपी ने अपना हिंदू वोट बैंक बिखर जाने के डर से इसके तुरंत बाद राम रथयात्रा निकालने की मुनादी फेर दी थी.
रघुवीर सहाय के अंतिम कविता संग्रह ‘एक समय था’ में संकलित कविता ‘मौका’ की ये पंक्तियां संभवत: पूर्व वित्तमंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को लेकर उनकी राय बताती हैं- ‘नेता ऐसा कुछ नहीं बता रहा/ जो जनता अभी नहीं देख रही/ और यह तो बिल्कुल नहीं कि यह जो पतन है/ वह किस अर्थनीति का नतीजा है/ वह केवल उसी अर्थनीति में विरोध की बात करता है/ जिसका मतलब है, अभी जो शासक है वैसा ही बनेगा/ सिर्फ भ्रष्ट नहीं होगा, ऐसा कहता है.’
काश, सहाय जी के यहां जाने से पहले यह कविता मैंने पढ़ रखी होती तो उनसे बात करने के लिए मेरे पास एक जमीन होती. लेकिन उस दौर में उनकी तो क्या किसी भी अच्छे कवि की कविताएं कम ही छपती थी. उन्हें छापने की इच्छुक ज्यादातर पत्रिकाएं एक-एक करके 1980 के दशक में ही बंद हो गई थीं. ‘क्षुधार काले पृथिवी गद्यमय’ वाली सुकांत की उक्ति हिंदी में चरितार्थ होने का पहला चरण तब तक पूरा हो चुका था.
बहरहाल, ऊपर वाली कविता में जाहिर राजनीतिक उचाट के अलावा चिड़चिड़ेपन के करीब पहुंचती सहाय जी की उदासी की कुछ निजी वजहें भी थीं. मुझसे मुलाकात के कोई साल भर पहले लिखी हुई ‘कविता’ शीर्षक वाली अपनी कविता में वे कहते हैं, ‘किसी ने बुढ़ापे में बोझ नहीं डाला/ लड़कियां ब्याह कर चली गईं, लड़के गुजर गए/ हर बार घूम फिर कर/ अपने एकाकीपन की व्याख्या करना/ क्या कविता है ?’
उस दोपहर साकेत की प्रेस एन्क्लेव सोसाइटी में पहुंचकर मैंने उनके खाली-खाली से फ्लैट की घंटी बजाई तो रघुवीर सहाय वहां बिल्कुल अकेले थे. दूरदर्शन में काम करने वाली उनकी बेटी मंजरी जोशी तब उनके साथ ही रहती थीं लेकिन उस वक्त वे ड्यूटी पर थीं. दरवाजे के छेद में लगे लेंस से अच्छी तरह तस्दीक कर लेने के बाद पायजामे और बांह वाली बनियान में कुछ लड़खड़ाते हुए से दरवाजा खोलने वाले एक काफी कमजोर, बुजुर्ग इंसान, जिनकी शक्ल बाद में पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में नरसिंह राव के साथ गड्डमड्ड हो गई.
हालांकि मुझे और लगभग पूरे देश के लिए बतौर प्रधानमंत्री, या किसी भी रूप में नरसिंह राव की शक्ल ठीक से पहचानने का मौका आठ महीने बाद जून 1991 में ही आ सका, जब सहाय जी को दुनिया से विदा हुए छह महीने बीत चुके थे. उनके यहां एक गिलास पानी पीकर मैंने अपना परिचय एक पॉलिटिकल होलटाइमर के रूप में दिया तो पहला सवाल सहाय जी ने मुझसे यही किया कि क्या मैंने लोहिया को पढ़ा है.
मैंने कहा- ‘बस, थोड़ा सा. ‘इतिहास-चक्र’, ‘भारत विभाजन के गुनहगार’, ‘अर्थशास्त्र : मार्क्स से आगे’ और कुछ छिटपुट लेख.’ रघुवीर सहाय इतना सुनते ही भड़क गए- ‘आप खुद को होलटाइमर कहते हैं, देश बदलना चाहते हैं, लेकिन लोहिया को नहीं पढ़ा ?’ बताने की जरूरत नहीं कि मैं बिल्कुल सकपका गया. कुछ गोलमोल सफाई देने की कोशिश की, फिर कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा ठंडा पड़ते देख वहां आने के मकसद के बारे में बताया- ‘क्या आप जनमत के लिए आठ-नौ सौ शब्दों का एक साप्ताहिक कॉलम लिख सकते हैं.’
उन्होंने कहा कि जनमत और आईपीएफ का नाम तो उन्होंने सुन रखा है और कॉलम लिखना भी पसंद करेंगे, लेकिन इसके लिए पैसे कितने मिलेंगे. उस समय तक जनमत में लिखने के लिए किसी को पैसे देना तो दूर, इस बारे में सोचा भी नहीं गया था. कम से कम मेरे राडार पर तो यह बात दूर-दूर तक नहीं थी. जाहिर है, इससे मेरी सकपकाहट और बढ़ गई.
रघुवीर सहाय जैसे कद्दावर संपादक, कवि, रेडियो और रंगमंच के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के सामने मेरे मुंह से इतना ही निकल पाया कि अपने कॉलम के लिए वे कितने धन की अपेक्षा रखते हैं ! उनके जैसा संवेदनशील और कुशाग्र व्यक्ति मेरे शब्दों में मौजूद अनमनेपन को ताड़े बिना नहीं रह सकता था. सो उन्होंने कहा, ‘आप अपने एडिटर या मालिक, जो भी हों, उनसे बात करके बताइएगा.’ साथ में यह भी पूछा कि ‘आप लोगों को भी तो काम के लिए कुछ मिलता ही होगा, फिर मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए ?’
मैंने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, न ही मैंने कभी इस बारे में कुछ सोचा है. उन्होंने कहा, ‘लेकिन कहीं रहते तो होंगे, खाते तो होंगे, इधर-उधर आते-जाते तो होंगे.’ मैंने कहा, ‘पार्टी ऑफिस में रहता हूं, वहीं बनाता-खाता हूं, शहर में आने-जाने और चाय-पानी के लिए हर महीने सौ रुपये मिलते हैं. कभी कम पड़ जाते हैं तो पहले भी मांग लेता हूं. बचे रह जाते हैं तो कह देता हूं कि अभी काम चल रहा है, बाद में ले लूंगा.’
किसी अंग्रेज लेखक की, संभवत: जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की उक्ति है कि ‘जवान लोगों पर जवानी यूं ही जाया हो जाती है.’ किसी कवि-चिंतक से उसकी कविताओं और विचारधारा के बारे में अपनी क्षमता भर जाने बगैर मिलने से बड़ी मतिमंदता और कृतघ्नता भला और क्या हो सकती थी ? रघुवीर सहाय से इस मुलाकात के बमुश्किल छह साल बाद मुझे भी दिल्ली शहर में पैसे-पैसे को लेकर चिंतित होना पड़ा और लिखवा कर पैसे न देने वालों के लिए जुबान से कटु वचन भले न निकले हों, लेकिन दिल से बद्दुआएं भरपूर निकलीं.
लोगों के बारे में झट से कोई राय बना लेने की दुष्प्रवृत्ति मेरे भीतर न होती तो शायद रघुवीर सहाय से मिलने के कुछ और मौके मुझे मिले होते. हालांकि इसके लिए वक्त कुल दो महीनों का ही मिलता, क्योंकि इसके बाद उनसे अगली मुलाकात मेरी 30 दिसंबर 1990 को ही हो सकी, जब उनका पार्थिव शरीर उनकी कॉलोनी प्रेस एन्क्लेव से बाहर ले जाया जा रहा था.
तब से अब तक पूरे तीन दशक गुजर चुके हैं. कवि रघुवीर सहाय के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय कोई पूछता है तो अपने संक्षिप्त से अनुभव के आधार पर इतना ही कह पाता हूं कि उनके पास खरेपन की शक्ति थी, साथ में पद-प्रतिष्ठा से जुड़े कवच-कुंडल छोड़ कर एक अनजान युवक तक से सीधा बोलने और खुली बहस में जाने की अद्भुत क्षमता भी थी. और अगर पूछने वाले के पास सुनने का धीरज हुआ तो सहाय जी की ये तीन पंक्तियां दोहराता हूं- ‘इस लज्जित और पराजित युग में/ कहीं से लाओ वह दिमाग़/ जो ख़ुशामद आदतन नहीं करता.’
Read Also –
अ-मृत-काल में सरकार, लेखक और उसकी संवेदनशीलता
रेणु का चुनावी अनुभव : बैलट की डेमोक्रेसी भ्रमजाल है, बदलाव चुनाव से नहीं बंदूक से होगा
यादों के झुरमुट में मुक्तिबोध
जनकवि शील – कुछ अप्रासंगिक प्रसंग
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]