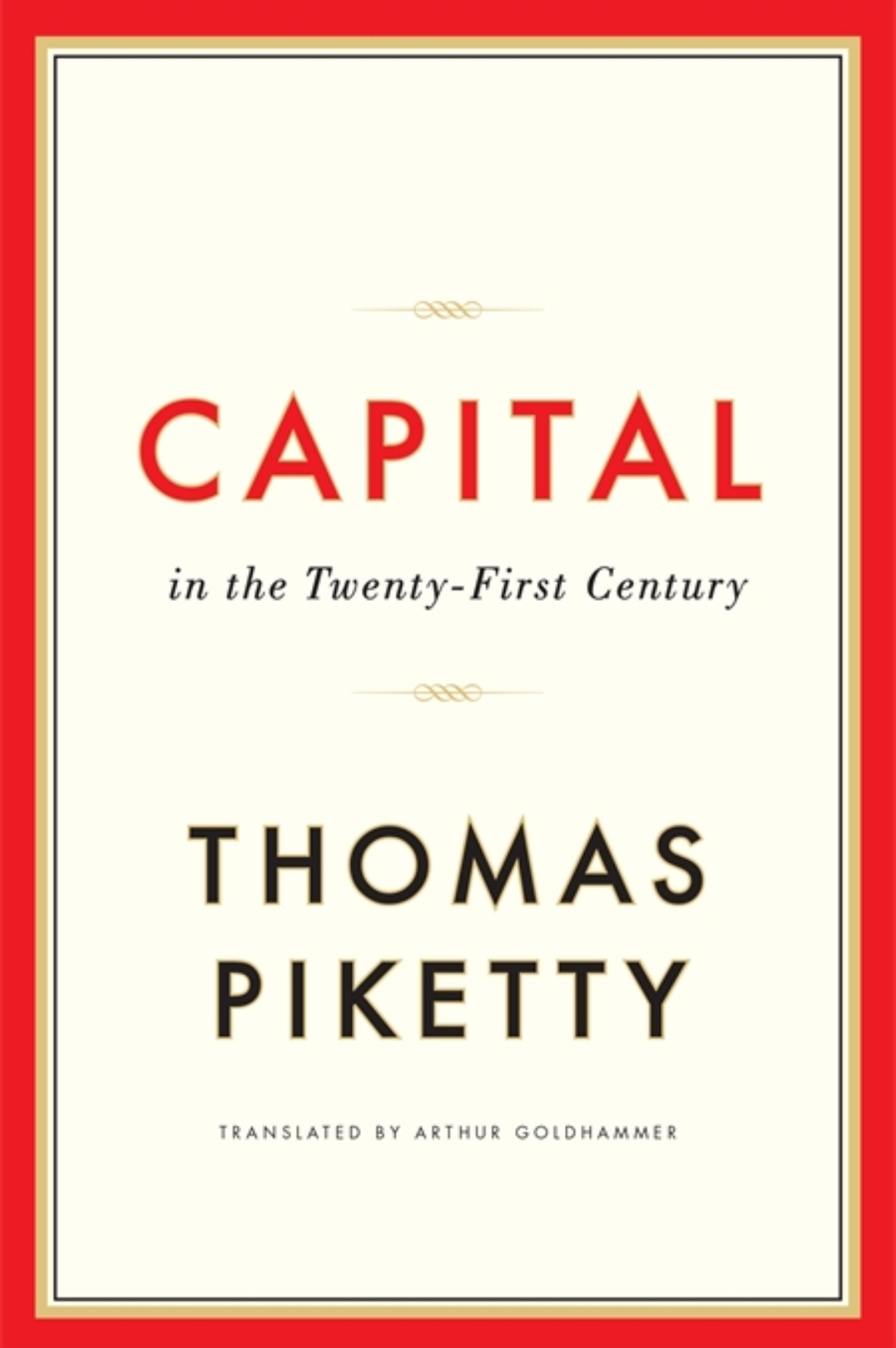रविश कुमार, अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकार
भारत की यह सच्चाई है कि यहां जातिवाद है. हर दिन घरों में आदरणीय माता-पिता जाति की ट्रेनिंग देते हैं. वो ट्रेनिंग शादियों के वक़्त संस्कृति बन जाती है. राजनीति जाति के नाम पर ही चलती है. आपकी जाति के जब मंत्री बनते हैं तो ख़ुश होते हैं और जाति के लोग उनका अलग से स्वागत करते हैं. अगर इसकी सच्चाई सामने आ जाए तो क्या दिक़्क़त है. ?
जाति की गिनती होगी तो जाति की राजनीति में बराबरी आएगी. सबको पता रहेगा कि किस क्षेत्र में किस जाति की संख्या है. इससे एक लाभ यह भी हो सकता है कि जाति की चुनावी राजनीति ख़त्म हो जाएगी क्योंकि तब आप भी जान जाएंगे कि फ़लां जाति की संख्या अधिक है इसीलिए ये दल इन्हें टिकट दे रहा है तो मुमकिन है आप उसे वोट न करें.
इसके अलावा एक सच्चाई और है. जाति से बड़ी सच्चाई. बल्कि इस सच्चाई को पहले नंबर पर लिखना चाहिए था. आर्थिक असमानता का कारण जाति में है. भारत में संसाधन पर शुरूआती क़ब्ज़ा किसका रहा है, इसका भी अध्ययन होना चाहिए. देखा जाना चाहिए कि जिनके पास 1947 के वक़्त ज़मीन थी उन परिवारों ने कितनी तरक़्क़ी की ? जिन परिवारों के बाद ज़मीन नहीं थी, उन परिवारों के कितनी पीढ़ी के बाद जाकर तरक़्क़ी की ? ज़रूर कुछ योजनाओं के तहत भूमिहीनों की ज़मीनें दी गईं तो उनका भी अध्ययन होना चाहिए. जब यह अध्ययन होगा तो पता चलेगा कि भारत में आर्थिक दौड़ बराबरी से कभी शुरू नहीं हुई और आज भी नहीं होती है.
स्कूल के दिनों में हमने एक रेस देखी थी. इस रेस में एक टांग बांध दिया जाता था. एक ही टांग से दौड़ना पड़ता था. दलित आदिवासी को न सिर्फ़ जाति का दंश झेलना पड़ा बल्कि उनकी दोनों टांगें रस्सी से बांध दी गई कि अब आप दौड़ कर दिखाएं. इसके बाद भी इस तबके के कई लोग आगे आए लेकिन आगे आने में ही जान निकल गई. ख़ूब अपमानित होते हुए, जाति का दंश झेलते हुए आगे भी आए तो एक सामान्य आर्थिक स्थिति तक पहुंच कर पस्त हो गए.
आज भी जब इस समाज के नौजवान घोड़ी पर चढ़ जाते हैं तो इनकी जाति का पता पूरे गांव को चल जाता है. दलित लड़के हेल्मेट पहन कर घोड़ी चढ़ शादी करने जाते हैं. क्या यह सच्चाई नहीं है ? तो जाति की गिनती के साथ किस जाति के पास कितनी ज़मीन है, इसका सर्वे होना चाहिए. जाति के हिसाब से ज़मीन का डेटा होना चाहिए.
इससे आप क्या जानेंगे ? अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी की किताब है CAPITAL. इस किताब में टैक्स रिटर्न का अध्ययन किया गया है. कई दशकों के रिटर्न को देखने के बाद पिकेटी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज भी वही चंद लोग टैक्स दे रहे हैं जिनके पूर्वजों के पास ज़मीन थी. उन्हीं के संपर्क बने, वही राजनीति में आए, वही लूट में शामिल रहे, भ्रष्टाचार में शामिल रहे.
भारत में भी इस तरह का अध्ययन होगा तो हमारा आपका समय बचेगा. डेटा रहेगा तो पता चलेगा कि किस जाति के पास कितनी ज़मीन है, कितनी नौकरी है, कितने लोग टैक्स देते हैं. जाति की बहस तथ्यों पर होने लगेगी. अब यह मत कहिए कि आप जाति में यक़ीन नहीं करते हैं. ज़रूर कुछ लोग जाति में यक़ीन नहीं करते हैं लेकिन क्या यह सच नहीं है कि ज़्यादातर लोग जातिवाद ही करते हैं. ऊपर से अब तो धार्मिक रुप से उन्मादी भी हो गए हैं, ख़ैर ये लेख पढ़िए.
कैपिटल-असमानता का अर्थशास्त्र
थामस पिकेटी की एक किताब आई है – कैपिटल इन दि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी. पिकेटी पेरिस स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के प्रोफेसर हैं. भारत सहित दुनिया भर के कई अर्थशास्त्रियों ने मिलकर लगभग तीन सदियों के दौरान उपलब्ध आय और संपत्ति से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया है. इन आंकड़ों के आधार पर लगभग बीस विकसित मुल्कों में इस पूंजीवादी व्यवस्था के तहत आई आर्थिक असामनता का अध्ययन किया गया है.
देखा गया है कि इन आर्थिक नीतियों से समाज में आर्थिक असामनता कम हुई है या बढ़ी है. यह किताब जिस निष्कर्ष पर पहुंचती है वो हमें मजबूर करती है कि हम मौजूदा दौर की आर्थिक नीतियों के प्रति राजनीतिक रूप से कोई प्रतिक्रिया तैयार करें. पिकेटी यह भी दावा करते हैं कि उनकी किताब पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है. वो सिर्फ इतना दावा करती है कि चंद कमज़ोरियों के कारण जो बहुत हद तक किसी के हाथ में नहीं है, यह असमानता बढ़ेगी ही कम नहीं हुई है. हर सरकार और उसकी आर्थिक नीतियों के साथ जो गरीबी दूर करने का भ्रम फैलाया जाता है, होता ठीक इसके उलट है.
पूंजी का संचय चंद हाथों में होता है और इस परिधि के बाहर की व्यापक जनता ग़रीब रह जाती है. कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल के बाद करीब साढ़े सात सौ पन्नों की इस किताब को पढ़ना चाहिए. पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट, विकास के दावों को इस किताब के बहाने तथ्यात्मक चुनौती दी जा रही है. हिन्दुस्तान में भी ज़रूरी है कि इस किताब को व्यापक संदर्भों में पढ़ा जाए और पूंजीवादी व्यवस्था में ही उन विकल्पों को खोज कर देखा जाए कि क्या प्रतिभा या मेधा पर आधारित इस बाज़ार व्यवस्था पर हम गरीबी दूर करने या आर्थिक समानता के उच्चतम स्तर कायम करने का भरोसा कर सकते हैं. इस पुस्तक का निष्कर्ष तो वैसा नहीं है.
किताब कुजनेट्स नाम के अर्थशास्त्री के काम की सराहना से शुरू होती है लेकिन इन्हीं के काम से सबक सीखते हुए अपने शोध का आधार तैयार करती है. और नतीजे में पाती है कि कुज़नेत्स की जो खोज थी वो दरअसल अल्पकालिक थी. कुज़नेत्स अमरीकी अर्थशास्त्री थे और अमरीका में उपलब्ध आय, आयकर और संपत्ति के आंकड़ों के आधार पर दावा करते हैं कि पूंजीवादी विकास के उच्चतम चरण में समाज में आर्थिक असामनता घटती है. ग्रोथ उस ज्वार की तरह है जो सभी नावों को उठा लेता है. यानी समाज के व्यापक तबके को इसका लाभ होता है और सबका उत्थान होता है.
कुज़नेत्स दावा करते हैं कि 1913-48 के बीच अमरीका में आय असमानता घट जाती है. चोटी के पूंजीपतियों की आमदनी या पूंजी संचय में दस से पंद्रह प्रतिशत की कमी आती है और यह कम हुई पूंजी समाज के दूसरे तबकों में वितरित होती है यानी कुछ और लोग भी अमीर होते हैं. हालांकि कुजनेत्स को पता था कि यह जो कमी आई है वो किसी नियम के तहत नहीं बल्कि दुर्घटनावश आई है. इसी दौरान दुनिया को दो विश्वयुद्धों का सामना करना पड़ा था. 1970 से दुनिया के अमीर देशों में फिर से आर्थिक असमानता बढ़ने लगती है जो आज तक जारी है. कभी भी यह प्रक्रिया उल्टी दिशा में नहीं चली. यानी ग्रोथ रेट की राजनीति या अर्थव्यवस्था से सबका भला नहीं होता.
पिकेटी कुज़नेट्स के आंकड़ों पर सवाल करते हुए अपने आंकड़ों और सोर्स को और व्यापकर करते हैं. 1913 में अमरीका में और 1922 में आयकर लागू हो चुका था. कुछ मुल्कों में इससे पहले और कुछ मुल्कों में इसके बहुत बाद लागू हुआ. फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका, स्वीडन, जर्मनी, भारत, चीन, जापान सहित बीस देश इस अध्ययन में शामिल हैं.
दो सदियों के आंकड़ों का अध्ययन कम चुनौतीपूर्ण और रोचक नहीं रहा होगा. इस काम में तीस शोधकर्ता लगे रहे और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक डेटाबेस तैयार कर दिया, जिसे वर्ल्ड टाप इनकम डेटाबेस कहते हैं. पिकेटी समझाते हैं कि हम और आप दो तरह से आमदनी हासिल करते हैं. एक वर्ग में तनख्वाह, मज़दूरी, बोनस आदि हैं तो दूसरे वर्ग में किराया, सूदखोरी, डिविबेंट, ब्याज, लाभ, कैपिटल गेन्स इत्यादि.
पिकेटी का कहना है कि संपत्ति के वितरण का इतिहास हमेशा से राजनीतिक रहा है. इसे सिर्फ आर्थिक ढांचे तक संकुचित कर नहीं समझा जा सकता. यानी पिकेटी कह रहे हैं कि आपके गांव में पहले एक ज़मींदार थे लेकिन बाद में कुछ और ज़मींदार पैदा हुए. इसके पीछे राजनीतिक फैसले का भी हाथ रहा है, न कि सिर्फ कुछ लोगों ने मजदूरी कर उतनी ज़मीन जायदाद खरीद ली. इसका भी राजनीति कारण रहा कि कुछ लोग मजदूरी ही करते रह गए और गांव में संपत्ति के मामले में ज़मींदार के बराबर कोई पैदा नहीं हो सका. गांव और ज़मींदारी का यह उदाहरण मैं आपको अपनी समझ से दे रहा हूं.
पिकेटी इस धारणा को धीरे-धीरे चुनौती देते हैं कि ज्ञान और कौशल (जिसे आप अंग्रेजी में नौलेज और स्किल बोलते हैं) पर खर्च करने या विकास करने से आर्थिक असमानता कम होती है. यानी ज्ञान का जितना विस्तार और मिश्रण होता है उससे समाज के व्यापक तबके को आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिलता है.
पिकेटी कहते हैं कि कोई यह मान सकता है कि समय के साथ उत्पादन तकनीकि को व्यापक कौशल (स्किल) की ज़रूरत होती है. ऐसा होने पर आय में पूंजी का हिस्सा कम होने लगेगा और श्रम का हिस्सा बढ़ने लगेगा. इसे इस तरह से समझिये कि मानवीय श्रम (ह्यूमन लेबर) की जो पूंजी है उसकी वित्तीय पूंजी और रियल स्टेट पर विजय होगी. यानी सिर्फ बिल्डर कंपनियों और स्टाक मार्केट के खिलाड़ी ही इस विकास से लाभांवित नहीं होंगे. (ऐसा मैंने समझा).
एक काबिल मैनेजर की शेयर बाज़ार के सटोरियों से ज्यादा पूछ होगी. बाज़ार में भाई भतीजावाद की पराजय होगी और कौशल जीतेगा. वैसे हम हिन्दुस्तानी राजनीति में ही परिवारवाद से ठीक से नहीं लड़ सके और बिजनेस की दुनिया में तो भाई भतीजावाद, जिसे अंग्रेजी में नेपोटिज्म कहते ही मतलब काफी व्यापक हो जाता है, को सामान्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं, जैसे यह बिजनेस का प्राकृतिक नियम हो. पिकेटी समझाते हैं कि ऐसा नहीं है. यह नेपोटिज्म फलता फूलता ही राजनीतिक कारणों से है. पिकेटी अपनी किताब में इस अवधारणा को चुनौती दे रहे हैं कि यह सोच की दुनिया में जो असमानता है वो प्रतिभा की कमी के कारण है, गलत है.
पिकेटी एक और आशावादी मान्यता को खंगालते हैं, वह यह कि क्या सचमुच इस पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था में क्लास वारफेयर यानी वर्ग युद्ध की स्थिति समाप्त हो जाएगी ? मतलब ऐसा होगा कि पूंजी का संचय और वितरण रेंटियर (सूदखोर, संपत्तियों के मालिक) के वंशजों और वंचितों के वंशजों के बीच टकराव का कोई कारण नहीं रहेगा. यह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है. हमारी राजनीति में युवा युवा का शोर ज्यादा सुनाई देता है.
पिकेटी कहते हैं (और इसे ठीक से समझे जाने की ज़रूरत है, जिसमें मैं सक्षम नहीं हूं) कि मेडिसिन और जीवन शैली मे सुधार के कारण जीवन प्रत्याशा बढ़ी है. लोग युवावस्था में ज्यादा संपत्ति संचय करते हैं. आप यह देखते भी होंगे कि जो युवा है उसे ही बैंक या बीमा वाले प्राथमिकता देते हैं.
ख़ैर, पिकेटी कहते हैं कि यह दोनों ही बातें भ्रामक हैं. इस बात के कम ही प्रमाण हैं कि राष्ट्रीय आय में श्रम का हिस्सा लंबे समय तक बढ़ा है. इसका मतलब यह है कि जो आप जीडीपी वगैरह देखते हैं, उसमें आपकी हिस्सेदार कम है उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है जो गिनती के थोड़े हैं और जिनकी पूंजी क्षमता कई लाख करोड़ तक पहुंच गई है. जबकि तथ्य है कि उन्नीसवीं, बीसवीं और अब तक की इक्कीसवीं सदी में गैर मानव पूंजी (नान ह्यूमन कैपिटल) जिसके हाथ में था, उसी के हाथ में रहा. यानी वो तबका ज्यादा संपत्ति संचय करता है जिसके पास पहले से ज़मीन जायदाद है, शहरों में संपत्ति है.
इस किताब में एक उदाहरण दिया गया है. जैसे किसी कंपनी में बाकी लोग भी स्किल्ड हैं मगर तनख्वाह या बोनस का बड़ा हिस्सा गिनती के शीर्ष मैनेजरों में बंट जाता है, शेष लोग अपनी कमाई जोड़ते रहते हैं और महीने के मैनेजर या एक्सेलेंट जैसे तमगे पाकर छोटे-मोटे कूपनों से संतोष कर लेते हैं, यह सोच कर कि प्रतिभा का उचित सम्मान हुआ है.
जब अर्थव्यवस्था के विकास दर से पूंजी पर ब्याज की कमाई का हिस्सा बढ़ने लगता है, तब ऐसी स्थिति में बाप-दादा (इनहेरिटेंस) की पूंजी या संपत्ति का विकास तेजी से होता है. जो पूरा जीवन श्रम में लगा देते हैं उनसे कहीं ज्यादा बाप दादा वालों के पास पूंजी संचय होता है. पूंजी का संग्रह इन्हीं चंद लोगों के हाथ में रह जाता है.
पिकेटी और उनके अर्थशास्त्रियों की टीम दुनिया भर के आंकड़ों से यह स्थापित करती है. यानी हम और आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि यह जो खुली बाज़ार अर्थव्यवस्था है उसमें प्रतिभा के दम पर सबके लिए समान अवसर हैं. प्रतिभा की अवधारणा पर ऐसा तर्कपूर्ण किया गया है जिसे और गंभीरता से परखने की ज़रूरत है. पिकेटी कहते हैं कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट और कम होगा, तब स्थिति और भयंकर हो जाएगी.
अब मैं यहां दो उदाहरण देना चाहता हूं. ब्लूमबर्ग पर एशिया के सबसे अमीर ली का शिंग का एक बयान मिला जिसमें वे आगाह कर रहे हैं कि अगर इसका समाधान नहीं खोजा गया तो खतरा यह है कि हम इसे नार्मल की तरह बरतने लगेंगे. हांगकांग के ली का शिंग कहते हैं कि सरकार को ऐसी नीतियां मजबूती से लागू करनी चाहिए जो समाज में संपत्ति या संसाधन का पुनर्वितरण करें.
ली के भाषण का शीर्षक है Sleepless in Hong Kong जिसे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है. संसाधनों की बढ़ती कमी और विश्वास में घटोत्तरी के कारण उन्हें रातों को नींद नहीं आती. जिस तरह का गुस्सा और ध्रुवीकरण समाज में बढ़ रहा है उससे विकास की प्रक्रिया थमेगी और असंतोष बढ़ेगा. विश्वास हमें समन्वय में जीने लायक बनाता है. अगर यह नहीं रहा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिस्टम से भरोसा कम होगा. यह बात कोई नक्सल नहीं कह रहा बल्कि वो कह रहा है जो इस व्यवस्था का लाभार्थी है.
आज के इंडियन एक्सप्रेस में मराठा आरक्षण पर राजेश्वरी देशपांडे और नितिन बिरमल का लेख छपा है. इसमें राजेश्वरी बताती हैं कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय के नेताओं का वर्चस्व तो रहा मगर इसका लाभ समाज के कुछ तबकों को ही मिला. पश्चिम महाराष्ट्र के हिस्से में मराठा नेताओं के पास पूंजी आई तो मराठवाड़ा के मराठा गरीब और पिछड़ेपन की तरफ धकेले गए.
इसी इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले एक लेख छपा था कि महाराष्ट्र की करीब 170 चीनी मिलों में से 160 मराठा समुदाय के हैं और ज़मीन का सत्तर फीसदी हिस्सा इसी समुदाय के हिस्से में है। इस लिहाज़ से समुदाय कितना ताकतवर लगता है मगर संपत्ति और आय के वितरण की नज़र से देखें तो उस राजनीतिक वर्चस्व का फायदा उन्हीं को मिला होगा जिनके पास बाप-दादा की संपत्ति होगी। क्या पिकेटी की बात उनकी किताब से बाहर भी सच हो रही है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं और खास समझ भी नहीं रखता फिर भी चाहता हूं कि आप सब इस किताब को पढ़ें। निष्कर्ष से ज्यादा पिकेटी के माडल को देखें और उसके आधार पर अपने आस पास के समाज को देखें। पिकेटी का एक ब्लाग भी है।
Read Also –
जातिवार जनगणना से कौन डरता है ?
भारत में जातिवाद : एक संक्षिप्त सिंहावलोकन
शैडौ ऑफ कास्ट : जातिवाद का जहर
भारत में जाति के सवाल पर भगत सिंह और माओवादियों का दृष्टिकोण
‘मदाथी : अ अनफेयरी टेल’ : जातिवाद की रात में धकेले गए लोग जिनका दिन में दिखना अपराध है
[प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करे…]