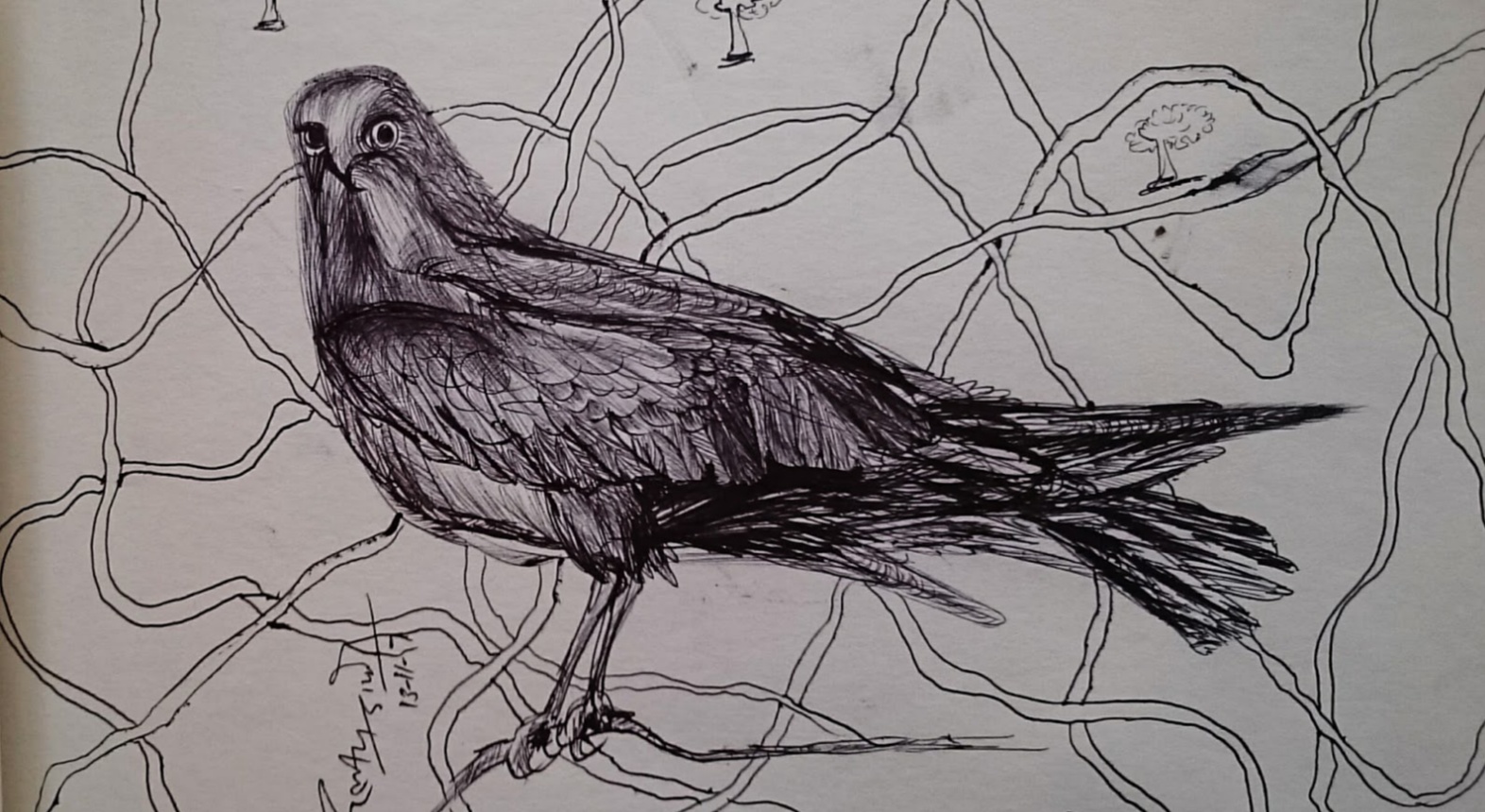
मैं डिंकू मुंडा, बाप सिंकू मुंडा, जंगल निवासी, अनपढ़, ग़रीब, जंगली कंद मूल पर जीने वाला हूंं.
वे कहते हैं मैं भी आदमी जैसा दिखता हूंं, तब भी, जब सिर्फ एक लंगोट में लिपटा मेरी हड्डियों का ढांंचा चमड़े को तोड़कर बाहर आने की कुलबुलाहट में दांंत निपोरे हुए किसी भिखारियों की बस्ती-सा दिखता है.
मैं डिंकू मुंडा, बाप सिंकू मुंडा, दिन भर अपने जंगल में भारी बूटों की आवाज़ सुनता हूंं और उनके चमकते संगीनों से धुंंधलाई आंंखों को धोने के लिए झरने का रुख़ करता हूंं.
मैं डिंकू मुंडा, बाप सिंकू मुंडा जब अपनी पत्तल की झोंपड़ी में सोता हूंं तो पुलिस बाहर से आवाज़ देती है, ‘कौन है वहांं ?’
मैं रोज़ एक ही जवाब देता हूँ, ‘मैं हूंं, डिंकू मुंडा, बाप सिंकू मुंडा’, और आगे बढ़ जाते हैं वे.
रात में बिना वर्दी वाले आते हैं, बंदूक़ धारी, और फिर पूछते हैं, ‘कौन है वहांं ?’ मैं उनको भी वही जवाब देता हूंं, ‘मैं डिंकू मुंडा, बाप सिंकू मुंडा.’ आगे बढ़ जाते हैं वे.
मैं अनपढ़, गंवार, जंगली, नहीं समझता रोज़ एक ही सवाल क्यों पूछते हैं वे ? वो तो जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन इतना भी नहीं कि धान रोपती मांं के बेतरा में समा जाऊंं, तो मांं ने मुझे यह जवाब रटा दिया था कि कभी अगर जंगल में भटक जाऊंं, और कोई पूछ ले तो यही जवाब देना. मैं अनगिनत बार भटका भी, और हर बार कोई अजनबी मेरा जवाब सुनकर मुझे मेरी मांं के पास लौटा दिया.
वे क्यों ऐसा करते थे नहीं मालूम.
कल रात जंगल हिल गया था गोलियों और बमों के धमाकों से.
सुबह जब झोंपड़ी से निकला तो हवा में बारूद की महक तैर रही थी. एक फ़र्लांग दूर एक पेड़ जल गया था.
रात भर डर से, शिकारी के डर से छुपे कुत्ते की तरह झोंपड़ी में पड़ा रहा.
आज शांति है. शहर की तरफ़ जाने का मन हुआ. पैदल निकल पड़ा.
शहर में लोग जगह-जगह तीन रंगों का एक झंडा फहरा रहे थे. मैं अनपढ़ गंवार, जंगली कुछ नहीं जानता. एक मिठाई का पैकेट किसी ने हाथ में थमा दिया. मैंने मांंगा नहीं. मैं पेड़ पौधों से फल छोड़ कर सिर्फ़ नदी से थोड़ा पानी मांंगता हूंं.
मैं डिंकू मुंडा, बाप सिंकू मुंडा, मिठाई मुंंह में डालने ही वाला था कि एक सिपाही आ कर पूछा, ‘क्या नाम है रे ?’
मैंने कहा, ‘मैं डिंकू मुंडा, बाप सिंकू मुंडा.’
‘घर ?’
‘जंगल में पातिपहाड़ गांंव.’
‘तो चल थाने, साला यहांं मिठाई खा रहा है.’
मैं अनपढ़, ग़रीब, जंगली कुछ नहीं समझता. सिपाही ने मेरे हाथ पीछे से बांंध दिए और गाड़ी में बैठा कर थाने ले गया.
थाने में पुलिस वाले वही तीन रंगों का झंडा फहरा रहे थे. सिपाही ने बड़े साहब के कानों में कुछ कहा. बड़े साहब ने लाल लाल आंंखों से मुझे घूरा.
एक बार जंगल में एक लकड़बग्घा इसी तरह से देखा था मुझे. वह चट्टानों के उपर था, मैं नीचे खेतों में. डर के मारे काठ मार गया था मुझे. क्या सोच कर लकड़बग्घा थोड़ी देर घूर कर आगे बढ़ गया, शायद उसे मेरे शरीर पर कोई मांंस नहीं दिखा.
तीन रंगों का झंडा फहर गया था. सबको मिठाई का पैकेट मिल रहा था. मेरे सामने भी आया. मैं अनपढ़, जाहिल, नहीं समझा कैसे लूंं ? मेरे हाथ तो पीछे से बंधे हुए थे. मैं हंस पड़ा.
बड़े साहब ने डांंट कर पूछा, ‘क्यों हंसता है बे ?’
मैंने हिम्मत कर पूछा, ‘साहेब, ये तीन रंगों का लत्ता क्या है ?’
उसके बाद तो प्रलय आ गया.
साहब ने मुझे एक लात मार कर ज़मीन पर गिरा दिया, और फिर लात घूंंसों और डंडे से पिटाई.
साहब चिल्ला रहे थे, ‘साले नक्सली, हरामी … तिरंगा नहीं पहचानता … साले हरामी … इसको आज़ादी कहते हैं रे सुअर … आज़ादी … आज़ादी … आज़ादी …’
मैं डिंकू मुंडा, बाप सिंकू मुंडा, अनपढ़, जाहिल, ग़रीब, जंगली कब का बेहोश हो गया था.
- सुब्रतो चटर्जी
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे…]


