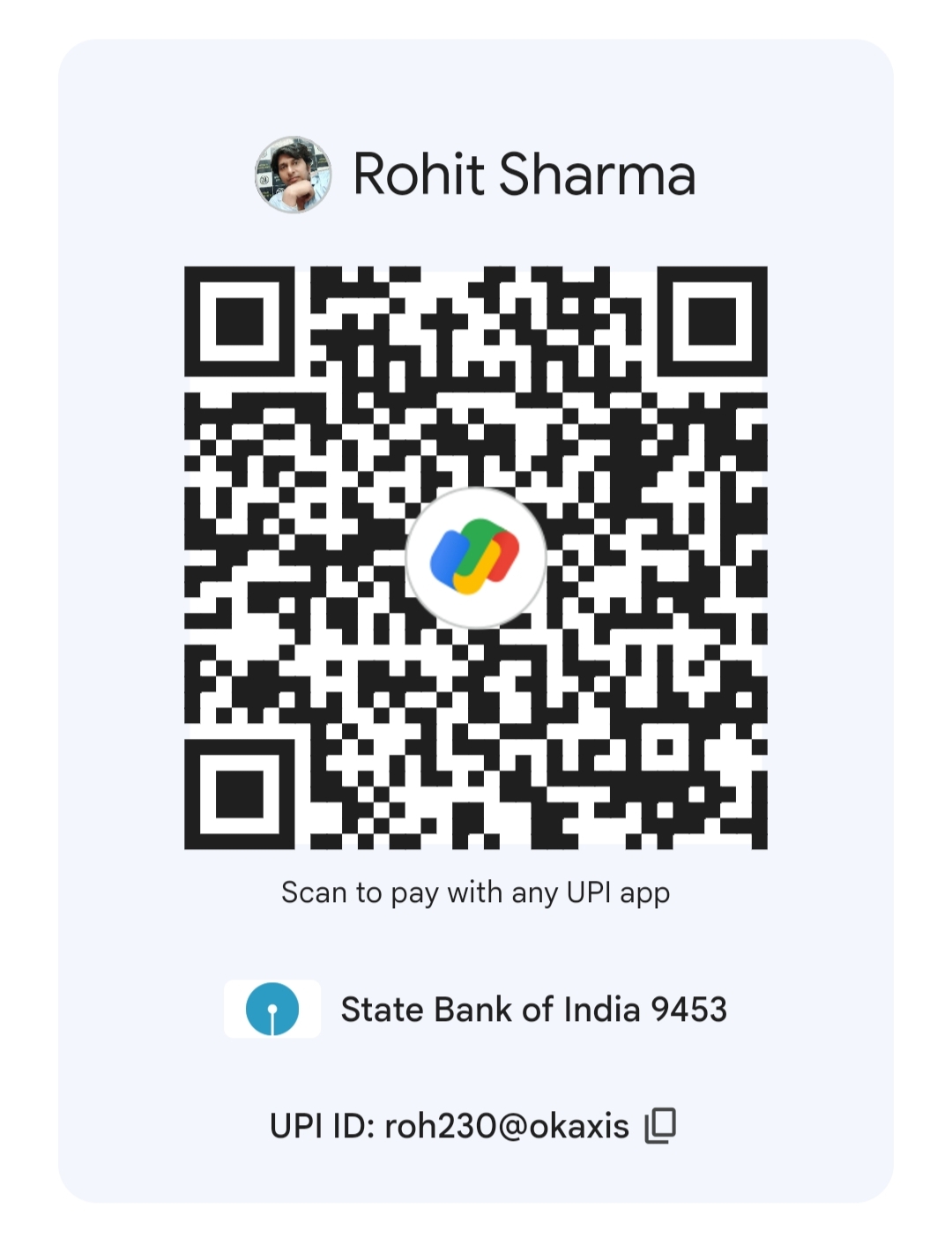अगर गांवों और शहरों में कहीं बदलाव की मांग कर रहे कुछ सैकड़ों या हजारों गरीब लोगों से हथियार छीन लिए जाएं तो क्या अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बंद हो जाएंगे ? क्या लोग अपना सिर हमेशा झुकाए रख सकते हैं जब उनका पेट और दिमाग आक्रोश से भरा हो ? क्या जो घटनाएं 1972 में पश्चिम बंगाल में नहीं घटीं, वे 2024 में दण्डकारण्य में घटेंगी ?

रक्षा खर्च के मामले में भारत अब विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है. हाल के वर्षों में, देश की सेना अविश्वसनीय गति से बढ़ी है. पिछले बजट में इस क्षेत्र के लिए करीब 75 अरब डॉलर का आवंटन किया गया था.
भारतीय नीति निर्माता बढ़े हुए रक्षा खर्च को उचित ठहराने के लिए अक्सर ‘प्रतिद्वंद्वी’ चीन और पाकिस्तान से खतरों का हवाला देते हैं. अगर सीमा पर दो देशों के हाथों कुछ सैनिक मर भी जाते हैं तो वह भारतीय मीडिया में टॉप हेडलाइन बन जाती है.
यह देश के स्वाभिमान पर प्रहार करता है और बदले की आवाज तेज़ हो जाती है. मनोवैज्ञानिक रूप से, भारत किसी भी तरह से चीन और पाकिस्तान पर सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने की होड़ में है, जिसका परिणाम उसकी सेना को मजबूत करना है.
लेकिन, आश्चर्य की बात है कि इतनी शक्तिशाली सेना दशकों से भारत के माओवादी गुरिल्लाओं से लड़ रही है. मौजूदा चुनावी तनाव के बीच झारखंड में माओवादियों के साथ झड़प की कई खबरें सामने आई हैं. किस पक्ष के कितने सैनिक मारे गए हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 48 साल बाद भी दिवंगत चीनी नेता के आदर्श भारत में कैसे जीवित हैं ? इसके पीछे सामाजिक कारण क्या है और क्या हमें जल्द ही कोई समाधान देखने को मिलेगा ?
भारत में माओवादी राजनीति और उग्रवाद के जनक में से एक चारु मजूमदार हैं, और उनके सहयोगी कानू सान्याल और जंगल संथाल थे. सभी का भाग्य बहुत पहले ही मिल गया था. हिरासत में रहते हुए, मजूमदार की हृदय रोग की आपातकालीन दवा मिले बिना ही मृत्यु हो गई. उस समय दुबले-पतले नेता पर प्रताड़ित करने के भी आरोप लगे थे. ये सब 52 साल पहले हुआ था जब कांग्रेस सत्ता में थी.
लेकिन यह स्पष्ट है कि जुलाई 1972 में कोलकाता के केओरातला श्मशान में पुलिस की निगरानी में मजूमदार का शव जलकर राख हो जाने के बाद भी विचारधारा ख़त्म नहीं हुई थी; बल्कि, इसकी विस्तार नक्सलबाड़ी से परे कहीं और की जाती थी. ‘नक्सलबाड़ी किसान शस्त्रागार’ के आयोजक-मजूमदार, सान्याल और संथाल-माओत्से तुंग को अपना गुरु मानते थे.
‘चेयरमैन माओ’ का एक उद्धरण उनका पसंदीदा था: ‘राजनीति रक्तपात के बिना युद्ध है जबकि युद्ध रक्तपात वाली राजनीति है.’ स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि भारत में आज के माओवादियों की खूनी राजनीति का स्वरूप क्या है ? और भारत सरकार पांच दशकों में इन्हें रोकने में क्यों विफल रही है ?
माओवादियों का इलाका
70 और 80 के दशक में, पश्चिम बंगाल में अपने प्रमुख आयोजकों को खोने के बाद, भारतीय माओवादी राजनीति धीरे-धीरे आंध्र प्रदेश तक फैल गई. अब इसका केंद्र मुख्य रूप से कई राज्यों के मध्य में स्थित दंडकारण्य क्षेत्र है. इसे ‘लाल गलियारा’ के रूप में भी जाना जाता है और इसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.
माओवाद का प्रभाव झारखंड और बिहार पर भी है. ये आदर्शवादी इन क्षेत्रों के अपेक्षाकृत जंगली और आदिवासी बहुल इलाकों में पाए जाते हैं. अर्थात यह समूह भारत के गरीब पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है. इन क्षेत्रों में माओवाद की पकड़ के पीछे मुख्य कारण आर्थिक अभाव है.
शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि आदिवासी गैर-आदिवासी गरीब आबादी से भी अधिक गरीब हैं. जिस तरह से आर्थिक उदारीकरण ने प्रमुख शहरों को चकाचौंध बना दिया, उसका असर आदिवासी समुदायों पर नहीं पड़ा, जो राष्ट्रीय आबादी का लगभग नौ प्रतिशत हिस्सा हैं.
सरकार का दावा है कि पिछले एक दशक में गरीबी काफी कम हुई है, लेकिन इस मामले में पूर्वी इलाके के आदिवासी इलाके राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं. शायद इसीलिए माओवाद द्वारा वादा किया गया आमूलचूल परिवर्तन इन जगहों पर अभी भी आकर्षक है. ऐतिहासिक जाति-आधारित भेदभाव के कारण भी समाज के निचले स्तर पर परिवर्तन आवश्यक हो गया है.
दंडकारण्य या आस-पास के इलाकों के बाहर, आरएसएस-बीजेपी से जुड़े अखबारों में दो शब्द, ‘अर्बन नक्सल’ व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं. यह शब्द शहरी माओवादियों को संदर्भित करता है, जिनका कार्य क्षेत्र कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में है, जो वैचारिक रूप से मानते हैं कि दक्षिण एशिया में वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था को वोटों की तथाकथित राजनीति द्वारा नहीं बदला जा सकता है.
शायद इसी वजह से जब चुनाव आता है तो नक्सली इलाकों में तनाव और छापेमारी बढ़ जाती है. शायद यह अभी हो रहा है: जबकि 19 अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में कई पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, राज्य सुरक्षा बलों को माओवादियों से लड़ने के लिए निर्धारित किया गया है.
‘शहरी नक्सलियों’ के खिलाफ लड़ाई
भारत के वर्तमान ‘सत्तारूढ़ परिवार’ द्वारा घोषित तीन वैचारिक प्रतिद्वंद्वी ईसाई, मुस्लिम और कम्युनिस्ट हैं, तीनों अल्पसंख्यक हैं. धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुख्य रूप से ईसाई और मुसलमानों को विभिन्न राजनीतिक पहलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर हाशिए पर रखा गया है.
एक समय मुस्लिम बहुल राज्य रहे जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा एक विधायी प्रक्रिया में रद्द कर दिया गया है. तीन ईसाई बहुल राज्यों-मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में लोकसभा में केवल चार सीटें हैं; 545 सीटों की लड़ाई में, ये मुद्दे कम चिंता का विषय हैं. इस बीच, चुनावों पर भरोसा रखने वाले कम्युनिस्टों का राजनीतिक दबदबा केवल केरल में ही बचा है.
वे अब पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के अपने पुराने गढ़ों में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए, अब भाजपा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं हैं. लेकिन आरएसएस परिवार अभी भी ‘वामपंथ’ को एक विशेष प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है. यह ‘माओवादी रवैये’ विशेषकर शिक्षा और संस्कृति को लेकर बहुत संवेदनशील है.
जो भी सत्ता विरोधी है उसे ‘शहरी नक्सली’ के रूप में टैग करना इस समय चलन में है. जब फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने शहरी माओवादियों को निशाना बनाते हुए फिल्म ‘बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम’ बनाई तो खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्माता को बधाई दी थी. अग्निहोत्री ने बाद में फिल्म की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए ‘अर्बन नक्सल्स’ नामक पुस्तक लिखी, जबकि भाजपा समर्थक अखबारों ने फिल्म और किताब की सराहना की.
माओवादियों को सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने का एक और प्रयास फिल्म ‘बस्तर: द नक्सल स्टोरी’ थी, जिसमें माओवाद को देशभक्ति के विरुद्ध खड़ा करने का एक कमजोर प्रयास किया गया था. उन सामाजिक-आर्थिक कारणों को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि क्यों लोग इन रचनात्मक प्रयासों में ‘परिवर्तन’ के आह्वान के प्रति आकर्षित होते हैं.
लगभग उसी दौर में ‘बस्तर: द नक्सल स्टोरी’ के निर्देशक ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ बनाई, जिसका विषय था ‘मुस्लिम समाज.’ आरएसएस परिवार ने भी इसकी सराहना की और लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकारी स्वामित्व वाले टेलीविजन चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित करने की अनुमति दी गई. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार किसकी मदद करना चाहती है.
मुसलमानों की तरह ही नक्सलियों की प्रतिक्रिया में, भाजपा और उसके आयोजकों ने हमेशा राज्य तंत्र पर अपनी सांस्कृतिक दृष्टि थोपने की कोशिश की है. शायद इसी भावना ने भारत में सुरक्षा अधिकारियों के लिए माओवादी समस्या का आधिकारिक नाम गढ़ा होगा: ‘एलडब्ल्यूई’ या ‘वामपंथी उग्रवाद.’ 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ के राजपुर में ऐसे अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि तीन साल के भीतर गांवों और शहरों दोनों से माओवादियों का सफाया कर दिया जाएगा.
अमित शाह की ओर से नई बात यह है कि उन्होंने माओवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक समय सीमा तय कर दी है. लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे लागू करना संभव है ? सुरक्षा एजेंसियों का दावा है, हां. 2005 से 2014 तक भाजपा-पूर्व की स्थिति की तुलना में, 2014 के बाद के दशक में ‘एलडब्ल्यूई आतंकवाद’ आधा हो गया है. कुल मिलाकर, अब केवल लगभग 45 जिले ही उन्हें आश्रय देते हैं.
सुरक्षा अधिकारियों के दावों पर विवाद हैं, लेकिन कुछ सच्चाई भी है. दो साल पहले की स्थिति की तुलना में माओवादियों ने बहुत कुछ खो दिया है. इस ‘सफलता’ का कारण प्रशासन और सत्तारूढ़ राजनीति के समन्वित प्रयास हैं. विभिन्न राज्य बलों द्वारा समन्वित सुरक्षा छापे के अलावा, दंडकारण्य में विभिन्न आर्थिक और सांस्कृतिक परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं.
आरएसएस परिवार ने वहां मंदिर बनाने पर बहुत जोर दिया है. धर्म-परिवर्तन पहल ‘घर वापसी’ के माध्यम से, जिन आदिवासियों को अभियान की ओर आकर्षित किया जा रहा है, उनका उपयोग माओवादियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी किया जा रहा है. इसके अलावा, आत्मसमर्पण करने वालों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी हैं.
घर वापसी का मुख्य कार्यान्वयन प्राधिकरण विश्व हिंदू परिषद है, और अभियान जिन मुख्य क्षेत्रों को लक्षित कर रहा है वे तेलंगाना, आंध्र और झारखंड हैं. इस पहल के कई समर्थकों के साथ, एक बार विभिन्न नामों के अर्ध-सैन्य बलों का गठन किया गया, जिन्होंने माओवादियों को दबाने में राज्य की सहायता की. यह आदिवासियों की मदद से आदिवासियों को बहुत हद तक रोक रहा है.
‘सलवा जुडूम’ छत्तीसगढ़ की एक ऐसी ताकत थी, जिसका गठन कांग्रेस शासनकाल में हुआ था. मानवाधिकार उल्लंघन की व्यापक शिकायतों के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समूह पर प्रतिबंध लगा दिया.
इन पहलों के अलावा, प्रशासन ने लगभग इसी उद्देश्य से एक और बड़ा कदम उठाया, वह था विभिन्न स्थानों पर प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के एक जन संगठन ‘रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (आरडीएफ) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना. इस गठबंधन जैसे संगठन ने भारत भर के विभिन्न शहरों में छात्र, श्रमिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में रेडिकल लोगों के बीच काम किया.
सरकार ने आरोप लगाया था कि हथियारबंद माओवादियों का उनके साथ वैचारिक संबंध है. लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय के अलावा संगठन के प्रमुख बुद्धिजीवियों को कई बार गिरफ्तार किया गया या उनसे पूछताछ की गई. इसके कारण शहरी क्षेत्रों में ‘माओवादी विचार’ के प्रसार में काफी बाधा उत्पन्न हुई है.
आरडीएफ का कहना है कि कलमधारी रेडिकल्स को दबाने के लिए उन्हें बंदूकधारी नक्सलियों के साथ टैग किया जा रहा है. चाहे यह दावा सही हो या गलत, आरडीएफ को खत्म करने की प्रक्रिया में भारतीय समाज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत नुकसान हुआ है. जिस तरह से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का इस्तेमाल बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा है, उस पर लोकतंत्र कार्यकर्ता विशेष रूप से आपत्ति जता रहे हैं.
हालांकि सरकार माओवादी विचारधारा-आधारित हथियारों को भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा मानती है. इसलिए, वह कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में अपने कार्यों की तरह ही इस मुद्दे से सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से निपटना चाहता है.
क्या माओवादी ख़त्म होने की कगार पर हैं ?
हालांकि भारत भर में माओवादियों के विभिन्न गुट और समूह हैं, लेकिन इस आंदोलन की मुख्य राजनीतिक ताकत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) है. किशनजी, गणपति और ‘किशन दा’ जैसे कई पुराने नेता अब मैदान में नहीं हैं; कुछ की मृत्यु हो गई है जबकि अन्य सेवानिवृत्त हो गए हैं. वर्तमान आयोजक भी डेथ वारंट के साथ मैदान पर रहते हैं.
किसी भी आपदा को रोकने के लिए सीपीआई-माओवादी नेता आमतौर पर दो से तीन स्तर का नेतृत्व रखते हैं. हालांकि सरकार द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी गई भारी मात्रा में शक्तियों को देखते हुए, दंडकारण्य के माओवादियों के लिए चल रहे अभियानों के सामने संगठित तरीके से ‘मुक्त क्षेत्र’ पर कब्जा करना मुश्किल है. कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में अपनी स्पष्ट सफलता के बाद, देश का सुरक्षा प्रशासन पूर्वी क्षेत्र में इस ‘समस्या’ पर तेजी से नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन समस्या कहीं और है.
भारत सहित दक्षिण एशिया में संपत्ति असमानता तेजी से बढ़ रही है. इस बीच, प्रमुख राजनीतिक दलों की छत्रछाया में निगम सीमांत और आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए, क्या समाज के निचले स्तर को परेशान करने वाला असंतोष और मोहभंग दूर हो जाएगा ? यदि मतदान की पारंपरिक राजनीति इन शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं देती है, तो विकल्प क्या है ?
अगर गांवों और शहरों में कहीं बदलाव की मांग कर रहे कुछ सैकड़ों या हजारों गरीब लोगों से हथियार छीन लिए जाएं तो क्या अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बंद हो जाएंगे ? क्या लोग अपना सिर हमेशा झुकाए रख सकते हैं जब उनका पेट और दिमाग आक्रोश से भरा हो ? क्या जो घटनाएं 1972 में पश्चिम बंगाल में नहीं घटीं, वे 2024 में दण्डकारण्य में घटेंगी ?
- अल्ताफ़ परवेज़ (इतिहास शोधार्थी)
- यह आलेख अंग्रेज़ी वेबसाइट ‘डेली स्टार’ पर प्रकाशित हुआ था, जिसका यह हिन्दी अनुवाद है. अनुवाद हमारा है.
Read Also –
माओवादियों के बटालियन से मुठभेड़, 12 की मौत और आजादी की कीमत
बस्तर में 12 नहीं 18 माओवादी गुरिल्ले हुए हैं शहीद, मार डाले गये 5 पुलिस, दर्जनों घायल
यदि आप संविधान, कानून, इंसानियत, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो आप नक्सलवादी और माओवादी हैं !
जब यॉन मिर्डल ने सीपीआई (माओवादी) के महासचिव गणपति का साक्षात्कार लिया
दस्तावेज : भारत में सीपीआई (माओवादी) का उद्भव और विकास
क्रूर शासकीय हिंसा और बर्बरता पर माओवादियों का सवाल
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]