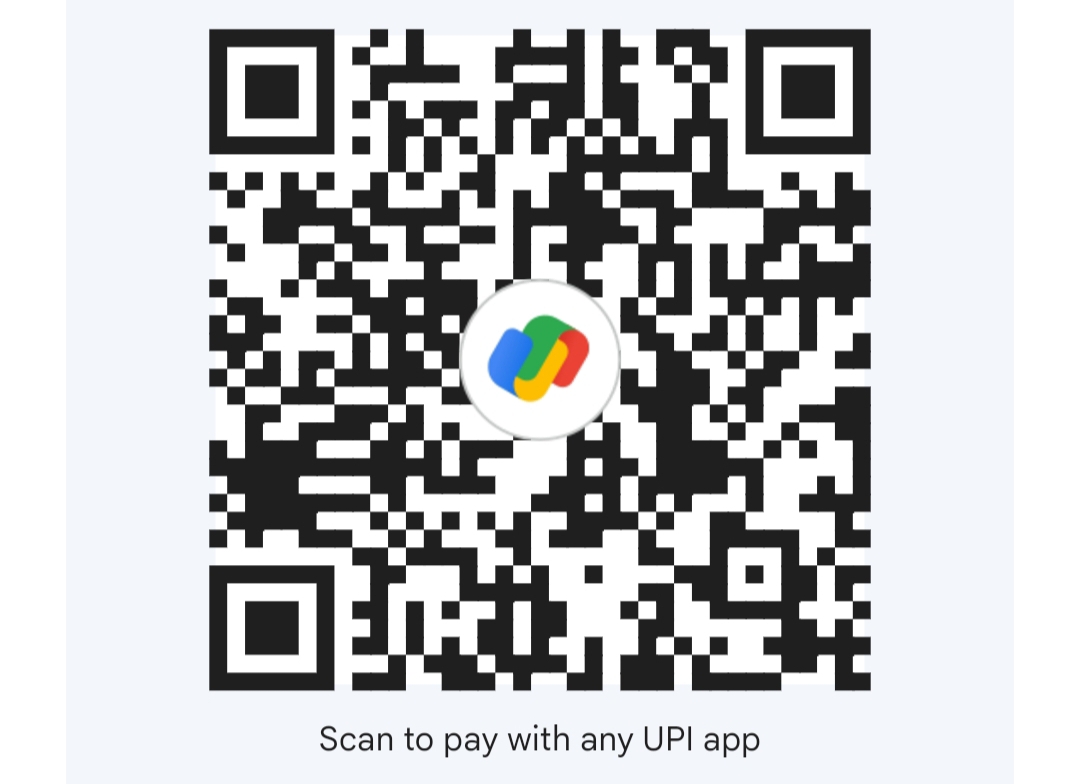तुलसीदास को हिंदी साहित्यकारों, आलोचकों ने मूलत: दो तरीके से देखा है. पहली तरह के लेखक आलोचक समझते हैं कि तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखकर हिंदू जनमानस को सबल बनाया और इस्लाम के बढते प्रभाव से क्षरित होते जा रहे हिन्दू धर्म की रक्षा कर ली. राम, लक्ष्मण, सीता आदि के चरित्रों के द्वारा हिन्दू समाज और हिन्दू संस्कृति के लिए अमिट अमर आदर्शों की प्रतिष्ठा कर दी. वहीं दूसरी तरह के लेखक आलोचक समझते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के पराभव को ब्राह्मणवाद का समर्थन करके सशक्त किया, जनता को भक्तिरूपी अफीम चटाई, उसे प्रारब्ध भरोसे रहना सिखाया, नारी की पराधीनता और अन्य प्रतिगामी प्रथाओं को आदर्श रूप में रखी…
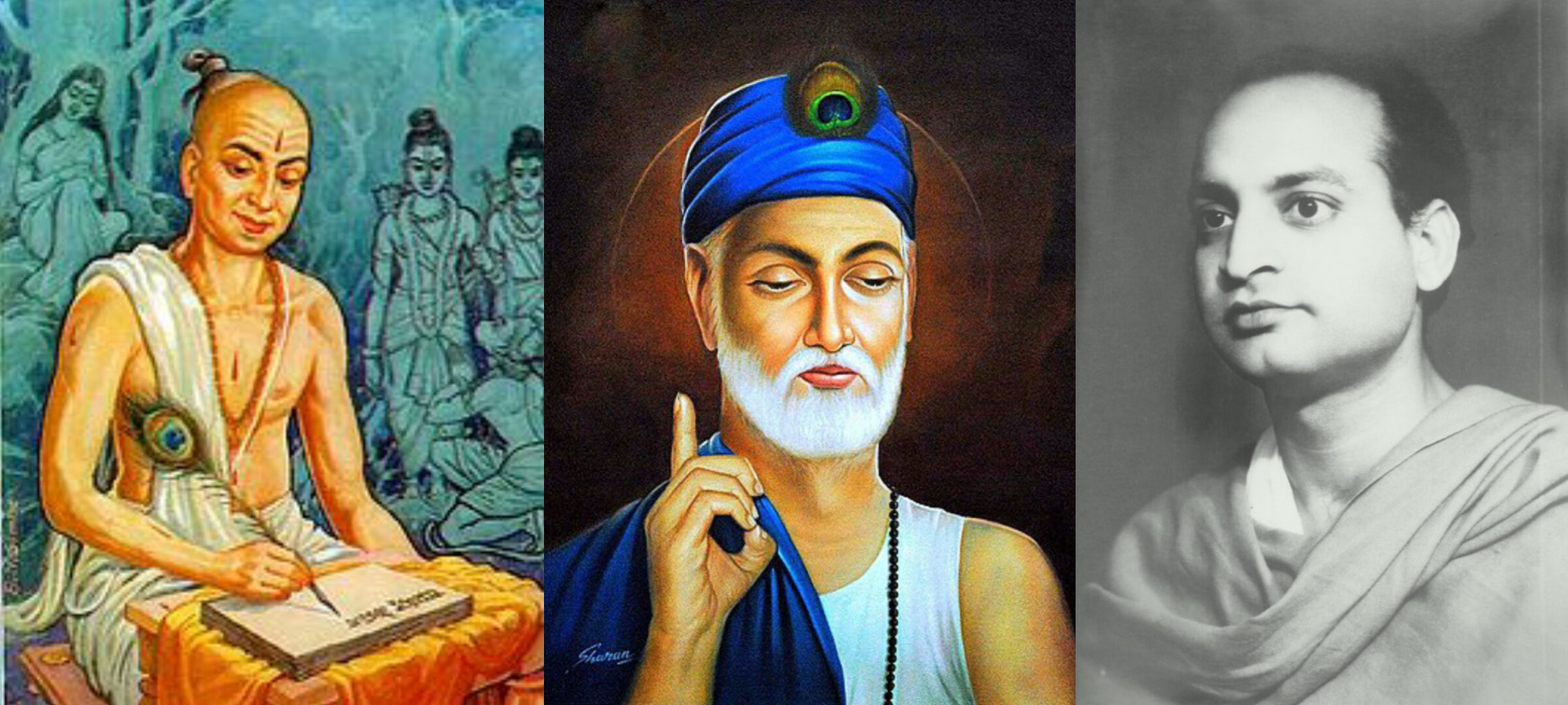
संजय कुमार श्रीवास्तव
हिंदी साहित्य से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले को रांगेय राघव और उनके साहित्यकर्म का परिचय देना शब्दों का अपव्यय होगा. उन्होंने साहित्य सृजन की अल्पावधि में जितना विशाल, विविध विस्तृत रचनाकर्म किया है वह अकल्पनीय है. रांगेय राघव ने कथा और कथेतर दोनों विधा में लेखनी चलाई.
गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय, रामानुजाचार्य, रामानुज इत्यादि के बारे में उनकी आलोचनात्मक कृतियां उल्लेखनीय हैं. कबीर की जीवनी को उन्होंने कबीर के बेटे कमाल के मुंह से कहलवाया है और पुस्तक का नाम रखा है ‘लोई का ताना.’ इसमें कबीर दास के बारे में उनका अपना दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है.
रांगेय राघव की लिखी तुलसीदास की जीवनी ‘रत्ना की बातें’ भी महज एक जीवनवृत्त नहीं है. इसमें भी रत्ना के मुख से और दूसरे चरित्रों के माध्यम से ऐसी बातें सामने आ ही जाती हैं जो रांगेय राघव की तुलसीदास के संबंध में उनके दृष्टिकोण विशेष को व्यक्त करती हैं. तुलसीदास पर उनकी एक और किताब है ‘तुलसीदास का कथा शिल्प.’
निस्संदेह उन्होंने तुलसीदास के कथा और काव्य शिल्प की ही नहीं बल्कि उनके लेखन पर समय, समाज, सत्ता तथा सांस्कृतिक वातावरण के प्रभावों के साथ साथ उनकी कथावस्तु और उसके अंतर्निहित प्रत्येक पक्ष को बहुत सूक्ष्मता से विवेचित किया है. इसमें भी तुलसीदास के बारे में उनकी पूर्वनियत मान्यताएं कहीं न कहीं परिलक्षित हो ही जाती हैं.
अपनी पुस्तक ‘संगम और संघर्ष’ में तुलसीदास को लेकर रांगेय राघव तकरीबन तीस पन्नों का एक विस्तृत विवेचनात्मक आलेख लिखते हैं, जिसमें वे तुलसीदास के बारे में अपने दृष्टिकोण को खुल कर और किंचित विस्तार से रखते हैं. हालांकि इस आलेख में वे दूसरे आलोचकों, लेखकों से अपने मान्यताओं का उल्लेख, तुलना बहुत महत्व के साथ नहीं करते परंतु वे जिस प्रकार अपनी बातों को रखते हैं इससे पता चलता है कि वे पूर्ववर्ती लेखकों के तर्कों, आरोपों, सम्मतियों का गंभीर अध्ययन कर चुके हैं.
वे इनका आवश्यकतानुसार सुतार्किक खंडन भी करते हैं. तुलसीदास के बारे में रांगेय राघव के अकाट्य तर्कों की उपेक्षा करना या उन्हें सिरे से नकारना संभव नहीं क्योंकि वे जब तुलसीदास की बात करते हैं तो महज कृतित्व या उनके कथा, काव्य शिल्प, कौशल, रचनाधर्मिता, अथवा व्यक्तित्व की ही बात नहीं करते उनके कालखंड उसकी सामाजिकता, परिवेश, सब की बात करते है और बहुधा पूर्वग्रह्मुक्त निरपेक्षता के साथ. उनकी इस विवेचना से सहमति असहमति स्वभाविक है.
असहमति सरल है पर असहमति को स्थापित करने के लिए गहन अध्ययन और पर्याप्त संख्या में उद्धरणों और उदाहरणों की आवश्यकता पड़ेगी.
रांगेय राघव ने भारतीय समाज के प्रत्येक पक्ष पर युग-सापेक्ष दृष्टि डाली है क्योंकि सत्य अटल नहीं होता, विभिन्न युगों में मनुष्य का सत्य परिवर्तित होता रहता है. उन्होंने तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व को भी देश-काल और युग-सापेक्ष रखकर देखा है इसीलिए उनकी इतिहास-दृष्टि वस्तुगत और तटस्थ प्रतीत होती है.
वे जब ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं तब ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण साम्राज्यवादियों की भरपूर भर्तस्ना करते समय भी बहुधा पूर्वाग्रहमुक्त और पर्याप्त तटस्थ दिखते हैं. उनका ध्यान सामाजिक शक्तियों और तदनुरूप उससे जुडे व्यक्तियों या उनकी कृतियों पर रहता है, वे उन्हें उन सामाजिक शक्तियों से असंपृक्त नहीं देखते.
रांगेय राघव ने कबीर, गोरखनाथ, रामानुज, तुलसीदास को जिस दृष्टिकोण से देखा वह उनका स्वतंत्र दृष्टिकोण था. तुलसीदास ने हिदी साहित्य के जितने बड़े फलक पर प्रभाव डाला है, उससे उनके बारे में कई स्वनामधन्य साहित्यकारों ने उनके बारे में अपने विचार और स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं.
बहुत से लेखकों ने तुलसीदास के बारे में रांगेय राघव से बिल्कुल उलट मान्यताएं सप्रमाण स्थापित की हैं. उनके पक्ष और पहलू से तुलसीदास रांगेय राघव के तुलसीदास से नितांत भिन्न दिखते हैं.
तुलसीदास को हिंदी साहित्यकारों, आलोचकों ने मूलत: दो तरीके से देखा है. पहली तरह के लेखक आलोचक समझते हैं कि तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखकर हिंदू जनमानस को सबल बनाया और इस्लाम के बढते प्रभाव से क्षरित होते जा रहे हिन्दू धर्म की रक्षा कर ली. राम, लक्ष्मण, सीता आदि के चरित्रों के द्वारा हिन्दू समाज और हिन्दू संस्कृति के लिए अमिट अमर आदर्शों की प्रतिष्ठा कर दी.
वहीं दूसरी तरह के लेखक आलोचक समझते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के पराभव को ब्राह्मणवाद का समर्थन करके सशक्त किया, जनता को भक्तिरूपी अफीम चटाई, उसे प्रारब्ध भरोसे रहना सिखाया, नारी की पराधीनता और अन्य प्रतिगामी प्रथाओं को आदर्श रूप में रखी.
पहली तरह के आलोचकों लेखकों के लिए तुलसीदास हिन्दू धर्म के उद्द्धारकर्ता और श्रद्धेय हैं. दूसरी तरह के लेखकों आलोचकों के लिए वे प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी विचारधारा वाले हैं. रांगेय राघव इसी दूसरी तरह के लेखकों की गिनती में आते हैं. मार्क्सवादी रचनाकारों द्वारा तुलसीदास के मूल्यांकन से धर्मप्राण जनता और पाठकों में विवाद की स्थिति बनी.
रांगेय राघव के विचार भी वाम विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं परंतु वाम विचारों के करीब रहने वाले रामविलास शर्मा मानते हैं कि, दोनों तरह के लेखक आलोचक-श्रद्धा अश्रद्धा के बावजूद – लगभग ‘एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ‘तुलसीदास जर्जर होती हुई सामन्ती संस्कृति के पोषक थे, इसलिए आज की जातीय संस्कृति के निर्माण में – ‘ऊंची’ जाति और ‘नीची’ जाति के हिन्दुओं, मुसलमानों आदि की मिली-जुली संस्कृति के निर्माण में – उनकी विचारधारा कोई मदद नहीं कर सकती.’ पर इसके साथ ही वे यह टिप्पणी भी देते हैं कि, ‘दोनों तरह के आलोचक भारतीय जनता को- खासकर हिन्दी भाषी जनता को- तुलसीदास की सांस्कृतिक विरासत से वंचित कर देते हैं.'[1]
रांगेय राघव तुलसीदास को समग्रता वाली दृष्टि से देखते हैं. तुलसीदास के किसी एक दोहे अथवा एकाध प्रसंग निरूपण, चरित्र चित्रण को वह भी समय संदर्भ से विलग कर देखना उचित नहीं जैसा वर्तमान में ढोल, गवार, सूद्र, पशु, नारी ।।। जैसे दोहे और उसके ‘ताड़ना’ शब्द के साथ हो रहा है. रामचरित मानस और तुलसीदास को लेकर विवाद की जड़ में यही प्रवृत्ति है.
यदि तुलसीदास को समय संदर्भ के साथ, उक्त कालखंड की सामाजिकता, आवश्यकता और परिस्थितियों के तदनुरूप देखें, तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व को परखने के निकर्ष में ये तत्व भी समाहित करें तो निस्संदेह जो धारणा बनेगी वह सकारात्मक या नकारात्मक नहीं वरन सत्य के समीप होगी.
इसलिए हिदी साहित्य के अध्यत्ताओं के लिये यह जानना आवश्यक है कि जब हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रचा गया तब उस कथा के और कौन से रूप उपस्थित थे, महाकवि की मानसिक दशा, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी और इस महाकाव्य का तात्कालिक उद्देश्य क्या था. परिस्थिति को अध्ययनपूर्वक देखने के पूर्व सिद्धांत बनाकर उस पर अपना पूर्वग्रही राग अलापना संकीर्णातावाद कहा जाएगा.
इतिहास वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहता है इसीलिये किसी कवि का मर्म समझने के लिये उसके उस रूप को अवश्य जान लेना चाहिये, जिसके द्वारा उसने संसार से और उसकी सामाजिक प्रक्रिया से उसने अपना संबंध निर्धारित किया है, क्योंकि यदि वह एक ओर समाज से प्रमावित हुआ है, तो दूसरी ओर उसने समाज को प्रभावित भी किया है ! तुलसी ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं.
इस प्रकार के तथ्यों की पड़ताल तुलसीदास और उनके रामचरित मानस के बारे में बहुत से अनजाने तथ्य उजागर करता है. रांगेय राघव लिखते हैं, ‘तुलसीदास उस कालखंड में सक्रिय हुए जब सामंतकाल में उच्छृंखलता का बोलबाला था. ऊंची जातियों के अतिशय शक्तिसम्पन्न सामंती वर्ग का हाथ था क्षत्रिय और मस्तिष्क था ब्राह्मण. इसके विरुद्ध बराबरी के लिये नीची जातियों का संघर्ष उक्त वर्ग की दृष्टि में उच्छृंखलता थी.
तुलसीदास का विचार था कि रामायण भूल जाने से समाज का ढांचा ढीला पड़ गया है, वह उच्छृंखल हो गया है. फिर से रामकथा लिखी जाए तो संभव है समाज का सामंतीय ढांचा फिर सशक्त हो जाए.'[2] यही सोच कर तुलसी ने रामकथा का चयन किया. रांगेय राघव लिखते हैं कि, ‘तुलसीदास और उनका रामचरित मानस नीची जातियों का ब्राह्मणों या ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उठे स्वर को समाप्त करने का महत्वपूर्ण और सफल उपकरण बना.
तुलसी के राम ने वीर रूप में समाज की उस उच्छृंखलता का नाश किया जो ब्राह्मणबाद के विरुद्ध थी. उसका नाश ही वे कलि का नाश कहते थे. इस तरह बराबरी तथा अधिकारों की मांग को लेकर उपजी नीची जातियों के विद्रोह के शमन के साथ संकटाकीर्ण ब्राह्मणवाद पुनर्स्थापित हुआ और चूंकि इस विद्रोह के अतिरिक्त सामंतकाल में सब कुछ सुव्यवस्थित था. अधिकारी वर्ग के सामने कोई समस्या नहीं रही, वह स्त्री के साथ विलास और रति में डूब गया, रीतिकाव्य प्रस्फुटित हुआ.'[3]
इस तरह रांगेय राघव की दृष्टि में तुलसीदास ब्राह्मणवाद के प्रबल समर्थक थे. उनके अनुसार तुलसीदास द्वारा ब्राह्मणवाद को फिर से जागृत करने का यत्न प्रतिगामी है. कई तर्कों पर रांगेय राघव से विपरीत राय रखने वाले राम विलास शर्मा भी मानते हैं कि :ह्रासकालीन सामंतकाल में जनवादी आन्दोलनों को कुचलना नितांत प्रतिगाामी कृत्य था.'[4]
विवरण मिलते हैं कि उस समय वाल्मीकि रामायण के अलावा संवृत रामायण, अगस्त्य रामायण, लोमश रामायण, मंजुल रामायण, सौपद्य रामायण, रामायण महामाला,रामायण मणिरत्न, सूर्य्य रामायण, चांद्र्य रामायण, मैंद रामायण, स्वाम्भुव रामायण, सुब्रह्म्य रामायण, सुवर्चस रामायण, देव रामायण, श्रवण रामायण, दूरंत रामायण, रामायण चम्पू और आध्यात्म रामायण इत्यादि उपलब्ध तो थे ही 18 पुराणों और महाभारत में भी रामकथा किसी न किसी प्रकार से मौजूद थी.
तुलसीदास ने इनमें से कितनों को पढा किसका अनुसरण किया कहा नहीं जा सकता. रांगेय राघव लिखते हैं, ‘तुलसी में आश्चर्यजनक गुण था कि वे वस्तु को अपना बना कर आत्मसात कर लेते थे. उन्होंने श्रीमद्भागवत के वर्षा वर्णंन को प्राय: ज्यों का त्यों–दामिनि दमक रही धन माही, खल की प्रीति यथा थिर नाहीं, वाले प्रसंग में उतार लिया है, परन्तु वह ऐसे सहज किया है कि पूरी की पूरी नकल होने पर भी तुलसी की प्रशंसा करने की इच्छा होती है, उन्हें नकलची कहने की नहीं.'[5]
निस्संदेह इन रामकथाओं के रहते एक युगव्यापी विषय को चुन कर ऐसी रामकथा रचने का दुष्कर कार्य संपन्न किया, जिसमें सामाजिक नियमन, शास्त्रर प्रतिपादन, दार्शनिक विवेचन करते हुये ऐसा धर्मपुराण लिखा जिसका काव्य सौंदर्य अत्यंत श्रेष्ठ और संदेश भी युगानुरूप था.[6]
बहुतों का विचार है कि तुलसीदास ने संस्कृत के विरुद्ध हिन्दी में लिखकर धोर प्रगतिवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया. उन्होंने ब्राह्मणों, पंडितों की भाषा संस्कृत को त्याग कर जनभाषा में रामचरित मानस लिख कर उन्हें सीधी और साहसिक चुनौती दी. इस पर रांगेय राघव कहते हैं, ‘अंग्रेज कहा करते थे कि अस्पताल और रेल बनाकर हमने भारत का कल्याण किया, वर्ना हमें तो इससे नुकसान ही है.
‘यह सच है कि रेल और अस्पताल बनाकर अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान का बहुत फायदा किया. लेकिन इसमें याद रखने की बात है कि अंग्रेजी पूंजी ने इन दोनों से बेहद फायदा उठाया और उनका राज्य इन बातों के बल पर और जमा, अवधि बढ़ी. इतिहास में यह देखा गया है कि एक वर्ग किसी बात को अपने फायदे के लिए करता है, लगता है कि वह दूसरे वर्ग के लाभ के लिये है. हिन्दुस्तान के ब्राह्मणवाद का इतिहास यही बताता है.
‘वैदिक देवता छोड़ कर आयों ने अनार्य देवताओं की पूजा शुरू की. जब उससे भी काम नहीं चला तो कृष्ण ने शुद्रों को रियायतें दीं. आगे चल कर कौटिल्य ने दासप्रथा का प्रायः अंत कर दिया. उसके बाद शंकराचार्य ने बौद्धों के शून्य को ब्रह्म का रूप देकर स्वीकार कर लिया. इसी परम्परा में हुए तुलसीदास.’
तुलसीदास द्वारा पंडितों के प्रखर विरोध के बावजूद जनभाषा में रामचरितमानस लिखा लेकिन इसके लिए उनको प्रगतिशील मानने से पहले यह देखना होगा कि बुद्ध ने भी अपने समय में क्रान्ति की और ब्राह्मण परम्परा की भाषा को अपनाने से अस्वीकार कर दिया.
बहुत दिन बाद सिद्धों और नाथों ने उसी परम्परा को चलाया और जनभाषा में लिखते रहे. कबीर, जायसी आदि में वही धारा फूट कर पलती रही. बुद्ध, सिद्ध, नाथ, कबीर, जायसी का विद्रोह ब्राह्मण व्यवस्था के प्रति था. ब्राह्मण व्यवस्था जाति-पांति को लेकर सामंतीय व्यवस्था का ही दूसरा नाम थी.
रामानुजाचार्य, रामानन्द, श्रीमद्भागवत आदि ने लचीलापन दिखाया ओर कुछ अधिकार दलित वर्गों को दिये. रामानुज ने ही चमारों को तिरू-नारायणपुर के मंदिर में घुसा दिया था. रामानंद ने इसी परंपरा में कबीर को चेला बनाया था. भागवत संप्रदाय के लोकप्रियता का आधार ही रियायतें थीं.
इनके प्रयत्न सतह पर तो तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग-अधिकारों के विरुद्ध दिखता था लेकिन वास्तविकता यह थी कि भीतर ही भीतर ये ब्राह्णवाद का नया संगठन खड़ा करना चाहते थे, भक्ति की लहर से वेदविरुद्ध पुरुष को आवृत कर दिया और समाज को आगे बढ़ा ले गये. क्या तुलसीदास ने उपयुक्त दो बातों में से कुछ किया !
तुलसी ने निम्न वर्गों को अपनी ओर जीतने की चेष्टा को दर्शाया जरूर लेकिन उन्हें श्रधिकार दिलाने का कोई का प्रयत्न नहीं किया. उन्हें अपनी बात सुनाने की बात तो की, पर उन्हें बन्धन से छुड़ाने का यत्न नहीं किया, वरन् तत्कालीन उच्च वर्ग के लोग जो कहते थे, वही लिखा. संस्कृत की जगह जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, उससे केवल रूप या फार्म बदला वस्तु विषय या कंटेंट में कोई बदलाव नहीं आया. बल्कि और भी रूढ़ता से पुनः वही पुरानी बातें प्रतिस्थापित की गई. तुलसीदास ने इस्लाम के विरुद्ध पूरी दीवार खड़ी कर दी पर इसी के साथ ब्राह्मणवाद को भी जागृत कर दिया.[7]
उनके अनुसार जनभाषा में लिखकर तुलसी ने लचीलापन इसलिये दिखाया क्योंकि संस्कृत के माध्यम से पहुंच कम रहती. बहुतायत वाला निम्नवर्ग तो उससे छूट जाता. तब संस्कृत बहुत थोड़े से सामंती लोगों के और मुट्ठी भर ब्राह्मणों की भाषा थी, यहां तक अधिकांश ब्राह्मण स्त्रियां भी संस्कृत बोल लिख नहीं पाती थीं. हिंदी या जनभाषा के माध्यम से जनता तक रामचरित मानस और ब्राह्मणवाद को पहुंचाया, उसे शक्तिशाली बनाया.
रांगेय राघव लिखते हैं, ‘सो उन्होंने हिन्दी में लिखा, पर प्रश्न उठता है कि लिखा क्या ? उसमें ब्राह्मणों की निंदा की गई ? स्त्रियों, शुद्रों से सहानुभूति दिखाई गई ! उसमें कबीर का स्वर तो था ही नहीं; उसमें वह भी नहीं था जो रामानुज ओर रामानन्द अथवा भागवत में था. तुलसी ने भक्ति की लहर में ब्राह्मणवाद को ढीला नहीं किया, वरन् उसे जटिल किया.
‘निम्न वर्ग की निंदा और हमदर्दी का लेखा-जोखा करके कहा कि वास्तव में वेदपथ भूल जाने के कारण यह सब हुआ है. भागवत ने भक्तिहीनता के कारण ब्राह्मण की निंदा की थी, भक्ति को ऊंचा कहा था. पर तुलसी ने कहा कि भक्ति अच्छी है और वही अच्छी है जो वेद सम्मत है. सबसे बड़ा भेद तो यही है कि तुलसी ने हिन्दी का प्रयोग जनहित के लिए इतना नहीं किया जितना ब्राह्मणवाद के पुनर्संगठन के लिए.'[8]
तुलसी ने जनभाषा में लिखकर पंडितों की धरोहर को नष्ट किया और उनके विरुद्ध इतना बड़ा विद्रोह अचरज की बात थी, ऐसा रांगेय राघव नहीं मानते, ‘उस समय तुलसीदास का हिंदी या भाषा में लिखना न तो ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्रोह था, न कोई अचरज या अत्यधिक प्रगतिशीलता का प्रमाण. ब्राह्मणों के अतिरिक्त हिंदी में बहुत लोग लिखते थे. हिंदी की अपनी परम्परा थी.
‘तुलसी से पहले भी जनभाषा खूब समृद्ध थी. उससे पहले स्वयंभू, देवसेन, पृष्पदत्त, बब्बर, हेमचन्द्र भाषा में लिख चुके थे. उनके ही दोहे चौपाईयों का विकसित रूप तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है. तुलसी का ब्राह्मणवाद को हिंदी में प्रस्तुत करना निस्संदेह उनका लचीलापन था, पर प्रगतिवादी नहीं, क्योंकि वही जटिल व्यवस्था प्रस्तुत की. सूर ने भी तो हिंदी में लिखा फिर उन्हें प्रगतिवादी क्यों नहीं कहा जाता ?'[9] ध्यातव्य है कि तुलसी ने संस्कृत की जड़ पर पहला कुठाराघात नहीं किया था. तुलसी से पहले कबीर ने कहा था – संसकिरत है कूप जल, भाषा बहता नीर.
तुलसी ने यह नहीं कह सके. ऐसा भी नहीं है कि तुलसीदास ने संस्कृत का अपमान करके हिंदी को आसन दिया हो. ‘यह स्पष्ट है कि तुलसी में संस्कृत के प्रति मोह था. उसे वे देवभाषा समझते थे. रामचरितमानस में प्रयुक्त श्लोक तथा स्तुतियां, विनयपत्रिका में बहुला पदावली, शिवस्तुति, रामस्तुति, सब संस्कृत में होना प्रमाण है कि तुलसी ने रामचरित मानस के लिये संस्कृत रणनीतिक कारणों से छोड़ी थी.'[10]
रांगेय राघव लिखते हैं, ‘उस युग में रीतिकवि केशव और तुलसी के अतिरिक्त किसी कवि में इतनी संस्कृत नहीं है. उन्होंने न सिर्फ़ नई बोतल में पुराना आसव दिया, वरन् बोतल को जब ढाला तब उसमें भी पच्चीकारी करके पुराने कांच के टुकड़ों को बीच बीच में जड़ दिया.
पुराणकार की परम्परा में वैदिक छोड़ कर, लौकिक संस्कृत के बाद, हिंदी को अपनाया. इस प्रक्रिया में जहां थोड़े से जड़ नियमकार उच्चवर्ग-बाह्मणों की ईच्छा से परे जाकर संस्कृत के विरुद्ध विद्रोह किया, पर इसके माध्यम से उन्होंने समस्त उच्च जातियों को एक किया और समूचे उच्चवर्ग को वह शक्ति दी कि विद्रोह दब गया. उच्चवर्ग का धर्मपक्ष दृढ़ हो गया. ब्राह्मण व्यवस्था फिर सुदृढ़ हो गई.'[11]
समाज के वर्ग और एक युग ने सिर उठाया था, अकेले तुलसीदास उसे झुका कर ब्राह्मणवाद को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते थे.
जनभाषा सामूहिकता का प्रभावी उपकरण हो सकती थी, भाषा तो प्रचलित थी ही. केवल ब्राह्मण वर्ग अपने संकोचों में बद्ध था. इस्लाम के विरुद्ध ब्राह्मणों को नेता बनाकर समस्त प्रजा का संगठन करने के लिए ब्राह्मणवाद को नये रूप की आवश्यकता थी. अतः उन्होंने हिन्दी को लिया.
तत्कालीन कट्टर उच्चवर्ग ने प्रारंभ में संस्कृत के स्थान पर हिन्दी रखने का विरोध इसलिए किया कि भाषाओं का प्रयोग कर तुलसी घर्म को सर्वसुलभ बनाकर उनकी जीविका छीन रहे थे. रांगेय राघव के अनुसार, ‘वे ब्राह्मण अपने तुच्छ स्वार्थ में थे. मध्यकाल के मुस्लिम-शासन के युग में अपने धर्म को संस्कृत के माध्यम से प्रचालित करते थे; पुराण सुनाते थे और अपने धर्म को जन-भाषा में ज्यों का त्यों जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए डरते थे. वह गलती उन्होंने जल्दी महसूस की और उनके जीवन के अन्तिम काल में ही ब्राह्मणों ने उनके सामने सिर झुका दिया और स्वीकार किया कि तुलसी ने धर्म के उद्धार के लिये ही भाषा को अपनाया था और वे ब्राह्मणवाद के लिये गहरी नींव खोद उसे मजबूत कर रहे थे.'[12]
तो इस प्रकार ब्राह्मणों की संकुचित सीमा को तोड़ कर ही तुलसी ने ब्राह्मण संस्कृति को सशक्त बनाया. इसलिये तुलसी ने भाषा के केवल तद्भव रूप को ही नहीं लिया, उसमें उन्होंने तत्सम शब्दों को बहुत घुसेड़ा. रांगेय राघव दूसरे लेखकों द्वारा स्थापित इस तर्क को भी मानने से मना करते हैं कि तुलसीदास ब्राह्मणों अथवा विधर्मियों तथा समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा प्रताड़ित और पीड़ित व्यक्ति थे, जिनका बचपन और युवावस्था निर्धनता में बीता.
तुलसीदास के समय में शैवों और वैष्णवों के बीच बहुत मतभेद था. शिव के दो रूप थे, एक वेद सम्मत और दूसरे वेद वाह्य. तुलसीदास ने जब शिव कहा है तो वेद ग्राह्य शिव को लिया है. वेद बाह्य के शव अघोरी, नाथ संप्रदाय वाले थे, जो वेद स्वीकृत शैव थे वे वेदों को स्वीकारते थे, पर विष्णु को नहीं मानते थे.
तुलसी ने इस पहले शैव वर्ग को विष्णु भक्तों के समीप कर दिया. यह तुलसी के चलते हो सका क्योंकि दक्षिण भारत में अब भी शैव और वैष्णब उतने समीप नहीं हैं. वेद ग्राह्य शैव सम्प्रदाय जाति प्रथा को मानता था जबकि ब्राह्मणबाद का धुर विरोधी वेद बाह्य शैव सम्प्रदाय जाति-पांति नहीं मानता था.
तुलसीदास ने जात पात और ब्राह्मणवाद विरोधी इस संप्रदाय को घृणित अघोर कहकर हतोत्साहित किया. वेद वाह्य शैवों का आहार विचार तुलसीदास को सह्य न था –
असुभ वेष भूषन धरे, भच्छाभच्छ जे खाहि।
तेई जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलियुग माँहि ॥
इसके अलावा उन्होंने लिखा –
कलिमलि ग्रसे धर्म सब, लुप्त भए सद्ग्रंथ
दम्भिन निज मत कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ
यानी दंभियों ने अपनी सोच से अनेक पंथ पैदा कर लिए हैं क्योंकि कलियुग में सद्ग्रंथ लुप्त हो चले हैं. कहते हैं तुलसीदास ने आडंबर का विरोध किया पर रांगेय राघव का मत है कि यह आड़ंबर विरोध नहीं था बल्कि जो जांत पांत और ब्राहमणवाद को खुली चुनौती दे रहे थे, खास तौर पर नाथ सम्प्रदाय, यह उन पर प्रहार था.
जाके नख और जटा विसाला
सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला
हालांकि कबीर ने भी कहा था–
जटा बढ़ाय जोगी होय गैले बकरा ।
पर कबीर ने उनके आडम्बर का विरोध किया था, उसका विरोध नाथों के उस चिन्तन से नहीं था, जो समाज में जाति-पांति का विरोधी था. गोरखपंथी कहते थे, ‘ना मैं हिंदू ना मुसलमान’, पर तुलसी दास का मत था, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग. यानी गोरखनाथ के योग प्रवर्तन ने लोगों को भक्ति से विमुख कर दिया. बौद्धों का विरोध करके वे प्राय; ब्राह्मणवाद का पोषण ही कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हठयोग को राजयोग से मिला दिया था –
सूद्र द्विजहि उपदेसहि ग्याना,
मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ।
या
बादहिं सूद्र द्विजन्ह संग , हम तुम्हते कछु घटि
जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आंख देखावहिं डांटि
तुलसीदास को बुरा लगता था कि शूद्र ब्राह्मण की बराबरी और उससे बहस करे –
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा
स्वपच किरात कोल कलवारा
नारि मुई गृह संपतिनासी
मूंडि मुडाई होईं सन्यासी
ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं
उभय लोक निज हाथ गवांवहि
अर्थात तेली कुम्हार जो चाहे वही सिर मुड़ा कर सन्यासी बन गया है और ब्राह्मणों से अपने को पुजवा कर स्वयं अपने दोनों लोक नष्ट कर रहा है. उनकी चिंता यह भी है कि –
सूद्र करहि जप तप नाना
बैठि बरासन कहत पुराना
इन सब के बावजूद रांगेव राघव मानते हैं कि, तुलसीदास ने सगुण, निर्गुण, शैव वैष्णव बैर, राम कृष्ण भेद सबको मिटाने का काम किया. तुलसी ने सब को बहुत ऊंचा उठा कर, सबका ही दूसरा रूप राम को प्रमाणित करके, राम को सबसे ही ऊपर उठा दिया है. तुलसीदास ने आकर देश की परिस्थिति को यों समझा – मुस्लिम शासक भारत पर छाए हैं. हिन्दू सामंत नतशिर हैं, वर्णाश्रम धर्म लुप्त होने से ब्राह्मण के अधिकार और लाभ क्षीण हो रहे हैं. प्रजा और किसान पीड़ित हैं.
यह घोर कलियुग किसी सुयोग्य स्वधर्मी शासक के आने, जातीय उत्थान, वर्णाश्रम धर्म को फिर से स्थापित करने से ही संभव है, परन्तु जनता अनेक पंथों के बीच भ्रमित है. ज्ञान मार्गियों और भक्ति मार्गियों का समन्वय समाधान हो सकता है, पर जो मार्ग वेदमयी मार्ग को नहीं स्वीकारता, वह त्याज्य है. इसी बात का द्योतक था –
जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिये ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही.
जब सामंतीय व्यवस्था में ब्राह्मणों के अत्याचारों से दुखी प्रजा ने भक्ति आंदोलन चलाया तब विरोधी ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद सामने थे. पर इसके चरम काल में जब तुलसी आए तब परिस्थिति बदल चुकी थी. सब को इस्लाम के सर्वोपरि शासन ने दबा लिया था. इसीलिये ‘तुलसीदास ने दो काम किये : पहला कि भारतीय संस्कृति यानी यहां ब्राह्मणवादी संस्कृति को ऊपर उठाया और इस्लाम के विरुद्ध मोर्चा खड़ा किया. साथ ही ब्राहणवाद के अंदरूनी द्वेष विभेद मिटाए, वर्णाश्रम स्थापित किया और प्रजा में सामंतीय ढांचा प्रतिस्थापित किया.
वेद ग्राह्य शिव-भक्तों और निर्गुण को वेद की कसौटी पर आंक कर तुलसीदास ने साथ लिया. इस कार्य ने नाथ संप्रदाय, कबीर संप्रदाय आ्रादि की उस बोली को बिल्कुल दबा दिया जो ब्राह्मणवाद का विरोध करती थी. तुलसीदास पुरातन गौरव की स्मृति के साथ इस्लाम के विरोध में स्वर उठाया और वर्णाश्रम धर्म को फिर से स्थापित कर पंथवाद का नाश किया. इसके बाद उच्चवर्गों को संतोष मिल गया. यह तुलसीदास का ऐतिहासिक कार्य था.
हालांकि वेद- पुराणों के जिन आदेशों के विरुद्ध नीच जातियों ने ईश्वर को अपना कहकर ‘भक्ति आंदोलन चलाया, उसी की भक्ति को तुलसी ने भी लिया, पर समस्त निम्न जातियों के संतों ने जिन वेद शास्त्र पुराण का विरोध किया था, तुलसी ने उसे स्थापित किया. निस्संदेह बुद्ध के बाद तुलसी के अलावा कोई इतना प्रभावशाली नहीं हुआ जो समस्त उत्तर भारत को अपनी वाणी से गुंजा देता.'[13] परन्तु प्रश्न उठता है कि निम्न वर्गों ने तुलसी की रामचरित मानस को इतना महत्व क्यों दिया ?
रांगेय राघव उत्तर देते हैं, ‘इसलिये कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस के उत्तर काएड में जिस आदर्श सामंतीय राज्य की कल्पना की, वह इस्लामी शासकों और उनके छुटभैये हिंदू सामंतों की लूट के सामने स्वर्ग सी दिखाई देती थी.'[14] तुलसीदास के नये दृष्टिकोण के बाद ही भारत में श्रमजीवी वर्ग ने सिंख, मराठी, जाट इत्यादि के रूप में विशाल मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सिर उठाया, जो कि अब तक हिंदू सामंतों के कंधों पर टिका हुआ था.
रांगेय राघव मानते हैं कि तुलसी दरबारी कवि नहीं, संत थे, समाज सुधारक थे और संसारत्यागी थे. ‘स्वांत:सुखाय’ लिखते थे. उनके स्वांत सुखाय लेखन को किसी जनवाद से जोड़्ना दूर की कौड़ी है. इस स्वांत सुखाय का अर्थ इतना भर समझे कि तत्कालीन कवि धनार्जन हेतु राजाओं के चाटुकार थे, पर तुलसी एक धर्मगुरु थे, किसी राजा के कहने से नहीं, अपने मन मुताबिक लिखते थे. तुलसी के स्वांतःसुखाय का जो अर्थ था उसमें वे जनवादी परंपरायें नहीं आती जिनमें कबीर थे. तुलसी तो पुराणकार परंपरा में आते हैं.
रांगेय राघव इस बात के साथ निष्कर्ष निकालते हैं कि, ‘उनके द्वारा किए वैज्ञानिक विवेचन तुलसी का निरादर नहीं, वह उसी तरह सत्य है जैसे यदि हम कहते हैं कि कबीर ने मनुष्यता का पाठ पढ़ाया परन्तु वे शून्य की खोज में रहते थे, तो हम उनका अपमान नहीं करते, वरन् वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं. तुलसीदास सिद्ध हैं, महान् हैं, कवि हैं, अतः उनका गलत विवेचन करके प्रगतिवादियों में नाम लिखाना हमारा कर्तव्य नहीं है. अधकचरे मार्क्सवादी उनको काफी विकृत कर रहे हैं. तुलसी ने इस्लामी शासकों का विरोध करके, कुछ बुरा नहीं किया. वे सबसे बड़े शोषक थे, हां तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म को जो प्रतिस्थापित किया इसका कारण वे यही समझते थे कि इसी से समाज ठीक हो सकता है.
तुलसी को जनवादी साबित करके ही क्या उनकी महत्ता प्रकट होती है ! विद्यापति, चंद में कौन सी जनवादिता थी. यह बात का बतंगढ़ ही व्यर्थ है. इतिहास को अपने दृष्टिकोण के लिये विकृत करना ही नहीं चाहिए.'[15] आचार्य शुक्ल ने भक्ति को जो निराशा की आशा मानकर गलती की थी कुछ आलोचकों ने उसी में से तुलसी का जनवाद ढूंढ़ निकाला, जिसकी हां में हां मिलाना आजकल के अवसरवादी तथाकथित या मार्क्सवादियों का ध्येय हो गया है, हमें उसके प्रति सदा सचेत रहना है क्योंकि उसके बिना हम कभी तुलसी की वास्तविक महानता को नहीं समझ सकेंगे.
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कबीर को समझने के लिये पूरा नहीं तो कुछ तो कबीर होना पड़ेगा.[16] रांगेय राघव के लेखन, जीवन में किंचित कबीरपन झलकता है. कबीर की जीवनी में कमाल के रूप में रांगेय राघव उपस्थित हैं और बहुत सहजता तथा भाव प्रवणता के साथ कबीर के जीवन दर्शन का मनोवैज्ञानिक वर्णन करने में सफल रहे. किताब में कमाल जुलाहे कबीर को कालजयी संत बनने की कथा जो कथा कह सकता है, जीवनी में कहता है. शेष रांगेय राघव पुस्तक की भूमिका में कहते हैं.
रांगेय राघव के अनुसार तुलसी दास और कबीर दोनों की अपनी महत्ता है लेकिन दोनों के काव्य, विषय और प्रभाविकता में कोई साम्य नहीं. नीची जाति में अनाम माता पिता द्वारा जन्म देने के बाद परित्यक्त्य, अनजाने निसंतान दंपति द्वारा पालित, हिंदू मुसलमान दोनों द्वारा उपेक्षित, आर्थिक अभावों से अतिशय त्रस्त होने के साथ अंतर्द्वंद की पीड़ा से ग्रस्त, परम सत्य की खोज के अथक यात्री जिस पर पुत्र, पिता, पति की भूमिका निर्वाह की जिम्मेदारी हो और जो लाखों का पथद्र्ष्टा भी हो उसके जीवन और दर्शन को रांगेय राघव ने बहुत स्पष्टता के साथ रखा है.
उनके अनुसार ‘कबीर पहले अवतरवाद मानते थे. निम्नजातीय हिंदू बन कर रहना चाह्ते थे पर रमानंद की दीक्षा के बाद जांतपांत से ऊपर उठ गए. फिर निर्गुण की ओर बढे, उसके बाद योगियों के रहस्यवाद, षटचक्र साधना वगैरह की तरफ. इस प्रक्रिया में वे चमत्कारवाद से आगे बढ गए. कबीर में सूफीमत, वेदांत, रहस्यवाद, नारीनिंदा जैसी अनेक बाते हैं जो बहस तलब हैं. कबीर पर नारी विरोधी, और दूसरे कई आरोप लगे वह निराधार थे और अधिकांश ब्राह्मणवाद से प्रेरित.[17]
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे ब्राह्मणवादी आलोचक कबीर को नीरस निर्गुणिया बताते हुए कहते हैं कि वे कोई राह नहीं दिखाते, उनका ज्ञान आम जन के लिये रहस्य में डुबोने वाला और अबूझ है.[18] यह ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, अवैज्ञानिक और त्याज्य है. लोई और कबीर के सहज रिश्तों के जरिए रांगेय राघव ने कबीर के नारी विरोधी होने के धब्बे को धोया है –
सब रसायन मं किया, प्रेम रसायन न कोय
रति एक तन में संचरै सब तन कंचन होय
जोई मिले सो प्रीत में और मिले सब कोय
मन सो मनसा ना मिले देह मिले का होय[19]
रांगेय राघव ने कबीर के प्रेम की ऐसी अद्वैत और पवित्र कल्पना के जरिए भी उनकी नारी विरोधी धारणा और व्यक्तित्व को बचाया है.
कबीर के राम कौन हैं, राघव लिखते हैं – लोई मैं और तू दो नहीं हैं. मैं तेरी वेदना को जब समझता हूं तब मुझे लगता है कि मैं राम के पास पहुंच गया हूं. तेरी विरह की शक्ति ही मेरी जड़्ता और अहंकार को नष्ट करती है. तू होती है तो मैं राम को अपने में पाता हूं, मुझे फिर तृष्णा नहीं रह जाती.[20]
कबीर की राह मनुष्यता को कल्याण पथ पर ले जाने वाला था. वे भारतीय संस्कृति के नाम पर भेदभाव वाले ब्राह्मणवाद को नहीं मानते थे. इस्लाम का विरोध करने के बावजूद उससे घृणा नहीं करते थे पर उसे मुक्ति का पथ भी नहीं समझते थे. कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों पर आक्रमण किया. कबीर ने दलित जनता को एक जुलाहे की तरह देखा था. तुलसी दास की तरह नहीं वे. सगुण ईश्वर को मानकर ब्राह्मणवाद में नहीं बंधे. तुलसी के विपरीत कबीर ने भाग्य से ज्यादा कर्म पर जोर दिया और बिना मेहनत के खाने वाले साधुओं को लताड़ा. कबीर की भाषा क्रांति थी. उन्होंने तुलसी की तरह इसमें कभी संस्कृत की बैसाखी या पैबंद नहीं लगाया.
तुलसी के देवता संस्कृत बोलते थे जबकि कबीर अच्छे सामाजिक आचरण पर जोर दिया. तुलसीदास सारी अवनति की जड़ कलि को मानते थे. कबीर ने कलि का शायद ही कभी नाम लिया बल्कि मोह, लोभ, दम्भ, धन, माया, को अनाचार का मूल मानते थे. कबीर का मुख्य ध्येय प्रेम का है0तुलसी का तर्कातीत भक्ति का.[21]
कबीर के चेलों ने ब्राह्मणॉं की नकल की और इस तरह से कबीर का विद्रोह और सत्य दबा दिया गया. जैसे संसार की असारता पर जोर, मायावाद का वर्णन, कबीर के ये विचार अनेक विकास की मंजिलें हैं. वे धीरे धीरे आगे बढे है. वे कितने आगे बढ गये हैं, यह समझना तब और अधिक अचरज में डाल देता है जब हम यह सोचते हैं कि कबीर सैकड़ों बरस पहले हुए थे. साधारण जनता ने कबीर को समझा और उसी ने कबीर को मुल्ला, मैलबियों पंडित, जोगी, पुरोहितों से बचाया और बाद में जीवन भर कबीर जिस पंथ का विरोध करते रहे, मरने के बाद बेटे कमाल के विरोध के बावजूद बना, फिर कबीरपंथियों ने ही कबीर को मिटा दिया.[22]
संदर्भ
- रामविलास शर्मा, परम्परा का मूल्यांकन, पृ 0- 74, संस्करण – 2004, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- रांगेय राघव, संगम और संघर्ष, तुलसीदास एक दृष्टिकोण पृ-34 से 72 संस्करण 1953, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद
- वही
- रामविलास शर्मा, मार्क्सवाद, साहित्य और प्रगतिशील, पृ.- 239, संस्करण – 1984, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
- रांगेय राघव, संगम और संघर्ष, तुलसीदास एक दृष्टिकोण पृ-34 से 72 संस्करण 1953, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद
- रांगेय राघव तुलसीदास का कथा शिल्प संस्करण 2015, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली
- रांगेय राघव, ग्रंथावली, पृ.- 217-218
- वही
- रांगेय राघव, संगम और संघर्ष, तुलसीदास एक दृष्टिकोण पृ-34 से 72 संस्करण 1953, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद
- वही
- वही
- रांगेय राघव रत्ना की बातें भूमिका संस्करण 1954 विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- रांगेय राघव, संगम और संघर्ष, तुलसीदास एक दृष्टिकोण पृ-34 से 72 संस्करण 1953, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद
- वही
- रांगेय राघव रत्ना की बातें भूमिका संस्करण 1954 विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ.- 43, संवत-2059, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
- हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास, पृ.- 59, 21 वीं आवृत्ति , 2010 राजकमल प्रकाशन , नई दिल्ली
- रांगेय राघव, संगम और संघर्ष, तुलसीदास एक दृष्टिकोण पृ-34 से 72 संस्करण 1953, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद
- वही
- रांगेय राघव लोई का ताना, भूमिका संस्करण 1957 विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
- रांगेय राघव लोई का ताना, भूमिका, संस्करण 1957 विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
- रांगेय राघव तुलसीदास का कथा शिल्प संस्करण 2015, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली
- रांगेय राघव लोई का ताना, भूमिका संस्करण 1957 विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
Read Also –
तुलसी और रहीम की मित्रता : तलवार दिखाकर, जबरन जयश्रीराम बुलवा कर तुम राम और हिन्दू धर्म का सम्मान कर रहे हो ?
हिंदु, हिंदू-शब्द और हिंदू-धर्म
कबीर : इंसान और इंसानियत के सच्चे प्रतीक और प्रतिनिधि
आरक्षण पर चन्द्रचूड़ : ब्राह्मणवाद जब जब संकटग्रस्त होता है, कोई बाभन अवतारी भेष में आता है
सनातन धर्म का ‘स्वर्णकाल’ दरअसल और कोई नहीं बल्कि ‘मुगलकाल’ ही था
(संशोधित दस्तावेज) भारत देश में जाति का सवाल : हमारा दृष्टिकोण – भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]