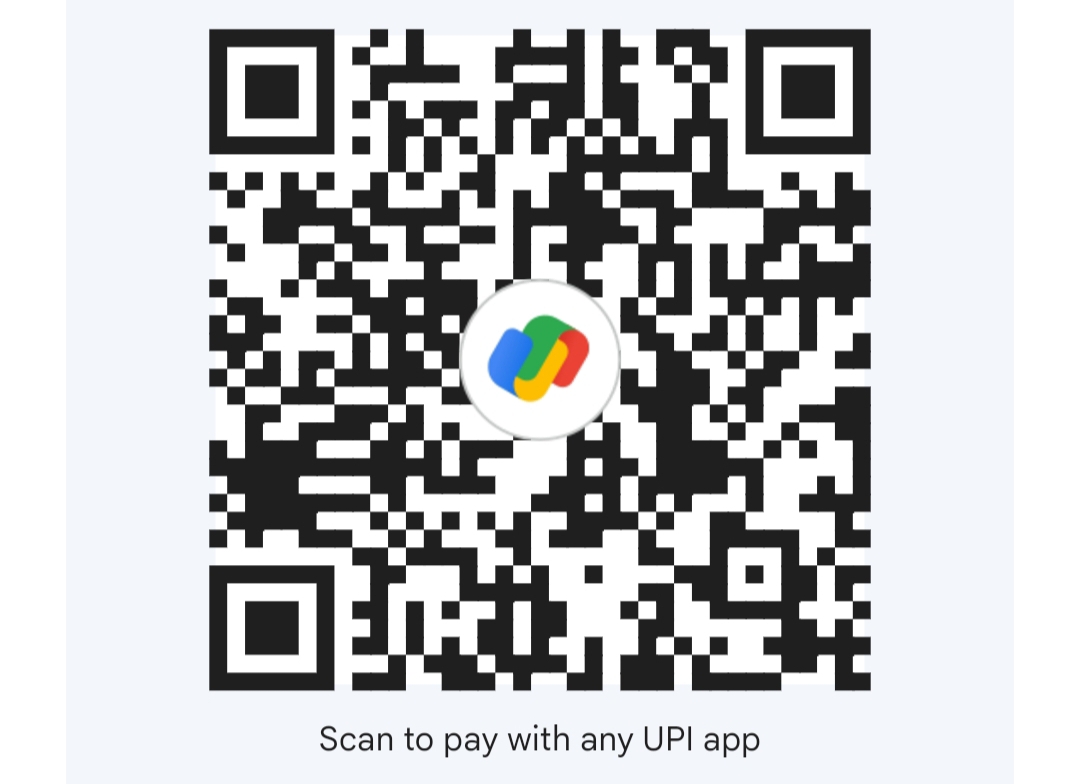चंद्रभूषण
हाथ में खोपड़ी लिए सड़क पर समूह में नाचते लोगों की आखिरी सार्वजनिक छवि कोई पांच दशक पुरानी है. वे खुद को आनंदमार्गी कहते थे और उस पंथ के एक सज्जन कुछ समय के लिए मेरे पड़ोसी भी थे. उनका परिवार शाम को दीया जलाकर ‘बाबा नाम केवलम’ का सामूहिक कीर्तन करता था. गुप्त रूप से उनके यहां कोई खोपड़ी रखी भी हो तो उसे वे कभी निकालते नहीं थे. जहां तक ध्यान पड़ता है, प. बंगाल में आनंदमार्गियों के खिलाफ काफी लंबा पुलिस एक्शन हुआ था और वे अंडरग्राउंड हो गए थे. इन लोगों का सुदूर अतीत में कभी कोई जुड़ाव कापालिकों से था या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बात अभी उसी पर करनी है. और हां, यह तंत्र पर जारी काम का हिस्सा नहीं है.
कापालिक पंथ मुख्यतः एक शैव पंथ था और आज भी शिव की मसानी छवि के लिए यह कुछ हद तक जिम्मेदार है. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वज्रयानी बौद्धों का एक हिस्सा भी खुद को कापालिक कहता था. समुदाय के रूप में इसका असर अभी औघड़ों से लेकर कश्मीर के कौलों तक देखा जाता है. लेकिन एक पंथ के रूप में यह बहुत पहले क्षीण होकर नाथपंथ में विलीन हो गया. 1000 ई. के आसपास, आदि-मध्यकाल में हुए कापालिक पंथ का जिक्र उस समय के संस्कृत महाकाव्यों में आम तौर पर भय और जुगुप्सा से ही जुड़ा मिलता है. हाल में एक किताब पर काम करते हुए कापालिकों से सामना हुआ तो लगा कि उनसे जुड़े एक छोटे से हिस्से का यहां उल्लेख किया जा सकता है.
एक लुप्त पंथ का मुकाम
‘संदेश रासक’ में एक और दिलचस्प बात कापालिकों के जिक्र से जुड़ी है. किताब में कुछ हिंदू तीर्थों के अलावा किसी और धार्मिक पंथ को लेकर कोई कोई चर्चा नहीं है लेकिन कापालिकों का उल्लेख दो बार आया है. छंद संख्या 46 पूरी तरह कापालिकों के रूपक पर आधारित है. इस छंद में विरहिणी अपने पति को जो संदेश दे रही है, यहां उसका केवल अर्थ प्रस्तुत है- ‘हे कापालिक, तुम्हारे विरह ने विरहिणी को कापालिनी बना दिया है. तुम्हारे मोह की समाधि में रहती हूं. जैसे कापालिक के हाथ से कपाल नहीं छूटता, वैसे ही मेरे बाएं हाथ से कभी मेरा सिर नहीं छूटता. कापालिकों के सिद्धासन और खट्वांग की ही तरह मैं अपना शय्यासन और खटिया का पावा नहीं छोड़ती.’
फिर काफी बाद में, छंद 183 में एक बार फिर यही जिक्र उठता है- ‘कावालिय कावालिणि तुय विरहेण किय.’ हे कापालिक, तुम्हारे विरह ने (मुझे) कापालिनी बना दिया है. एक अर्से से भारत के काव्य जगत में कापालिकों को भय और जुगुप्सा से ही देखा जाता रहा है. त्रिशूल पर खोपड़ी टांगे, खोपड़ी में ही भोजन करने वाले, पशुबलि के अलावा जब-तब नरबलि को भी सिद्धि-प्राप्ति का जरिया बना लेने वाले खतरनाक लोग.
भवभूति के चर्चित नाटक ‘मालती-माधव’ में आए कापालिक अघोरघंट और कापालिनी कपाल कुंडला से लेकर माधवाचार्य की रचना ‘श्रीशंकर दिग्विजय’ में अपनी बातों से उन्हें श्रीपर्वत क्षेत्र में आत्मघात के बहुत पास तक पहुंचा देने वाले कापालिक आचार्य तक, यूं कहें कि 8वीं से 14वीं सदी ईसवी तक यह प्रस्थापना, बिना किसी दुविधा या आंतरिक द्वंद्व के, एक ही तरह से आती दिखती है.
‘संदेश रासक’ के जैसी इज्जत से, इतने वांछनीय ढंग से कापालिक युगल का जिक्र इस पंथ से जुड़े ग्रंथों के अलावा साहित्यिक संदर्भ में कहीं और सुनने को मिलता है तो वह है 11वीं सदी ईसवी में ही चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के समवर्ती कृष्ण मिश्र का रूपकीय नाटक ‘प्रबोध चंद्रोदय.’
शिवप्रसाद सिंह के उपन्यास ‘नीला चांद’ में ये कृष्ण मिश्र एक चरित्र की तरह आते हैं. उनके इस नाटक में एक कापालिक युगल को आपसी बहस में उलझे बौद्ध और जैन भिक्षुओं को असल विराग समझाते और दोनों को अपने विशिष्ट शैव मत में लाते दिखाया गया है. संदेश रासक के उलट यहां कापालिकों का संदर्भ प्रेम जैसे किसी बुनियादी मानवीय रिश्ते का नहीं, फलसफे का है.
यहां रेखांकित करना जरूरी है कि बाहर की सारी भयावहता के बावजूद कापालिक पंथ में शैवों के अलावा बौद्धों की भी भागीदारी थी. कृष्णपाद या कान्हपा, जिन्हें बौद्ध धर्म के वज्रयान पंथ और नाथपंथ, दोनों में बराबर की इज्जत हासिल है, दावे के साथ खुद को कापालिक घोषित करते हैं- ‘आलो डोंबि तोए सम करिबो मो साङ्ग, निघिन काह्ण कापालि जोइ लाङ्ग.’ कान्हपा का समय दसवीं सदी ईसवी का माना जाता है और काठमांडू में मिली प्रतिष्ठित वज्रयानी प्रार्थना पुस्तक ‘चर्यापद’ में सबसे ज्यादा पद उन्हीं के हैं.
बौद्धों और नाथपंथियों के बीच
हिंदी साहित्य के इतिहास की आलोचनात्मक समझ में वज्रयानियों और कापालिकों के प्रति नकारात्मकता भरी पड़ी है, लेकिन ‘संदेश रासक’ में एक ललित रूपक की तरह कापालिकों की उपस्थिति यह संकेत देती है कि 10वीं सदी ईसवी में बौद्धों के मुख्यधारा से हटने और 12वीं सदी में नाथपंथी योगियों के उनकी जगह लेने के बीच आम लोगों की दृष्टि कापालिकों के प्रति सहज हो गई थी.
मृत्यु से जुड़े प्रतीक हमेशा अनजान लोगों को बेचैन कर देते हैं. मेक्सिको में खोपड़ी की शक्ल वाली आइसक्रीम देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके कि यह प्रतीक वहां 1821 से 1910 तक जमीन के लिए संघर्ष करने वाले किसानों पर वहां की सरकार और सामंती शक्तियों द्वारा किए गए अमानुषिक दमन और प्रतिरोध से पैदा हुआ है. बौद्ध कापालिकों के लिए खोपड़ी अनित्यता, विराग और बुद्धत्व का प्रतीक थी. श्मशान में रहना बौद्ध भिक्षुओं के लिए और स्वयं बुद्ध के लिए भी एक आम बात थी.
शैव कापालिकों में इसके पीछे विनाश में निर्माण और विराग में राग वाला वही भाव था जो अभी छन्नूलाल मिश्र के गाए उस चर्चित बनारसी फाग में जाहिर होता है- ‘खेलैं मसाने में होरी दिगंबर, खेलैं मसाने में होरी.’
वेदमार्गी इसे अशौच मानते थे लेकिन डरने-डराने से इसका कोई लेना-देना नहीं था. बहरहाल, गृहस्थों के लिए यह प्रतीक कभी बहुत सहज नहीं रहा होगा और भक्ति तथा सूफिज्म के जोर पकड़ने के साथ ही त्याज्य होता गया होगा. महमूद गजनवी के पीछे-पीछे भारत की खोज-यात्रा पर निकले बौद्धिक अलबरूनी के यहां कापालिकों का जिक्र मिलता है. उसके सौ साल बाद उभरनी शुरू हुई सूफियों की धारा में जहां-तहां योगियों के संदर्भ जरूर मिलते हैं लेकिन कापालिक उनके यहां इस तरह गायब हैं, जैसे वे कभी भारत में थे ही नहीं.
भारत के हिंदी इलाके में भक्ति आंदोलन से बने नए संदर्भ को छोड़ दें तो एक तरफ गांधार, पंजाब और सिंध तक और दूसरी तरफ नेपाल, असम, बंगाल तक उत्तर-मध्य भारत के दोनों सांस्कृतिक छोरों पर बारहवीं से पंद्रहवीं सदी तक नाथपंथी योगियों का बोलबाला रहा. इन इलाकों में सूफी इस्लाम से उनकी एक तरह की संगति भी बनी रही. यह सिलसिला देर तक चला. अफगानिस्तान में गोरख के गीत गाने वाले मुस्लिम जोगियों का जिक्र हजारीप्रसाद द्विवेदी की 1942 में छपी किताब ‘नाथ संप्रदाय’ में विस्तार से आया है जबकि सिंध में नाथपंथियों के गाए गाने आज भी यूट्यूब पर छाए रहते हैं.
पच्छिम का राग-विराग
सूफिज्म का रचाव सबसे ज्यादा पंजाबी संस्कृति में रहा, लेकिन वारिसशाह की अमर रचना ‘हीर’ में भी नायक रांझे को वियोग में योगी होता ही दिखाया गया है- ‘रांझा जोगी हो गया.’ नाथपंथ से जुड़े चरित्र पूरन भगत का जिक्र हाल में दिवंगत हुए पंजाबी कवि सुरजीत पातर की एक मशहूर गजल में बहुत सुंदर ढंग से आया है- ‘कते नूर नूं कते नार नूं कते बादशा दी कटार नूं, जाईं दूर ना मेरे पूरना तेरी हर किसे नूं उड़ीक है.’
‘संदेश रासक’ के विरह वर्णन में दो बार कापालिकों की बात आने से ऐसा लगता है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र की संस्कृति में नाथपंथी जोगियों का जोर बढ़ने से पहले यह विशाल जगह कापालिकों ने ही भर रखी थी. लोगों के मन में निजी संपत्ति की मारामारी से दूर, विराग वाली जगह सबसे पहले यहां बौद्ध भिक्षु भरते थे, फिर थोड़े समय तक वज्रयानी साधुओं और कापालिकों ने भरी, फिर कई सदियों तक योगी इसे भरते रहे.
पश्चिमी भारत के सूफिज्म की सांस्कृतिक भव्यता और रचनात्मकता का शायद यही मुख्य कारण है. हीर-रांझा, सोहनी-माहीवाल, मिर्जा-साहिबां जैसी रचनाएं राग-विराग की जिस अद्भुत केमिस्ट्री से निकलती हैं, उसका बीज रूप संदेश रासक में भी मौजूद है.
बहरहाल, विशेष बात यह कि नाथपंथियों ने ईसा की 11वीं सदी बीतते न बीतते कापालिकों को खुद में पूरी तरह से समेट लिया था. ‘श्रीशंकर दिग्विजय’ का शंकराचार्य-कापालिक संवाद नाथ-साहित्य में अलग तरह से आता है. वहां कापालिक आचार्य शंकर को वाकई शिरोच्छेद तक ले जाता है और इस क्रम में जीवन और मृत्यु का अंतर मिटाकर उन्हें जीव और ब्रह्म के अद्वैत का वास्तविक अर्थ समझा देता है.
नाथपंथ और कापालिक मत का एक-दूसरे के साथ और समय के साथ यह रिश्ता ‘संदेश रासक’ के काल निर्धारण में भी सहायक सिद्ध हो सकता है. इस रूप में कि किसी योगी का जिक्र अगर वहां बिल्कुल नहीं आता और कापालिकों का दो बार आता है तो इस रचना में मौजूद समाज 11वीं सदी के पूर्वार्ध का ही हो सकता है. रही बात मुल्तान में इस्लामी संस्कृति की मौजूदगी और हिंदू संस्कृति के साथ उसका कोई टकराव न होने की, तो इस बारे में कुछ दिलचस्प सूचनाओं पर हम आगे बात करेंगे.
दो बहुत पुराने ‘भगत’ और सूमरो राज
सिक्खों का सबसे प्रतिष्ठित धर्मग्रंथ ‘गुरु ग्रंथ साहब’, जो दसवें गुरु गोविंद सिंह के बाद इस धार्मिक समुदाय के लिए एक जीवित गुरु की भूमिका निभाता है, बारहवीं से सोलहवीं सदी तक के मध्यकालीन भक्ति काव्य की एक प्रामाणिक एंथोलॉजी भी है. इसमें संग्रहीत कुल 15 भगतों की बानियां दस गुरुओं के वचनों जितनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. इन भगतों में दो सबसे पुराने नाम बाबा फरीद (1173-1266 ई.) और सधन कसाई (1180 ई.-अनिश्चित) के हैं. दोनों के नाम पर बनी दरगाहें और मस्जिदें आज भी मौजूद हैं और उनके मुसलमान होने में कोई शक नहीं है, लेकिन दोनों की आस्था परंपरा एक-दूसरे से बहुत अलग है और इतिहास-भूगोल में आपस की बहुत करीबी होने के बावजूद दोनों के बीच परस्पर संवाद या आस्थागत विमर्श की कोई सूचना कहीं नहीं है.
हमारे ‘संदेश रासक’ के किस्से से इन दोनों भगतों की कहानी दो बिंदुओं पर जुड़ती है. एक तो दोनों का संबंध दक्षिणी पंजाब के शहर मुल्तान और वहां से लगभग चार सौ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित सिंध के शहर सेहवण शरीफ (पास का बड़ा शहर हैदराबाद) से है. दोनों जगहें मोटे तौर पर संदेश रासक में वर्णित भूक्षेत्र में ही आती हैं. दूसरे, दोनों का शुरुआती समय उस दौर से जुड़ा है, जिसे मुनि जिनविजय ने मोहम्मद गोरी के हमले (1175 ई.) और मुल्तान की पारंपरिक संस्कृति तथा समृद्धि की स्थायी बर्बादी वाला बताया है. इस दौर की कुछ-कुछ गूंज हमें दोनों ‘भगतों’ की कविता में सुनाई पड़ सकती है, जो संदेश रासक के विपरीत आज भी गुम होने से बची हुई है.
बाबा फरीद का जन्म मुल्तान से दस किलोमीटर दूर कोठेवाल नाम की जगह में हुआ था और उनका समय गोरी सल्तनत का बताया जाता है. युवावस्था में ही उनकी मुलाकात बगदाद से दिल्ली जा रहे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हुई और वे उनके चिश्तिया सूफी सिलसिले का हिस्सा बन गए. इसमें यह सूचना भी छिपी है कि मुल्तान की स्थिति उस समय एशिया के कुछ बहुत खास रास्तों के चौराहे जैसी थी.
बाबा फरीद ने भारत में सूफी मत का ठेठ देसीकरण कर दिया. उनके काव्य में कोई अलग धार्मिक रंग खोजना असंभव है और उठते-बैठते यह हर पंजाबी की जुबान पर होता है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो या सिक्ख हो- ‘बिरहा बिरहा आखिए बिरहा हूं सुल्तान, जा तन बिरह न ऊपजै ता तन जान मसान.’ (विरह-विरह कहते हो, विरह सभी भावों का राजा है. जिस शरीर में विरह नहीं उपजता, उसे श्मशान समझना चाहिए.) या फिर, ‘रोटी मेरी काठ दी लावां मेरी भुक्ख, जीना खांदी चोपड़ी घणे सहेंगे दुक्ख.’ (मेरी रोटी काठ की है लेकिन मेरी भूख जला देने के लिए वह काफी है. जो हमेशा चिकनी-चुपड़ी ही खाते हैं उन्हें बहुत दुख सहने होंगे.)
सधन कसाई को हम सधना कसाई और सधना भगत के नाम से भी जानते हैं. नाम से ही जाहिर है कि उनका काम जानवर काटकर उसका मांस बेचने का था. गुरु ग्रंथ साहब में उनका एक पद संकलित है और भक्ति की सगुण और निर्गुण, दोनों ही धाराओं में उनकी कविता तो नहीं लेकिन उनका नाम खूब चलता है. मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी कमाने वाला एक भक्त, जिसका ईश्वर से निस्संग लगाव उसको मुक्ति तक ले गया.
कबीरपंथी कथाओं में उन्हें कबीर का शिष्य कहने का रिवाज है, हालांकि उनका समय कबीर से दो सदी पहले का स्थिर किया जा चुका है. वैष्णव धारा में सधन कसाई को शालिग्राम का उपासक कहा जाता है. एक किस्सा एक वैष्णव संत द्वारा उनके यहां से मांस तौलने वाले बाट के रूप में पड़े शालिग्राम को उठाकर अपने यहां लाने, फिर सपने में मिले ईश्वरीय संदेश के मुताबिक शालिग्राम को उसी सधना के पास ही छोड़ आने का सुनाई पड़ता है. दूसरा किस्सा उनके द्वारा किसी भी पत्थर की पूजा के विरोध का भी चलता है.
पंजाब के सरहिंद कस्बे में उनके नाम पर एक मस्जिद बहुत पहले से बनी हुई है. उनकी वैष्णव आस्था को लेकर कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता. कह सकते हैं तो इतना ही कि सभी उन्हें अपना मानते थे. एक सुंदर दोहा उनके नाम से जोधपुर प्राचीन संस्थान के ‘भगत बानी संग्रह’ में दर्ज है- ‘प्रीतम तुमरे दरस को हमरे नैन अधीन, तड़फ तड़फ जिउ देत है जिउं बिछरे जल मीन.’ और गुरु ग्रंथ साहब में संकलित उनके अकेले सबद की आखिरी पंक्तियां हैं- ‘मैंहो करमी तुम मेटना औगुन सब मेरा, कूरा कपटी रामजी सधना जन तेरा.’
बहरहाल, यहां दोनों भगतों के जिक्र का एक अलग उद्देश्य भी है, और वह यह कि मुल्तान और सेहवण शरीफ, दोनों ही इनके जन्म के थोड़ा पहले तक जिस शासन के तहत आते थे, उसे इतिहास में सूमरो, सुम्रा, सुम्रः या सूमरा जाति के राज के रूप में याद किया जाता है. इस जाति के ही किसी वंश का शासन मुल्तान में था, जो 1175 ई. में मोहम्मद गोरी के हमले के बाद चला गया, लेकिन सेहवण शरीफ में यह बचा रहा और सधना भगत के परिचय में इसका उल्लेख मिलता रहा. इनका जिक्र सिर्फ एक जगह, अबुल हसन अली के फारसी रोजनामचे ‘दीवान-ए-फर्रूही’ में आता है, जो अब कहीं नहीं मिलता, लेकिन उसके उद्धरण हर जगह छाए रहते हैं.
ऐसे ही एक उद्धरण में बताया गया है कि सन 1025 ई. में सिंध पर महमूद गजनवी के आखिरी हमले में वहां का अरब इस्माइली राजवंश समाप्त हो गया और स्थानीय सूमरों ने सत्ता पर कब्जा करके इसका पूरी तरह सिंधीकरण कर दिया. अलग-अलग वर्तनी के साथ मिलने वाले इस जातिनाम से जुड़ी बहुतेरी कहानियां हैं. कहीं इन्हें अरबों और सिंधियों की मिश्रित नस्ल कहा जाता है, कहीं जाट, कहीं सोढा तो कहीं परमार राजपूत. लेकिन समझ यही बनती है कि यह जातिप्रथा से बाहर कोई कबीला था और सिंध में मौजूद लंबे अरब इस्माइली शासन के दौरान इसने इस्माइली मिजाज का ही शिया धर्म अपना लिया था.
सबसे बड़ी बात यह कि सिंध-मुल्तान की इस शासक जाति की जीवन पद्धति में अपने इस्लाम-पूर्व हिंदू-बौद्ध अतीत के लिए पूरा सम्मान मौजूद था और इन धर्मों के रीति-रिवाज और धर्मस्थल यहां पूरी तरह सुरक्षित थे.
1175 ई. में मोहम्मद गोरी के मुल्तान पर हमले के पीछे असल वजह लाहौर में गजनवी वंश की जड़ें खोदने का बहाना तैयार करने की थी, लेकिन हमले के लिए निकलने से पहले उसने इसका मकसद मुल्तान जैसे ‘दारुल इस्लाम’ में कुफ्र का खात्मा करने का घोषित किया था. यहां पहुंचकर संदेश रासक में बटोही संदेशवाहक द्वारा किए गए अपने शहर समोरु के कलमतोड़ वर्णन को एक बार फिर से याद करें. क्या समोरु का सूमरो, सूमरा, सुम्रा या सुम्रः से कोई ध्वनिसाम्य समझ में आता है ? खासकर यह देखते हुए कि अबुल हसन अली का फारसी रोजनामचा बहुत पहले लुप्त हो चुका है और उससे दिए जाने वाले उद्धरणों में मिलने वाले जातिनाम की मात्राएं स्थिर नहीं हैं ?
संदेश रासक पर काम करने वाले साहित्यिक समालोचक समोरु नाम के शहर का कोई सिर-पैर नहीं खोज पाए हैं और इतिहासकारों के लिए यह कभी एजेंडे पर ही नहीं रहा. यह भी हकीकत है कि सिंध और दक्षिणी पंजाब के अर्ध रेगिस्तानी मिजाज वाले शहरों के बनने-बिगड़ने और छोटे-बड़े होते रहने का एक इतिहास रहा है. ऐसे में मेरा एक प्रस्ताव है कि स, म और र, तीन अक्षरों से बनने वाले इस शहर और जाति के नामों को जोड़कर देखने का प्रयास किया जाए. यह सही है कि एक कवि की कल्पना पर कोई सीमा आयद नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बाकी स्थान-नाम अगर वास्तविक हैं- विजयनगर, मुल्तान और खंभात- तो सिर्फ एक को, वह भी कहानी के कुल दो मुख्य चरित्रों में से एक के बहुप्रशंसित गृहनगर को ‘सांबपुर’ जैसा काल्पनिक नाम देने का कोई तुक नहीं बनता.
- ‘संदेश रासक’ पर केंद्रित एक लंबे निबंध का हिस्सा
Read Also –
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]