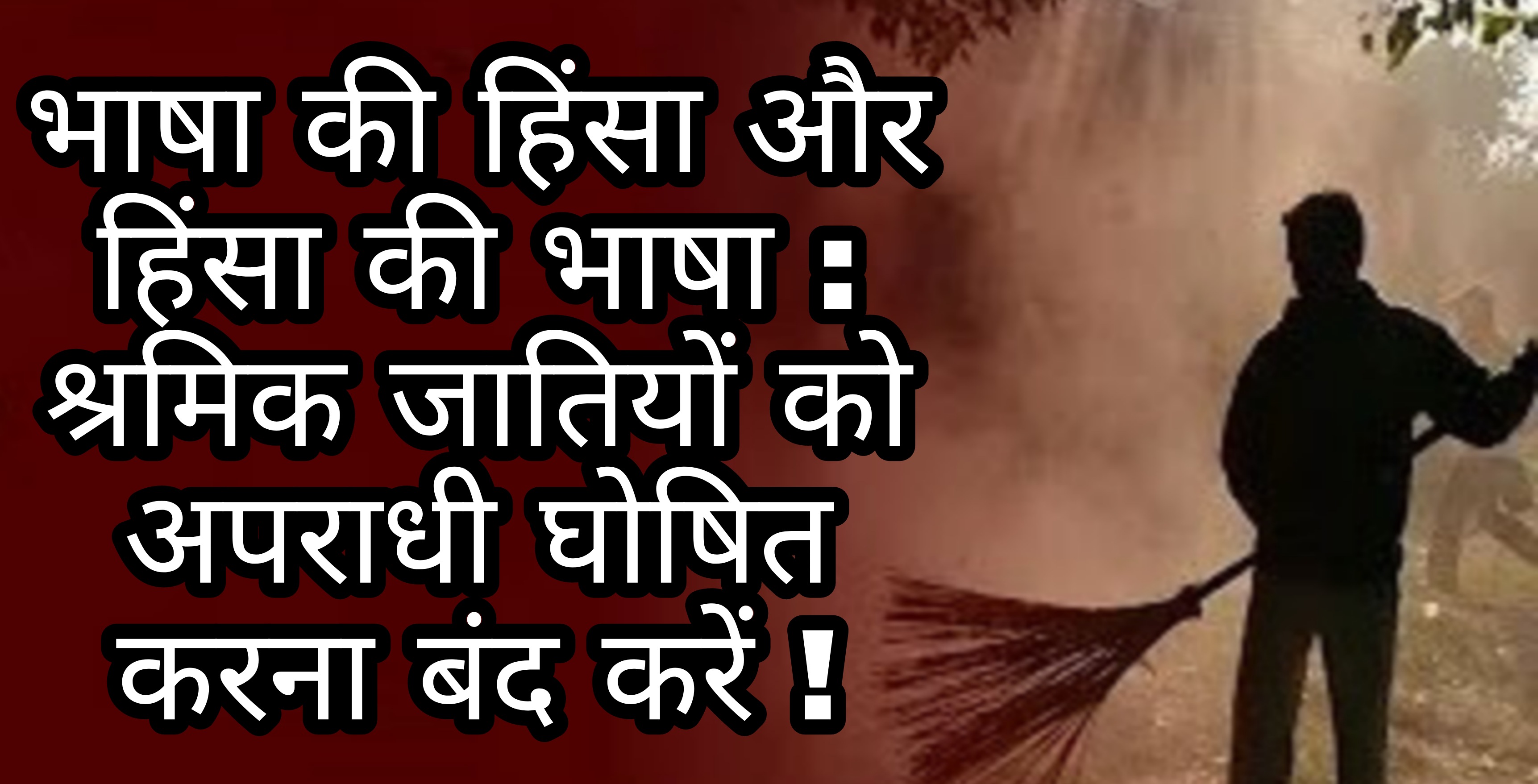
दुनिया भर में भाषा को राष्ट्र राज्य का एक पैमाना माना जाता है. राष्ट्र की भाषाई उत्पत्ति को लेकर स्टालिन की परिभाषा आम तौर पर गैर-मार्क्सवादियों द्वारा भी स्वीकार की जाती है लेकिन राज्य या राष्ट्र की तरह या फिर राष्ट्रराज्य की तरह भाषा भी हिंसक हो सकती है, होती है.
भाषा की हिंसा और हिंसा की भाषा पर मैंने अपनी पिछ्ली कुछ नोट्स और बिखरे विचारों को एक लेख का रूप देकर इस मुद्दे पर अपनी सोच को आकार दिया है, जो यहां प्रस्तुत है. यह एक जाति, लिंग, वर्चस्व आधारित समाज में भाषा की कथित सकारात्मक भूमिका की सीमाओं को लेकर मेरा स्पष्ट मत है, जो मेरे विचार में हिंदी ही नहीं सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में लागू होती है.
हिंदी के प्रसिद्ध कवि दिवंगत मंगलेश डबराल जी ने दो साल पहले सोशल मीडिया पर लिखा –
हिंदी में कविता, कहानी, उपन्यास बहुत लिखे जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इन सबकी मृत्यु हो चुकी है. हालांकि ऐसी घोषणा नहीं हुई है और शायद होगी भी नहीं क्योंकि उन्हें खूब लिखा जा रहा है. लेकिन हिंदी में अब सिर्फ ‘जय श्रीराम’ और ‘बन्दे मातरम्’ और ‘मुसलमान का एक ही स्थान, ‘पाकिस्तान या कब्रिस्तान’ जैसी चीज़ें जीवित हैं. इस भाषा में लिखने की मुझे बहुत ग्लानि है. काश, मैं इस भाषा में न जन्मा होता !
(मंगलेश डबराल की 26 जुलाई 2019 की सोशल मीडिया पोस्ट )
इस पोस्ट पर पक्ष विपक्ष में तब काफ़ी हंगामा मचा. उसी समय ‘the hindu’ में छपे एक लेख में यही बात कही गई है कि 1925 से 1945 के बीच जर्मन भाषा नस्लवाद और सामूहिक नरसंहारों को जायज़ ठहराने का माध्यम बन गई थी. अब हिंदी भी उसी रास्ते पर है. मैं मंगलेश डबराल और इस लेख से पूरी तरह सहमत था लेकिन साथ ही मेरा मानना है कि भाषा नहीं बल्कि उसका समाज और उस समाज की बनावट ज्यादा मायने रखते हैं, भाषा तो बस माध्यम है.
मैं मानता हूं हिंदी भाषा आज के आसन्न या स्पष्ट फासीवादी दौर में हिंसक नहीं हुई है, वो हमेशा से हिंसक रही है. अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण हिंदी के अपर कास्ट प्रगतिशील साहित्यकार हिंसा की भाषा और भाषा की हिंसा की उन गहरी जड़ों को नहीं देख पाते जो जो जाति, वर्ग और लिंग वर्चस्व आधारित समाज में बहुत भीतर तक समायी हुई हैं.
हिंदी की वर्तमान दशा में जितना अफ़सोस आज जताया जा रहा है, उसका कुछ हिस्सा भर अफ़सोस भी साहित्यकारों को तब नहीं हुआ जब इस भाषा में भंगी, चमार, डोम, चूहड़ा, रंडी जैसे तमाम शब्द इसके समाज से गाली के रूप में जगह बना चुके थे.
इसी भाषा में कहा गया-
पिछड़ी जाति कहां से आई
कर्पूरी की मां………..चु….
इस तरह की भाषाई अभिव्यक्तियों से इन्हें क्यों नहीं लगा कि ये भाषा मर चुकी है ? उच्च जातीय प्रगतिशील मानस जातीय गालियों और वर्चस्व को स्वाभाविक मान कर चलता है और वही जब साम्प्रदायिक रूप ले लेता है तो वो उन्हें फासीवाद का स्पष्ट रूप लगने लगता है. ये उनकी दृष्टि की सीमा है जो एक गहन ऐतिहासिक समस्या को तात्कालिकता में समेट देना चाहती है.
हिंदी के प्रिय साहित्यकारों, आपकी ‘श्रेष्ठ ‘भाषा में हमारे लिये गालियों के अलावा शब्द तक नहीं हैं और ये बात आपको समस्या नहीं लगती, आपको बिलकुल अहसास नहीं कि आपकी भाषा कितनी दरिद्र है.
आपका समाज और इसकी भाषा हमेशा से फासीवादी रहे है और वंचित तबकों का आपराधीकरण आपकी भाषा का एकदम सामान्य चरित्र है बानगी देखें –
समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध
– दिनकर
हिंदी साहित्य की इस बेहद प्रसिद्ध कविता में ये व्याध कौन है ? और ये व्याध होने के कारण स्वाभाविक ही अपराधी क्यों है ?
ये बहेलिया है जो एक श्रमिक अस्पृश्य जाति होती है, जो पक्षियों को पकड़कर अपना रोजगार करती है, जो कि बेहद मेहनत का काम है. लेकिन हिंदी कवि इसे स्वाभाविक ही पापी मानकर चलता है. लगभग सभी हिंदी कवि ऐसा करते हैं और इनमें से कोई कवि राम को क्रूर नहीं मानता, जो कि अपनी पत्नी के कहने पर एक मृग का शिकार करने को आवश्यक मानते हैं. राम भगवान हैं और व्याध अपराधी ऐसा क्यों ?
तथाकथित प्रगतिशील महाकवि ??? निराला ने ‘राम’ को अपनी प्रसिद्ध कविता में प्रगतिशीलता और क्रांति ??? के वाहक के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है और मार्क्सवादी ?? रामविलास शर्मा के विमर्श का तो कहना ही क्या, वे एक वैदिक ब्राह्मण मार्क्सवादी का रामराज्य है और कुछ नहीं.
आपको कई कविताएं और कहानियां मिल जाएंगी जिनमें बहेलिये को एक क्रूर, स्वार्थी इंसान के लिये बिम्ब के बतौर इस्तेमाल किया गया है, कई इनमें से प्रगतिशील लोगों ने भी लिखी हैं. इसी तरह कसाई का बिम्ब भी साहित्य में आता है. चांडाल भी एक अस्पृश्य जाति है, जिसका चित्रण और साथ ही इस बिम्ब का प्रयोग भद्दे तौर पर हिंदी साहित्य में किया जाता है.
कंजर, जो एक घुमंतू अस्पृश्य और श्रमशील जाति है, को आम बोल चाल के अलावा फ़िल्मों और कहानियों आदि में एक गाली के बतौर इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह मछुवारों का भी जिक्र होता है.
क्या आपने किसी ख्यातिलब्ध सवर्ण प्रगतिशील कवि या साहित्यकार की कोई ऐसी कविता या रचना पढ़ी है जिसमें किसी पुरोहित या ज्योतिषी आदि को ठीक वैसे ही नकारात्मक बिम्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया हो जैसे बहेलिया, कंजर, कसाई या चांडाल को किया जाता है ? जबकि ज्योतिषी द्वारा की गई सामाजिक हिंसा के सामने अपना पेट पालने के लिए पक्षियों को पकड़ने वाले दलित बहेलिया के द्वारा की गई हिंसा कुछ भी नहीं.
बहेलिया, कंजर, चांडाल, नट, मदारी आदि सब दलित जातियों के नाम हैं. अगर किसी को संदेह है तो के. एस. सिंह का ‘पीपुल ऑफ इंडिया’ देख ले.
वर्चस्व की अपनी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते हिंदी के कवि साहित्यकार अपने समाज की संरचना से वर्चस्व की भाषा को ही इस्तेमाल करते हैं. वो अपने आपको प्रगतिशील मूल्यों का वाहक दिखाने की कोशिश में श्रम की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, लेकिन साथ ही सचेत रूप से या अनजाने में श्रमिक जातियों के समाज मे ब्राह्मणीय तन्त्र द्वारा स्थापित आपराधिक चरित्रबोध को और गहरे स्थापित करते हैं. श्रम की प्रतिष्ठा और श्रमिकों का आपराधिक प्रस्तुतिकरण दोनों बातें एक साथ कहने के लिए या तो पर्याप्त भोलापन चाहिये या हद दर्ज की धूर्तता.
अपनी भाषा और बिम्बों के चयन में ब्राह्मणीय तन्त्र के प्रतीकों को बचाते हुए ये लोग श्रमिक जातियों को स्वाभाविक ही अपराधी घोषित करते हैं और तुर्रा ये कि इन्हें लगता है कि ये प्रगतिशील हैं. फिर अंत में ये शिकायत करते हैं कि भाषा मर रही है.
ऐसे ही तमाम शब्द हैं जिनकी पैदाइश एक खास समुदाय से होती है, जिन्हें न केवल आपत्तिजनक बल्कि गाली बना दिया गया. शूद्र, चांडाल, कमीना, बहेलिया, कंजड़, कसाई और भी न जाने कितनी गालियां या नकारात्मक शब्द कुछ खास समुदायों को इंगित करते हैं. ‘शूद्र’ एक जाति थी जिसका पहला उल्लेख ईसा से 300 साल पहले यास्क के निरुक्त में मिलता है. इसी तरह ‘कमीन’ एक समुदाय है.
आप हिंदी की कोई भी गाली उठायें वो या तो जाति आधारित है या लिंग आधारित. दरअसल ये वर्चस्व की संस्कृति की दरिद्रता है जो स्त्रियों और पराजित या शोषित समुदायों के नाम को गाली की तरह इस्तेमाल करती है.
अब कुछ ख़ास शब्दों पर चर्चा जो आम बोल चाल, साहित्य, फ़िल्मों आदि में अपने वास्तविक अर्थ में प्रयोग होने की बजाय कुछ इस तरह इस्तेमाल किये गये जिससे ना केवल उनके अर्थ बदल गये बल्कि उन शब्दों के चारों ओर एक ऐसा नकारात्मक वातावरण, साहित्य के द्वारा बना दिया गया कि वो शब्द साधारण समय में शंका और असाधारण समय (जैसा कि आजकल है) में घृणा और हिंसा को उकसाने में सहायक हुए. जैसे एक शब्द है ‘कसाई.’
कसाई कौन है ? ये हमारे समाज को सस्ता और ताज़ा प्रोटीन मुहैया करने की कड़ी का अहम हिस्सा है, बस इतना ही. इतनी ही इसकी पेशागत सच्चाई है. ये बिलकुल आम इंसान है जिसे आपकी और हमारी तरह दर्द होता है. जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं. जिसका एक परिवार होता है. सोचिये अगर आपके समाज में कसाई ना हों तो क्या होगा ?
लेकिन हमारा साहित्य, जो वस्तुनिष्ठ होने और मानवीय गरिमा पर बात बहुत करता है, वो कसाई के प्रति वस्तुनिष्ठ और गरिमापूर्ण व्यवहार कभी नहीं करता. कसाई का बिम्ब इस तरह रूढ़ बना दिया गया है कि ये कविता, कहानी आदि सभी जगहों पर नकारात्मक अर्थो में प्रयोग होता है.
मोबलिंचिंग का शिकार होने वाले लोगों में धार्मिक पहचान के बाद पेशागत पहचान देखी जाय तो कसाई काफी मिल जाएंगे, ऐसा क्यों है ? हम ऐसी भाषा क्यों बना रहे हैं जिसमें किसी खास जाति और पेशे के लोग Vulnerable हो जांय ? इस तरह के अनगिनत उदाहरण दिये जा सकते हैं जिसमें प्रगतिशील साहित्यकारों ने भी कसाई को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया है.
उदाहरण के लिये मैंने कुछ समय पहले अरुंधति की किताब ‘एक था डॉ एक था संत’ पढ़ी. एक जगह विभाजन को लेकर रेडक्लिफ लाइन का जिक्र करते हुए लेखिका लिखती हैं –
विभाजन की इस रेखा को इस तरह खींचा गया कि एक कसाई भी गोश्त को काटते हुए इससे अधिक संवेदनशील होगा.
बड़ी बात है, साहित्यिक रूप से चमत्कार वाली बात ! लेकिन कसाई का क्या दोष है ? इस बात से कसाई का क्या चित्र दिमाग़ में बनता है ? पहली बात तो यह चित्र ही गलत है. मैं अपने पेशे के कारण जानता हूं कि एक कुशल कसाई को गोश्त बहुत सलीके और संवेदनशीलता से काटना पड़ता है, नहीं तो उसकी वैल्यू कम हो जायेगी. दूसरी बात हम संवेदनशीलता की दुहाई देने के क्रम में एक पूरे समुदाय के प्रति समाज के असंवेदनशील हो जाने को बढ़ावा दे रहे हैं.
अरुंधति के विचार क्या हैं ये सब जानते हैं लेकिन उनकी भाषा उनसे क्या करवा रही है, वो खुद नहीं जानती. ये सभी प्रगतिशीलों की कहानी है. प्रगतिशील साहित्यकारों को पढ़ते हुए ही ऐसे कई उदाहरण आपको दिखाई देंगे.
हिंदी के प्रसिद्ध कवि वीरेन डंगवाल की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति ‘दुश्चक्र में स्रष्टा’ से ली गई यह कविता देखिएगा –
विद्वेष
यह बूचड़खाने की नाली है.
इसी से होकर आते हैं नदी के जल में
ख़ून
चरबी, रोयें और लोथड़े.
प्रेम की सुंदरता का निषेध करनेवाले
इसी तट पर आते हैं
हाथ-पैर धोने.
इस कविता को पढ़कर आपके मन में बूचड़खाने / बूचड़ /कसाई का कैसा चित्र बनता है या पहले से बने हुए चित्र पर कैसा रंग चढ़ता है ? मेरे विचार में ये वही रंग है जिसका निषेध करने की कोशिश कवि कर रहा है. भाषा की हमेशा हत्या नहीं होती, कई बार वो गफ़लत में भी मारी जाती है. और ये गफ़लत अपनी सांस्कृतिक जड़ों के कारण प्रगतिशीलों से अक्सर हो जाया करती है.
अगर श्रम की प्रतिष्ठा वास्तव में स्थापित करनी है तो श्रमिकों को अपराधी घोषित करना बंद करें, और अगर श्रमिकों को अपराधी बताकर ‘कालजयी’ रचना लिखना चाहते हैं तो वो समय अब जा चुका है. कृपया सुधर जायें, ऐसा करने पर अब आपको लानत ही ज़्यादा मिलेगी.
श्रमिक जातियों, वंचित तबकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को स्वाभाविक ही निम्न और आपराधिक घोषित करने वाली किसी भी हिंसक भाषा को, भाषा की हिंसा को, हिंसा की भाषा को ज़रूर ही मर जाना चाहिए. मैं इसकी मौत की दुआ करता हूं.
- मोहन आर्या
Read Also –
शुद्ध हिंदी ने हिंदुस्तानी डुबोई, अंग्रेज़ी तार दी
आइआइटी इंदौर : संस्कृत भाषा में पढ़ाई – एक और फासीवादी प्रयोग
क्या इस समय और समाज को एक नई भाषा की ज़रूरत नहीं है ?
[प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे…]


